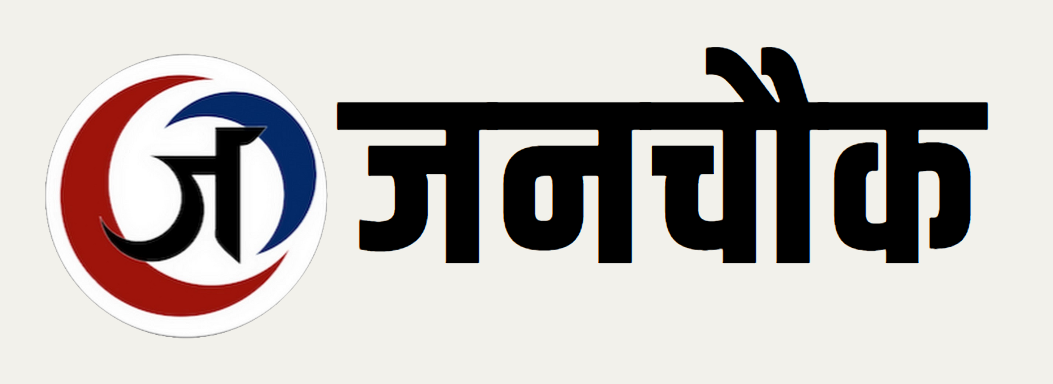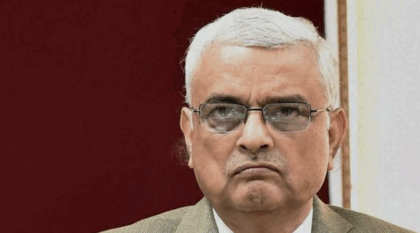पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या, पूर्णिया में हुआ नरसंहार और सिवान में हुई सामूहिक हत्याएं — ये तीनों घटनाएं बिहार की वर्तमान दशा का त्रासद प्रतीक बनकर उभरी हैं। ये केवल ‘कानून व्यवस्था की समस्या’ नहीं है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक दिवालियापन, सामाजिक असंतुलन और राजनीतिक शून्यता की संगठित अभिव्यक्तियां हैं।
यह वह समय है, जब बिहार को केवल अपराधियों से नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र से डर लगने लगा है, जो नागरिकों की सुरक्षा और संविधान की रक्षा के लिए बना था, परंतु बिहार में वह तंत्र आज अपने ही बोझ तले चरमराता दिखाई दे रहा है।
गोपाल खेमका की हत्या: चेतावनी की उपेक्षा और कानून का अपमान
व्यवसायी गोपाल खेमका की उनके ही घर के सामने सरेआम हत्या उस शहर में हुई, जहां सरकारी बैठकों में ‘कानून-व्यवस्था’ के दावे रोज़ गूंजते हैं। यह न केवल एक हत्याकांड है, बल्कि बिहार के व्यापारिक समुदाय को दिया गया एक सीधा संदेश है: सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी ख़ुद की मजबूरी है।
यह भूलना नहीं चाहिए कि खेमका के बड़े बेटे की हत्या पहले ही हो चुकी थी, और उसके हत्यारे की भी हत्या कर दी गई थी। यानी एक पूरा चक्र चलता रहा — हत्या पर हत्या — और पुलिस-प्रशासन बस मूक दर्शक बना रहा।
खेमका को मिल रही धमकियों की जानकारी भी पुलिस को थी, पर कार्रवाई नहीं हुई। यह केवल निष्क्रियता नहीं, बल्कि आपराधिक लापरवाही है, और इससे भी ज़्यादा खतरनाक यह है कि यह सब बिहार में अब ‘सामान्य’ बन चुका है।
पूर्णिया और सिवान के नरसंहार: क्या लौट रहा है अपराध और सत्ता का गठजोड़?
पूर्णिया में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को जलाकर मार दिया गया। सिवान में एक ही दिन में कई लोगों की हत्या हुई — जिनमें किसी के पास अपराधी बैकग्राउंड था, तो किसी के पास नहीं। इससे यह साफ़ है कि अब किसी की भी हत्या संभव है — अगर वह सत्ता के समीकरण में असुविधाजनक हो, या अपराधियों के रास्ते में आए।
सवाल यह है कि क्या बिहार उस दौर में लौट रहा है, जब अपराधी राजनीति करते थे और नेता अपराधियों की तरह व्यवहार करते थे?
सिवान की पहचान दशकों तक बाहुबलियों के अड्डे के रूप में रही है। उनके खिलाफ जो भी खड़ा हुआ, या तो मारा गया या मिटा दिया गया। अब फिर से वही खून-खराबा, वही खामोश पुलिस, वही डरे हुए पत्रकार — यह सब इस बात की ओर संकेत करता है कि माफिया-राज अब फिर से स्थापित हो रहा है, शायद इस बार और अधिक आत्मविश्वास और अधिक संरक्षण के साथ।
राजनीतिक निष्क्रियता और प्रशासनिक अकर्मण्यता: क्या शासन अब केवल भाषण में रह गया है ?
जब अपराध होते हैं, तब नेता ट्वीट करते हैं। जब नरसंहार होता है, तब जांच के नाम पर टीम भेज दी जाती है और जब परिवार न्याय मांगते हैं, तब उन्हें शांति बनाए रखने की अपील सुनने को मिलती है।
यह पूरी राजनीति अब संवेदना की नहीं, रणनीति की भाषा बोलती है, जहां उद्देश्य पीड़ित की मदद नहीं, छवि की रक्षा करना है।
‘सुशासन बाबू’ के बिहार में प्रशासनिक सुशासन अब महज़ पोस्टर की बात बन गया है।
थाने केवल रसूखदारों की सुनवाई करते हैं, आम जनता के लिए एफआईआर दर्ज कराना भी एक संघर्ष बन गया है। ज़िले के अधिकारी जनता की रक्षा करने में नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ताधारी नेताओं को संतुष्ट करने में लगे हैं।
अगर प्रशासन जनता के डर के बजाय नेताओं के आदेश पर चले, तो फिर जनता को सिर्फ़ अपराधियों से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वह प्रशासन से ही डरने लगती है।
सामाजिक परिप्रेक्ष्य: जब समाज न्याय व्यवस्था से मुंह मोड़ने लगे
इन घटनाओं ने बिहार के सामाजिक ढांचे में ज़हर घोल दिया है। कानून जब निष्क्रिय हो, पुलिस जब मूकदर्शक हो, न्याय जब अमीर और प्रभावशाली के आगे ही संभव हो, तब आम लोग या तो चुप हो जाते हैं, या हथियार उठा लेते हैं।
जातीयता, सामंती मानसिकता, और आर्थिक असमानता पहले से ही बिहार को जकड़े हुए हैं। उस पर अब जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी खुलेआम हत्या कर रहे हैं, तो समाज में डर के साथ-साथ आक्रोश भी गहराता जा रहा है।
सबसे भयावह बात यह है कि लोग अब यह मानने लगे हैं कि पुलिस और न्यायपालिका सत्ता के अलावे किसी के साथ नहीं हैं।
जब जनता को अपनी ही सरकार से भरोसा उठ जाए, तो लोकतंत्र केवल एक चुनावी तमाशा बनकर रह जाता है।
इस अराजकता की जवाबदेही किसकी?
इन प्रश्नों का उत्तर अब कोई नहीं देना चाहता:
अगर हत्या के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, तो किसने उन्हें संरक्षण दिया?
जब व्यवसायी को धमकी दी जाती है, तो पुलिस क्यों मौन रहती है?
पुलिस सुधार का मुद्दा हर बार चुनावी घोषणापत्र में आता है, पर कभी ज़मीन पर क्यों नहीं उतरता?
यह सब महज़ ‘सिस्टम फेल’ की नहीं, बल्कि फेल कर दिए गए सिस्टम की कहानी है। ऐसे में बिहार तेज़ी से एक ऐसे राज्य में तब्दील होता जा रहा है, जहां सरकार घटनाओं को रोकने की नीयत से नहीं, घटनाओं की प्रतिक्रिया में चल रही है।
चौराहे पर खड़ा बिहार: आगे इतिहास या दुहराव?
पटना, पूर्णिया और सिवान की घटनाएं केवल अख़बार की सुर्खियां भर नहीं हैं, ये गंभीर चेतावनियां हैं। बिहार को तय करना है कि क्या वह एक बार फिर अपराध, जातिवाद और माफिया-राज के गर्त में जाएगा, या फिर एक नया, न्यायपूर्ण, और नागरिकों की रक्षा करने वाला राज्य बनाएगा ?
इस समय बिहार को किसी और ‘विकास यात्रा’ की ज़रूरत नहीं, उसे ईमानदार, संवेदनशील और जवाबदेह शासन की ज़रूरत है।
यह शासन ऐसा होना चाहिए, जो ‘घटना होने के बाद प्रतिक्रिया’ न करे, बल्कि ‘घटना न हो’ यह सुनिश्चित करे।
और यह परिवर्तन केवल सड़कों पर प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या सांत्वना यात्रा से नहीं आएगा- यह परिवर्तन जनता के आत्मबल, वोट की शक्ति और चेतना से सम्भव है।
हत्या केवल व्यक्ति की नहीं, समाज की भी होती है
हर हत्या के साथ कोई परिवार उजड़ता है, कोई व्यापारी डरता है, कोई बच्चा खामोश हो जाता है, और समाज एक और बार असहाय हो जाता है। पटना, पूर्णिया और सिवान की हत्याएं केवल कानून की हार नहीं हैं, ये बिहार की आत्मा का लहूलुहान होना है।
अब बिहार को यह तय करना है- क्या वह इसी खौफ, चुप्पी और हिंसा के साथ जीते रहना चाहता है, या वह सच में बदलाव चाहता है।
बदलाव की शुरुआत वहां से होगी, जहां डर खत्म होगा, और डर तभी खत्म होगा जब शासन जनता के खिलाफ नहीं, जनता के लिए होगा। सामने चुनाव है और जनता के सामने मौक़ा है कि वह अपनी इस मंशा को वोट की चोट से करे।
(उपेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं।)