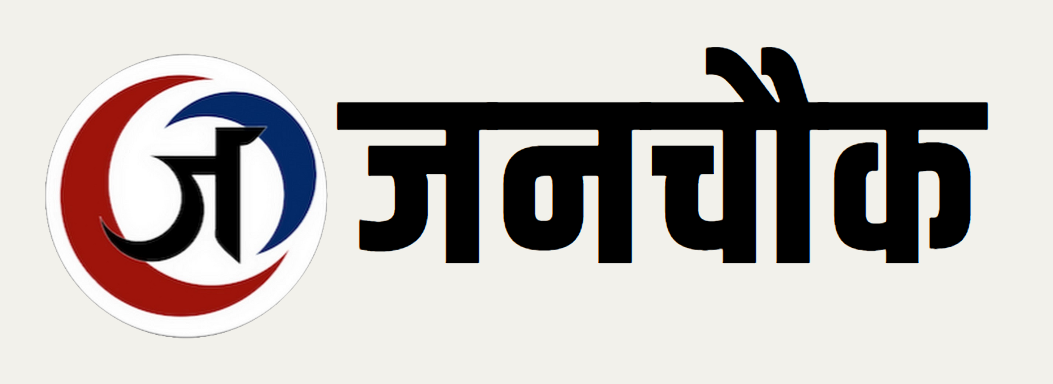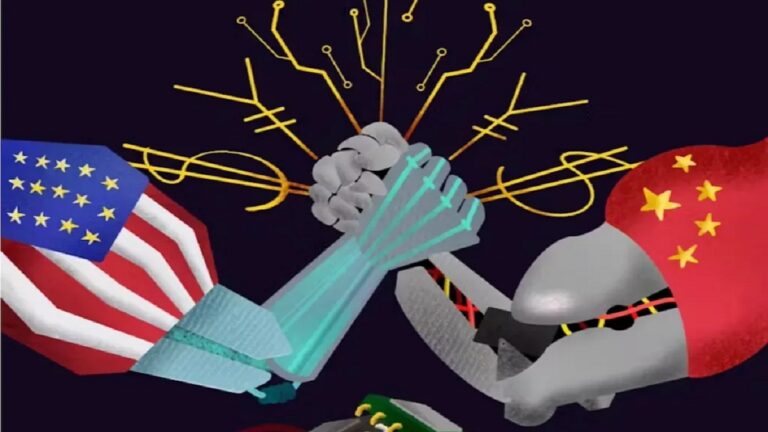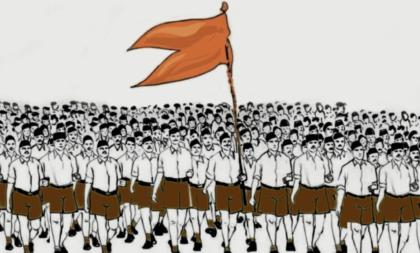भारत में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ढंग से नहीं होती, बच्चे कुछ सीखते नहीं, और परिणाम खराब होते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सवाल किया कि उन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वास्तव में पढ़ाने का पूरा समय और अनुकूल वातावरण मिल भी रहा है या नहीं?
सरकारी स्कूलों के शिक्षक पढ़ाने के अलावा और क्या-क्या करते हैं, इसका जवाब अगर आपको नहीं पता, तो जानिए: उन्हें बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की ज़िम्मेदारी निभानी होती है, जनगणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों में भाग लेना पड़ता है, कभी चुनावों में ड्यूटी करनी होती है तो कभी सरकारी योजनाओं के फार्म भरवाने और लाभार्थियों की सूची बनाने का काम भी उन्हें ही सौंपा जाता है। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन से लेकर जन वितरण प्रणाली की जांच तक-शिक्षक हर जगह मौजूद हैं, बस अपने मूल कार्य यानी शिक्षण में नहीं।
क्या शिक्षक पढ़ा नहीं सकते?
यह तर्क देना कि शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाते, सरासर गलत है। नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में यही सरकारी शिक्षक जब पढ़ाते हैं, तो देश के सबसे बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्र न केवल बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल आते हैं बल्कि राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शानदार प्रदर्शन करते हैं। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि राज्य सरकारों के अधीन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ये शिक्षक क्यों पिछड़ जाते हैं?
जवाब साफ है: नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक से केवल शिक्षक का काम लिया जाता है, जबकि राज्य सरकारें अपने शिक्षकों को बहुद्देशीय कर्मचारी बना चुकी हैं। वे शिक्षकों को हर सरकारी सर्वेक्षण, अभियान और दस्तावेज़ीकरण के लिए उपलब्ध मानती हैं। ऐसे में शिक्षक का ध्यान बँटता है, समय नष्ट होता है, और विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती।
विश्व के विकसित देशों से सीखने की ज़रूरत
फिनलैंड को दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्थाओं में गिना जाता है। वहाँ शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण के अग्रदूत माने जाते हैं। शिक्षक बनने के लिए वहाँ उच्च स्तरीय मास्टर डिग्री ज़रूरी होती है, और समाज उन्हें डॉक्टर और न्यायाधीश जैसी प्रतिष्ठा देता है। फिनलैंड में शिक्षकों को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक या गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं झोंका जाता, जिससे वे पूरी तरह शिक्षण कार्य पर केंद्रित रहते हैं।
नॉर्वे में भी शिक्षक सृजनशील और नीति-निर्माता भूमिका में होते हैं। वहाँ शिक्षक बच्चों के समग्र विकास में भागीदार होते हैं और स्कूल प्रशासनिक निर्णयों में भी उनकी भागीदारी रहती है। किसी भी चुनाव, सर्वेक्षण या योजनाओं के क्रियान्वयन से उनका कोई संबंध नहीं होता। शिक्षक पूरी तरह बच्चों के साथ-कक्षा में, लाइब्रेरी में, प्रयोगशालाओं में या उनकी रचनात्मक गतिविधियों में ही संलग्न रहते हैं।
स्वीडन में शिक्षक को बच्चों के विकास का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्हें बच्चों की ज़रूरत के अनुसार शिक्षण पद्धतियाँ चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है और उनकी जवाबदेही भी केवल शिक्षण के परिणामों पर होती है। अन्य सभी कार्यों के लिए अलग प्रशासनिक तंत्र होता है। इसीलिए वहाँ के विद्यालय आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और वैज्ञानिक सोच रखने वाले नागरिक तैयार करते हैं।
पंचायत स्तर पर नियुक्त हो अलग प्रशासनिक ढांचा
शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने का सबसे व्यावहारिक और जरूरी उपाय यह है कि पंचायत स्तर पर सचिव, सहायक सचिव और लेखपालों की स्थायी नियुक्ति की जाए। यह वर्ग स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को संभाले, बीएलओ की भूमिका निभाए, जनगणना, सर्वेक्षण और योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे कार्यों में सरकार का साथ दे। आज डिजिटल युग में डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग विशेषज्ञ कार्य बन चुका है-जिसे ठीक से करने के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण और तकनीकी दक्षता आवश्यक है, न कि शिक्षण कौशल।
परिणाम आधारित शिक्षा की बात सिर्फ काग़ज़ पर क्यों?
जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सरकारी योजनाएँ परिणाम आधारित शिक्षा की बात करती हैं, तो क्या वे यह सुनिश्चित नहीं कर सकतीं कि शिक्षक को पढ़ाने के लिए पूरा समय और सम्मान मिले? पढ़ाई का परिणाम तब ही बेहतर हो सकता है जब शिक्षक की भूमिका को केंद्र में रखा जाए और उसे प्रशासनिक कार्यों से मुक्त किया जाए।
यदि सरकार यह अपेक्षा करती है कि शिक्षक पढ़ाई के साथ-साथ बीएलओ का भी काम करे, योजनाओं का भी प्रचार करे, सत्यापन का भी भार उठाए, तो यह वैसा ही है जैसे किसी डॉक्टर को ओपीडी के साथ-साथ दवाइयों का स्टॉक भी गिनने और अस्पताल की बिजली बिल भरने की ज़िम्मेदारी दे दी जाए। क्या हम ऐसा किसी डॉक्टर या इंजीनियर के साथ करते हैं? फिर शिक्षक के साथ यह अन्याय क्यों?
शिक्षा को बचाना है तो शिक्षक को पढ़ाने दो
सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए न कोई विदेशी मॉडल चाहिए, न कोई भारी भरकम बजट। बस इतना कर दिया जाए कि शिक्षक को पढ़ाने का समय, संसाधन और सम्मान मिले-बाकी काम वो खुद कर देगा। नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के उदाहरण सामने हैं। आज जरूरत इस बात की है कि केंद्र और राज्य सरकारें स्पष्ट नीति बनाएँ जिसमें तय हो कि शिक्षकों से किसी भी प्रकार का गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा, और इसके लिए पंचायत स्तर पर अलग प्रशासनिक तंत्र तैयार किया जाएगा।
शिक्षक समाज का वह स्तंभ है जो आने वाली पीढ़ियों को गढ़ता है। उसकी ऊर्जा, समय और विवेक को गैर-जरूरी कार्यों में झोंकना केवल शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्याय नहीं, बल्कि राष्ट्र की बौद्धिक पूंजी को नष्ट करना है। अब वक्त आ गया है कि हम एक स्वर में कहें-“शिक्षक को शिक्षक रहने दो। बाकी काम पंचायत सचिवों और लेखपालों को दो!”
(मनोज अभिज्ञान स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)