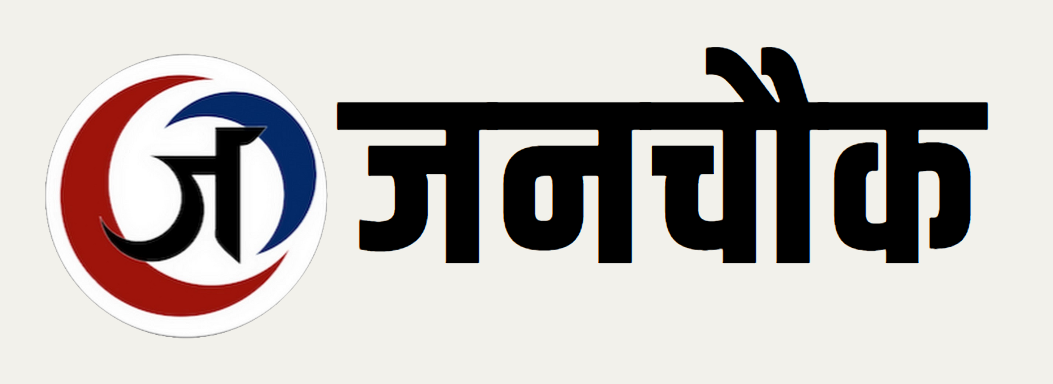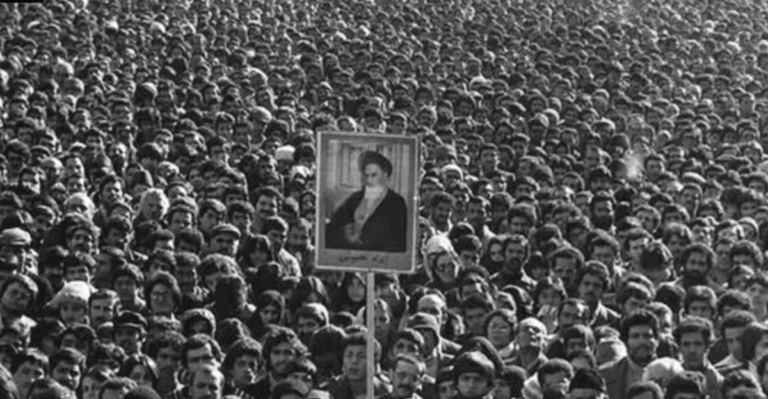आलेख की शुरुआत आइए, पहले घटनाक्रम पर ध्यान देः
- बीते दो जुलाई को निर्वासन में रह रहे तिब्बती नेता दलाई लामा ने अपने 90वें जन्म दिन से ठीक पहले ये एलान किया कि उनके उत्तराधिकारी का चुनाव फोद्रांग ट्रस्ट करेगा, जिसकी स्थापना दलाई लामा के कार्यालय ने 2015 में की थी।
- चीन ने तुरंत इस एलान को ठुकरा दिया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दलाई लामा और (तिब्बती बौद्ध धर्म में दूसरे नंबर के नेता) पंचेन लामा का चयन धार्मिक रिवाजों और ऐतिहासिक परंपराओं के अनुरूप होगा। यह चुनाव ‘स्वर्ण कलश’ से पर्ची निकाल कर होता आया है और यह अनिवार्य है कि इस चुनाव प्रक्रिया को चीन की सरकार अपनी मंजूरी दे।
- अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरन रिजीजू ने तुरंत चीन के दावे को ठुकराते हुए दलाई लामा के रुख का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी का चुनाव दलाई लामा की इच्छाओं के अनुरूप ही होगा।
- चीन ने किरन रिजीजू के बयान पर एतराज जताया। माओ निंग ने कहा कि भारत को तिब्बत संबंधी मुद्दों पर सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि सुधर रहे आपसी संबंधी पर खराब असर ना पड़े। माओ ने भारत से चीन के अंदरूनी मामलों में दखल ना देने की सलाह दी।
- चीन के इस सख्त रूख के बाद भारत सरकार रिजीजू के बयान से पीछे हटी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में स्पष्ट किया कि किसी धर्म या आस्था से संबंधित मामलों में भारत सरकार ना तो कोई रुख नहीं लेती है, ना ही ऐसे मामलों में बोलती है।
- बहरहाल, दलाई लामा का 90वां जन्म दिन रविवार को हिमाचल प्रदेश के मैकलियॉडगंज मनाया गया। खबरों के मुताबिक भारत सरकार के दो मंत्रियों- किरन रिजीजू और राजीव रंजन सिंह ने इस समारोह में भाग लिया।
इस प्रकरण ने भारत- चीन संबंध में तिब्बत के पहलू को फिर से जिंदा कर दिया है। ये कांटा 1950 के दशक में ही आ फंसा था, जब 1959 में दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ तिब्बत से भाग कर भारत आ गए और तत्कालीन जवाहर लाल नेहरू सरकार ने ना सिर्फ उन्हें पनाह देने, बल्कि भारत की जमीन से तिब्बत की “निर्वासित सरकार” चलाने की इजाजत भी दी। तब से ये कांटा लंबे समय तक चुभता रहा। बल्कि 1962 में हुए युद्ध का भी यह एक प्रमुख कारण था।
इस विवाद को विराम देने का महत्त्वपूर्ण कदम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान उठाया था। वहां चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ वाजपेयी की बातचीत के बाद जारी साझा बयान में भारत ने स्पष्ट रूप से कहा- ‘तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है।’ यह पहला मौका था, जब भारत ने TAR को चीन के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता दी। वैसे, 1954 में हुए पंचशील समझौते में चीन के इलाके के रूप में तिब्बत की चर्चा हुई थी, मगर उसके बाद से भारत की तमाम सरकारों ने इस मामले में एक किस्म की अस्पष्टता बनाए रखी।
(यहां ये साफ कर लेना चाहिए कि तिब्बत और TAR शब्दों का इस्तेमाल अलग संदर्भों में होता है। तिब्बत बहुत बड़ा पवर्तीय इलाका है, जिसमें चीन के कई प्रांत आते हैं। तिब्बत असल में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, किंगहाई, सिचुआन, युन्नान, और गांसु प्रांतों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र वह इलाका है, जो पहले चीन के तहत स्वायत्त क्षेत्र होता था और जहां दलाई लामा का शासन था। मौजूदा दलाई लामा से पहले 13 अन्य दलाई लामा हो चुके हैं।)
तिब्बत पर भारत के रुख परिवर्तन के बदले में चीन ने सिक्किम पर भारत की संप्रभुता को मान्यता देने की दिशा में कदम उठाए। सिक्किम 1975 तक स्वतंत्र देश था, जिसका तब भारत में विलय हुआ। चीन ने 2003 तक इस विलय को मान्यता नहीं दी थी। मगर 2003 के संयुक्त घोषणापत्र को इस रूप में लिखा गया, जिसका सीधा अर्थ यह था कि चीन सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग मानता है।
इस घटनाक्रम के बाद एक दशक तक भारत-चीन संबंधों में तिब्बत का मुद्दा नहीं उठा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई ऐसे मौके आए, जब ये संकेत मिला कि भारत सरकार फिर से ‘तिब्बत कार्ड’ खेलना चाहती है। लेकिन जब कभी मामला गरमाता दिखा, तो अक्सर मोदी सकार ने कदम वापस खींचे हैं। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की तिब्बत नीति को लेकर फिर से एक तरह की अस्पष्टता पैदा कर दी है। इस सिलसिले में कुछ घटनाएं उल्लेखनीय हैः
- नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में लोबसांग सांगेय को आमंत्रित किया गया, जो उस समय तिब्बत की निर्वासित सरकार (Central Tibetan Administration- CTA) के प्रमुख थे। इस कदम को तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रति प्रतीकात्मक समर्थन के रूप में देखा गया।
- दिसंबर 2016में राष्ट्रपति भवन में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में दलाई लामा को भी आमंत्रित किया गया। यह भारत की पिछली नीति से हट कर था। पहले दलाई लामा के साथ उच्च-स्तरीय आधिकारिक संपर्क से बचा जाता था।
- 2017 में दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश के तवांग की यात्रा करने की अनुमति दी गई। चीन अरुणाचल प्रदेश को ‘दक्षिण तिब्बत’ कहता है। इस यात्रा के दौरान तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दलाई लामा की अगवानी की।
- 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन सैन्य संघर्ष के बाद भारत ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) का उपयोग किया, जिसमें तिब्बती निर्वासित समुदाय के लोग शामिल हैं। इस बल को पांगोंग त्सो में तैनात किया गया और SFF के एक सैनिक की मृत्यु के बाद उनकी अंत्येष्टि को मीडिया में व्यापक कवरेज दी गई।
- 2021 से प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्म दिन पर सार्वजनिक रूप से बधाई देना शुरू किया, जो पहले के वर्षों में नहीं हुआ था। इसके अलावा दलाई लामा की लद्दाख यात्रा को भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा सुगम बनाया गया।
- जून 2024 में अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें नैंसी पेलोसी और माइकल मैककॉल शामिल थे, धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की। इस यात्रा को भारत सरकार ने समर्थन दिया बाद में इन सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह कदम पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
हाल में हुई घटनाओं को इसी क्रम में देखा गया है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी संबंधी विवाद पर किरन रिजीजू के बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण आया। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि चीन उससे संतुष्ट हुआ है। छह जुलाई को भारत स्थित चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिसकी भाषा खासी तल्ख थी। शू ने कहा,
“इस पर ध्यान दिया गया है कि कुछ भारतीय अधिकारियों ने हाल में दलाई लामा के पुनर्अवतरण के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। पुनर्अवतरण प्रक्रिया में हस्तक्षेप या उसे निर्देशित करने के विदेशी संगठनों या व्यक्तियों के हर प्रयास का चीन सरकार विरोध करती है। शिजांग (तिब्बत) चीन का अभिन्न हिस्सा है। तिब्बती बौद्ध धर्म की जड़ें चिनघाई तिब्बत पठार में हैं। जिन प्रमुख क्षेत्रों में तिब्बती बौद्ध धर्म का अनुपालन होता रहा है, वे चीन के अंदर हैं। दलाई लामा की वंशावली ने चीन के तिब्बत क्षेत्र में आकार ग्रहण किया और विकसित हुई।
धार्मिक हैसियत और पदनाम प्रदान करना चीन की केंद्रीय सरकार का विशेषाधिकार है। दलाई लामा का पुनर्अवतरण एवं उत्तराधिकार पूर्णतः चीन का आंतरिक मामला है। चीन सरकार धार्मिक मामलों में स्वंतत्रता एवं स्वशासन के सिद्धांतों का पालन करती है। वह दलाई लामा सहित सभी जीवित बुद्ध संबंधी प्रशासन कानून के तहत करती है। इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी जाएगी।”
(https://x.com/China_Amb_India/status/1941860724541722938?t=LDca8cIq_S8u8G3WlQOuNA&s=03)
जाहिर है, इस मामले में चीन का रुख सख्त है। भारत सरकार ने अगर चीन के रुख को चुनौती देने का मन बनाया है और इसके लिए जरूरी तैयारी की है, तो भारतीय अधिकारियों के वक्तव्यों का संदर्भ समझा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और इस मामले में सिर्फ नीतिगत अस्पष्टता को वापस लाने और उसे जताने के लिए “तिब्बत कार्ड” खेला जा रहा है, तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कहा जा सकता है कि बिना राष्ट्रीय शक्ति को विकसित किए और हर स्थिति के लिए देश को तैयार किए, ऐसा कार्ड खेलना खतरनाक हो सकता है।
इस मामले में अमेरिका और उसके साथी पश्चिमी देशों की वक्ती जरूरतों के हिसाब से तय की जाने वाली नीति से प्रभावित होना कतई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। उस समय तो बिल्कुल नहीं, जब पश्चिमी देश चीन को घेरने के लिए विभिन्न मुद्दों को अपनी सुविधा से उठा रहे हैं। तिब्बत का मुद्दा पुराना है। खुद दलाई लामा का समूह अतीत में यह स्वीकार कर चुका है कि वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए से धन प्राप्त करता रहा है। (https://www.nytimes.com/1998/10/02/world/world-news-briefs-dalai-lama-group-says-it-got-money-from-cia.html). कई लेखकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि सीआईए ने अपने कम्युनिस्ट विरोधी अभियान के तहत दलाई लामा के गुट का इस्तेमाल किया। इसलिए पश्चिमी नैरेटिव के अनुरूप नीति तय करना सही कदम नहीं माना जाएगा।
भारत को इस संबंध में अपने हितों के अनुरूप स्वतंत्र समझ के आधार पर चलना चाहिए। अतः सही नीति तय करने का दो आधार हो सकता है। पहला, इसे ध्यान में रखते हुए कि तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति क्या रही है? दूसरा, यह कि आजादी के बाद से भारत का इस मामले में क्या रुख रहा और उसके क्या परिणाम हुए? इन दोनों मुद्दों पर एक जानकारी भरी किताब 2021 में आई। नेहरू, तिब्बत एंड चाइना नाम की इस किताब के लेखक भारतीय विदेश मंत्रालय में शोध इकाई के प्रमुख रह चुके पूर्व राजनयिक अवतार सिंह भसीन हैं। इस किताब में भसीन ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखागार की सामग्रियों का विस्तृत उपयोग किया है। इनमें नेहरू पेपर्स नाम से ज्ञात दस्तावेज और भारतीय विदेश मंत्रालय के कागजात शामिल हैं।
इस किताब में भसीन ने कहा है,
- तिब्बत पर चीन का दावा चिंग वंश के दौरान उस क्षेत्र पर चीन के रहे प्रभुत्व (suzerainty) पर आधारित है।
- भसीन ने तिब्बत के बारे में भारत में प्रचलित परंपरागत कथानक को चुनौती दी है। कहा है कि तिब्बत के मामले में चीन का रुख पूर्णतः निराधार नहीं है।
- इस पुस्तक के मुताबिक 1720 से, जब चिंग वंश का शासन था, तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व रहा।
- 1912 में चिंग वंश का राज खत्म होने के बाद अस्तित्व में आए चीनी गणराज्य ने तिब्बत पर अपने उत्तराधिकार का दावा किया।
- तब भारत पर ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन ने तिब्बत पर चीनी suzerainty को मान्यता दी, लेकिन तिब्बत पर चीन की संप्रभुता (sovereignty) के बारे में अस्पष्ट नीति बनाए रखी। इस दौरान चीन का केंद्रीय शासन कमजोर रहा और बाद में चीन गृह युद्ध में उलझ गया। उस दौरान तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पर दलाई लामा के शासन को लगभग स्वायत्तता हासिल रही।
(भसीन की तिब्बत संबंधी समझ इन इंटरव्यूज में भी व्यक्त हुई हैः
https://www.youtube.com/live/jPbw69AvPBg)
- एक अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट क्रांति के बाद अस्तित्व में आए PRC (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) ने सूरत बदलने का प्रयास किया। अक्टूबर 1950 में वहां चीन की सेना गई। उसके दबाव में 1951 में दलाई लामा ने PRC के साथ 17 सूत्री समझौता किया, जिसमें चीन की संप्रभुता को उन्होंने मान लिया।
- 1954 में पंचशील समझौते के तहत भारत ने भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया।
- मगर 1959 में तिब्बत में आंतरिक विद्रोह और उस पर सैन्य कार्रवाई के बाद जब मौजूदा दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ भारत आए, तो तत्कालीन नेहरू सरकार ने उन्हें धर्मशाला स्थिति मैकलियोडगंज से निर्वाचित सरकार चलाने की इजाजत दे दी। यहां से वो तनाव शुरू हुआ, जिसकी परिणति 1962 में भारत- चीन युद्ध के रूप में हुई।
- तब से 2003 तक भारत की तिब्बत संबंधी नीति में अस्पष्टता थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तब अपनी बीजिंग यात्रा के समय उसे दूर कर दिया।
लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में स्थिति फिर से बदलती दिखी है। डोकलाम संकट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अप्रैल 2018 में चीन के वुहान में हुई अनौपचारिक शिखर वार्ता के जरिए विवाद के मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश हुई थी। मगर अगस्त 2019 में धारा 370 को खत्म करने और उसके तुरंत बाद भारत का नया राजनीतिक मानचित्र जारी करने के मोदी सरकार के कदम के बाद भारत-चीन संबंधों में तनाव वापस आ गया। अक्टूबर 2019 में महाबलिपुरम में फिर से मोदी और शी के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता हुई। लेकिन वह संभवतः नाकाम रही। जून 2020 में गलवान घाटी की वारदात के बाद संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए।
अब जबकि संबंधों में सुधार के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, दलाई लामा संबंधी मसले ने नई स्थिति पैदा कर दी है। इस स्थिति में प्रासंगिक मुद्दा यही है कि अगर राष्ट्रीय शक्ति निर्मित कर चीन के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भारत तैयार है, तो तनाव का जोखिम उठाने का तर्क समझा जा सकता है। मगर बात सिर्फ पिन चुभा कर कदम वापस खींचने जैसी है, तो उचित यही होगा कि ऐसा ना किया जाए।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)