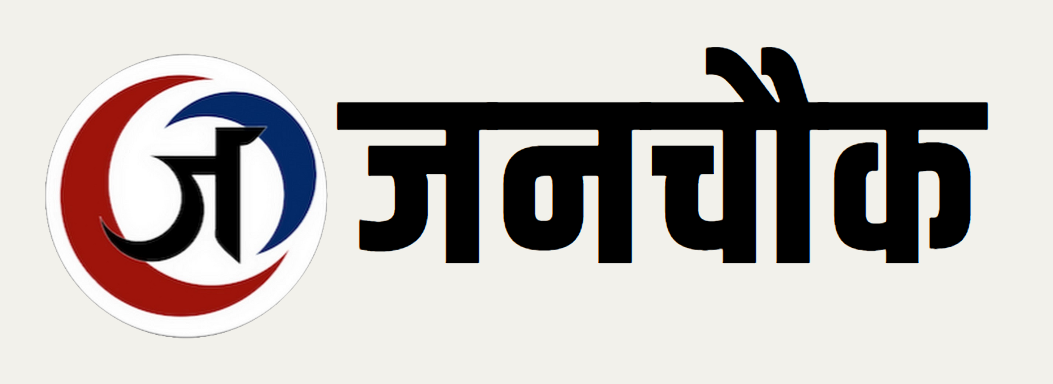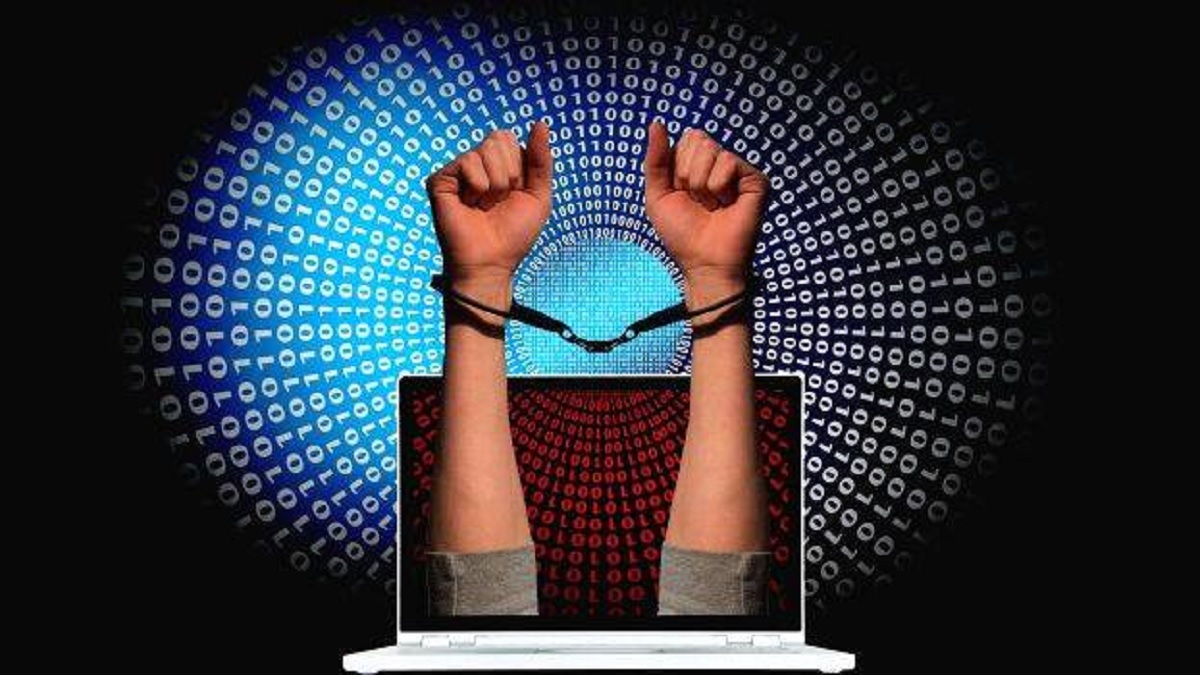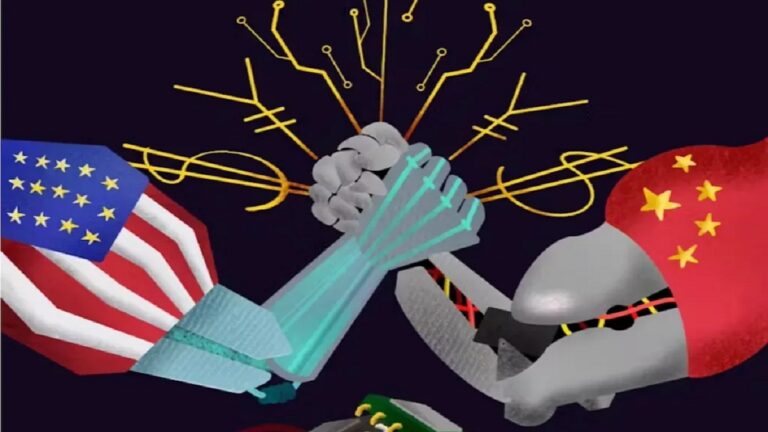हर युग की सत्ता अपने समय की सबसे ताकतवर तकनीक को हथियार बनाकर जनता पर शासन करती है। पहले यह ताकत तलवार थी, फिर बंदूक हुई, फिर मीडिया बनी, और अब यह डेटा है। आधुनिक सत्ता अब सिर्फ आपकी देह पर शासन नहीं करती, आपकी चेतना को भी नियंत्रित करती है। वह यह नहीं चाहती कि आप केवल उसके आदेश मानें-वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आप सोच ही न सकें।
जिस क्षण आपकी सोच भविष्य के किसी संभावित विरोध की गंध देने लगती है, उसी क्षण सत्ता आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है-चुपचाप, अदृश्य, लेकिन बेहद सटीक निशाने के साथ। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका अधिकार, आपका वोट, आपकी आवाज, आपके ही डेटा की मदद से आपसे छीन लिया गया।
आज के डेटा युग में आपकी हर हरकत पर सरकार की नजर है-आप क्या सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं, किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, क्या खरीदते हैं, किसे वोट देने वाले हैं-यह सब सरकार को पहले से पता होता है। आपको पता भी नहीं चलता और आपके बारे में एक-एक जानकारी जमा हो रही होती है।
मोबाइल, इंटरनेट, बैंक, आधार कार्ड, राशन कार्ड, और सोशल मीडिया-ये सब मिलकर आपकी पूरी जिंदगी सरकार की निगरानी में ला चुके हैं। अब सरकार को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप क्या सोचते हैं, वह आपके डेटा से खुद जान लेती है।
जब आप कोई पोस्ट लाइक करते हैं, कोई खबर पढ़ते हैं, किसी नेता के बारे में अच्छा या बुरा कमेंट करते हैं, जब आप व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कोई वीडियो या मैसेज फॉरवर्ड करते हैं-ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। आप जिस दुकान से रोज़ाना सामान खरीदते हैं, जो पेट्रोल पंप इस्तेमाल करते हैं, जिस इलाके में जाते हैं, जिस स्कूल में बच्चों का नामांकन कराते हैं-सरकार के पास इन सबका डिजिटल रिकॉर्ड होता है। आपने कौन-सी फिल्म देखी, कौन-सा ऐप डाउनलोड किया, कितनी देर तक मोबाइल पर एक्टिव रहे, कौन-से नंबर पर ज्यादा बात की-ये सब भी सरकार के पास दर्ज हो रहा है।
अब जो विरोध करेगा, सरकार उसे चुप कराने के लिए लाठी या गोली का सहारा नहीं लेगी- पहले वो उसका डेटा पढ़ेगी। जिस तरह से आप अपने स्मार्टफोन में हर दिन कुछ न कुछ खोजते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट लाइक करते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, उससे आपकी सोच, आपकी पसंद, आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी राजनीतिक विचारधारा का पूरा नक्शा तैयार हो जाता है। अब सरकार इस नक्शे को इस्तेमाल करेगी।
जब आप किसी धरने या प्रदर्शन में जाएंगे, तो आपके फोन के ज़रिए यह पता लग जाएगा कि आप किसके समर्थक हैं, किस बात के विरोध में आए हैं और किस सोशल नेटवर्क से जुड़े हैं। यह भी पता चलेगा कि आप कोई नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, या बस सहानुभूति रखने वाले आम नागरिक।
और सिर्फ इतना ही नहीं-आपका फोन, आपकी जेब में रखा हुआ छोटा सा उपकरण, यह भी बता देगा कि आप कितनी आमदनी वाले हैं, आपके पास महंगा फोन है या सस्ता, आपने ऑनलाइन कितने महंगे प्रोडक्ट मंगवाए हैं, महीने में कितनी बार पेट्रोल भरवाते हैं, आप बिजली का कितना बिल भरते हैं- यानी सरकार को यह भी पता होता है कि आपके खिलाफ सख्ती करनी है या आपको फुसलाना है। एक बटन दबाकर सरकार यह तय कर सकती है कि किस धरने में किसे पकड़ना है, किसे डराना है और किसे ‘मैनेज’ करना है। विरोध की संभावना को डेटा में बदलकर सरकार पहले ही उसका उपाय तय कर लेगी।
अब सोचिए, जब चुनाव आते हैं, तो सरकार के पास एक बहुत बड़ा डेटा बैंक होता है जिसमें वह देखती है कि कौन लोग सरकार के समर्थक हैं और कौन विरोधी। और फिर क्या होता है? चुन-चुन कर उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाते हैं जो सरकार के खिलाफ माने जा रहे हैं। कोई नोटिस नहीं, कोई खबर नहीं-आप वोट डालने जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका नाम लिस्ट में तो है ही नहीं।
चुनाव आयोग कहता है कि यह गलती से हुआ, लेकिन जब लाखों लोगों के नाम एक ही पैटर्न में कटते हैं-यानी गरीब, पढ़े-लिखे, विपक्ष समर्थक, जातियों और धर्मों के आधार पर अलग-अलग इलाके में-तो ये महज़ गलती नहीं लगती, ये साज़िश लगती है। और इसके पीछे जो तकनीक है, वह बिल्कुल चुपचाप और चालाकी से काम करती है। फेस रिकॉग्निशन अर्थात् चेहरे से पहचान, आधार से लिंकिंग, मोबाइल नंबर से आपकी गतिविधि का पता लगाना-ये सब आज की सरकार के लिए बहुत आसान है।
पहले सरकारें जनता से डरती थीं, अब सरकारें जनता की सोच को पहले ही जानकर उससे निपटने लगी हैं। जिसको वोट देने से वो डरती है, उसका नाम पहले ही लिस्ट से गायब कर देती है। जिसको विरोध करने का डर है, उस पर नजर रखती है। और ये सब कानून के नाम पर होता है-कि ‘डेटा सिक्योरिटी’ है, ‘आधार जरूरी है’, ‘डिजिटल इंडिया’ है। लेकिन असल में यह डिजिटल कंट्रोल है-यानी जनता पर डिजिटल ताला।
भारत में आधार को शुरू में कल्याणकारी परियोजना के रूप में पेश किया गया था-ऐसा यूनिक नंबर जो हर नागरिक को सरकारी सेवाओं और सब्सिडी तक आसान पहुंच देगा। लेकिन धीरे-धीरे यह पहचान पत्र से आगे बढ़कर निगरानी और नियंत्रण का औजार बन गया। आज आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा है, मोबाइल नंबर से जुड़ा है, राशन कार्ड से जुड़ा है, पेंशन, स्कॉलरशिप, टैक्स, अस्पताल, स्कूल, यात्रा-हर जगह आधार अनिवार्य बना दिया गया है।
यहां तक कि मौत के बाद शवदाहगृह में अंतिम संस्कार के लिए भी कई जगह आधार मांगा जाने लगा है। जब एक नंबर से आपकी पूरी जिंदगी जुड़ जाए, तो सरकार को आपकी हर गतिविधि का ब्योरा मिल जाता है-आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, कितना खर्च कर रहे हैं-और यह सब बिना आपके बताए।
आधार डेटा के इस केंद्रीकरण ने नागरिकों को बेहद असुरक्षित बना दिया है। आधार डेटा लीक की घटनाएं बार-बार सामने आई हैं। अखबारों और वेबसाइटों पर खुलेआम लोगों की आधार जानकारी, मोबाइल नंबर, बैंक खातों की जानकारी तक दिखाई दी है। लेकिन न सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और न ही सुप्रीम कोर्ट का बहुमत इसके खिलाफ खड़ा हुआ। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आधार के खिलाफ ऐतिहासिक असहमति दर्ज की थी।
उन्होंने कहा था कि आधार नागरिकों की निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन है और इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा था कि आधार डेटा को नष्ट करके समुद्र में फिंकवा देना चाहिए ताकि इसे फिर कभी इस्तेमाल न किया जा सके।
लेकिन दुर्भाग्य से न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ उस समय बहुमत में नहीं थे। बाकी जजों ने आधार को संविधान सम्मत मानते हुए वैध करार दे दिया, हालांकि कुछ सीमाओं के साथ। यह निर्णय अपने आप में विरोधाभासी था-एक तरफ निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया, और दूसरी तरफ आधार को, जो उसी निजता का अतिक्रमण करता है, वैध बता दिया गया।
बाद में जब पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ तब मुख्य न्यायाधीश बन चुके थे। लेकिन उन्होंने भी इस मामले को फिर से सुनने या उस पर कोई कड़ा कदम उठाने का साहस नहीं दिखाया। यह विडंबना है कि जिन्होंने आधार के खिलाफ सबसे कड़ा विरोध दर्ज किया था, वे ही बाद में पूरी तरह मौन रह गए।
आधार अब भारत में अदृश्य हथियार बन चुका है, जो नागरिकों की पहचान को उनके अधिकारों से जोड़कर उन्हें नियंत्रित करने का काम कर रहा है। जो लोग आधार नहीं बनवाते या जिनका आधार किसी कारण से निष्क्रिय हो जाता है, वे कई बार राशन, इलाज, पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। यहां तक कि आदिवासी इलाकों में भूख से मौत की खबरें भी सामने आई हैं क्योंकि अंगूठा नहीं मिला या इंटरनेट नहीं चला।
इसका मतलब यह है कि अब एक मशीन और एक डेटाबेस यह तय कर रहा है कि आप जिंदा रहने के लायक हैं या नहीं। आज जब हम एक सर्विलांस स्टेट में तब्दील हो चुके हैं, तब शायद हमें समझ आ रहा होगा कि उस डेटा को समुद्र में फेंकना क्यों ज़रूरी था।
आप सोचिए-आज आपकी पूरी जिंदगी एक स्क्रीन में समा चुकी है, और सरकार उस स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठी है, सब देख रही है। आप रात में क्या गूगल कर रहे हैं, सुबह कौन-से बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, दोपहर में किससे चैट कर रहे हैं, शाम को कौन-सी पार्टी की मीटिंग में जा रहे हैं-सरकार को सब पता है। और जब उसे लगे कि आप उसकी राह का कांटा बन सकते हैं, तो वह आपको लोकतंत्र की प्रक्रिया से बाहर कर देती है।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि सर्विलांस स्टेट बन चुका है-यानी निगरानी वाला देश। यहां अब आपकी नागरिकता आपके आधार कार्ड या वोटर आईडी से नहीं, आपके डेटा से तय होती है। और जब यह तय हो जाए कि आप सरकार के काम नहीं आ सकते, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाता है-बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए।
ये खतरा बहुत गहरा है, और ये चुपचाप हमारे लोकतंत्र को निगल रहा है। अगर आज हम चुप रहे, तो कल हमारे बच्चों को यह भी नहीं पता चलेगा कि उन्हें कभी वोट देने का अधिकार था भी या नहीं। यह लड़ाई अब सिर्फ वोट की नहीं, सोच की है-और यह सोच को बचाने की लड़ाई है, तकनीक के ज़रिए खत्म की जा रही आज़ादी के खिलाफ।
इस तरह हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हमारी पहचान महज़ एक नंबर है, और आज़ादी सिर्फ भ्रम। जिन हाथों ने तकनीक को प्रगति के दीपक की तरह जलाया था, उन्हीं हाथों ने उसे निगरानी का अग्निकुंड बना दिया है । अब हमारी हर सांस रिकॉर्ड है, हमारा हर कदम रजिस्टर में दर्ज है। यह ऐसा युग है जहाँ समुद्र की लहरों की तरह बहते विचारों को डेटा सेंटर की दीवारों में क़ैद कर दिया गया है।
(मनोज अभिज्ञान स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)