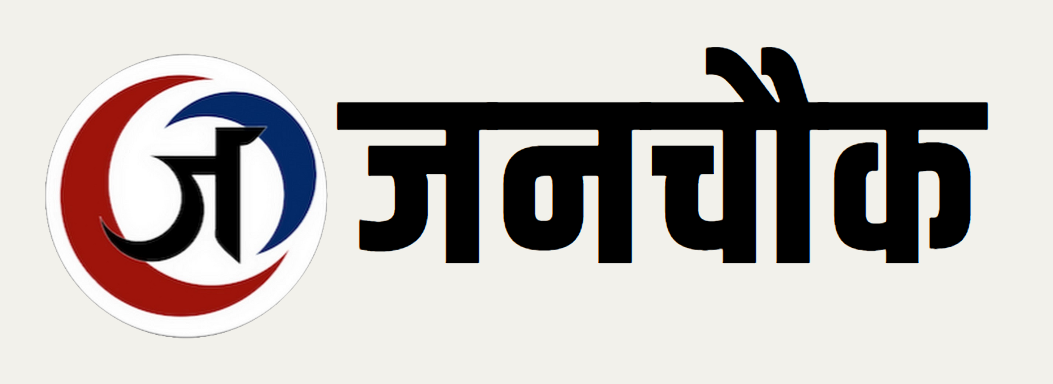लगभग एक दर्जन राज्यसभा सांसदों को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन सदन से निलंबित कर दिया गया। इन सदस्यों को अगस्त में मानसून सत्र के अंत में उनके आचरण के लिए निलंबित कर दिया गया था। सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 के पारित होने के दौरान इन विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन के वेल में हंगामा करने के बाद उस समय मार्शलों को बुलाना पड़ा था। लेकिन इसके बाद एक और घटना घटी कि सदन में राज्यसभा में, संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। यह संविधान के उद्देशिका, प्रिएम्बल को संशोधित करने के बारे में था। पर हंगामा हुआ और फिर सन्नाटा। इस तरह का महत्वपूर्ण बिल बिना जनचर्चा और सभी दलों से बातचीत के बिना लाया जाना, यह दर्शाता है कि, सरकार और सत्तारूढ़ दल के मन में संविधान, संसद और संसदीय परम्पराओं को लेकर कितना सम्मान है। मैं संशोधन के गुणदोष पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की लोकतांत्रिक शैली और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति दायित्वबोध की बात कर रहा हूँ।
2014 के बाद, अगर संवैधानिक संस्थाओं की कार्यक्षमता की ऑडिटिंग या समीक्षा की जाय तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि अधिकतर संवैधानिक संस्थायें, धीरे धीरे या तो अपने उद्देश्य से विचलित हो रही हैं या उनकी स्वायत्तता पर ग्रहण लग रहा है या उन्हें सरकार या यूं कहें प्रधानमंत्री के परोक्ष नियंत्रण में खींच कर लाने की कोशिश की जा रही है। संविधान का चेक और बैलेंस तंत्र जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच एक महीन सन्तुलन बनाये रखता है को भी विचलित करने की कोशिश की जा रही है।
मैं उन संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो कार्यपालिका के सीधे नियंत्रण में थोड़ी बहुत फंक्शनल स्वायत्तता के साथ, गठित की गयी हैं, बल्कि उन संस्थाओं की बात कर रहा हूँ जो सीधे तौर पर संविधान में अलग और विशिष्ट दर्जा प्राप्त हैं और जिनके अफसरों की नियुक्ति में सरकार यानी कार्यपालिका का दखल भी सीमित है, यानी सरकार उनकी नियुक्ति तो कर सकती है, पर बिना एक जटिल प्रक्रिया के उन्हें हटा नहीँ सकती है। उदाहरण के लिये, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कम्पट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जैसे कुछ अन्य संस्थाएं हैं।
पर एक और संवैधानिक संस्था है जो संसदीय लोकतंत्र की मातृ संस्था है, भारतीय संसद, उसकी भी गरिमा पिछले 7 साल में गिरी है और उसे भी सत्तारूढ़ दल के दलगत एजेंडे के अनुसार, हांकने का षड्यंत्र किया गया है। अफ़सोफ कि संसद के दोनों सदनों के सभापति, या स्पीकर या उपसभापति, भी अपने सदन जिनकी वे अध्यक्षता करते हैं, का मान मर्दन होते देखते रहे। वे अपने दलीय हित के पाश से मुक्त होकर संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वाह करने में विफल रहे। प्रोटोकॉल और सदन में हैसियत रखते हुये भी वे कभी कभी तो, सरकार के एक एक्सटेंशन के रूप में परिवर्तित नज़र आये।
इस पतन का सबसे बड़ा प्रमाण है, राज्यसभा में बिना किसी चर्चा और मत विभाजन के, तीनों किसान कानूनों का पास कर दिया जाना और फिर बिना किसी चर्चा और मतविभाजन के उन्ही पास किये गए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना। सरकार के यह दोनों कृत्य, आगे आने वाले समय मे संसदीय इतिहास के छात्रों के लिये सबक बनेंगे कि कैसे और क्यों यह लाये गए थे और कैसे और क्यों यह वापस ले लिए गए। न लाते समय सदन में सदन में विशद चर्चा हुयी और न उन कानूनों के तशरीफ़ ले जाते समय कोई बात हुयी। बिल्कुल एक शेर की तरह कि, आये भी वो, गए भी गए वो, खत्म हुआ फसाना सारा !
पर क़ायदे क़ानून, कोई दास्तान ए इश्क़ तो है नही कि सारा फसाना खत्म मान ही लिया जाय। पर एक साल में, पारित होने और निरस्त होने के बीच इन तीन किसान बिलों ने देश को सरकार और प्रधानमंत्री की प्रशासनिक क्षमता, राजनैतिक कुशलता, सत्तारूढ़ दल की आर्थिक नीतियों के खोखलेपन, जनता के सड़क पर अपने अधिकारों के लिये उतर कर संघर्ष करने की जिजीविषा को उजागर कर दिया। सरकार इन कानूनों को लेकर न केवल एक्सपोज हुयी बल्कि यह भी लगा कि, सरकार न तो कानून ड्राफ्ट करना जानती है, न उसके सांसदों को पेश किए जाने वाले बिल के बारे में पता है, न ही वे इस बात के लिए भी, तैयार थे कि इस पर बहस होगी, न ही सरकार ने कोई ऐसा होमवर्क किया था कि, तीनों कानूनों का क्या दूरगामी असर देश की कृषि संस्कृति पर पड़ेगा।
सत्तापक्ष जिसे सदन में ट्रेजरी बेंच कहते हैं, क्योंकि उनके पास राजकोष रहता है, तो यह मान के बैठा था कि मोदी जी, यह कानून लाये हैं तो कुछ सोच के ही लाये होंगे, और मोदी हैं तो मुमकिन है की, तर्ज पर वे यह कानून पास करा ही लेंगे और उनका यह सोचना गलत था भी नहीं। मोदी जी भी यह तीनों कानून ‘कुछ’ सोच कर ही लाये थे, और उन्होंने इसे पास भी करा लिया। पर दुर्भाग्य यह रहा कि, राज्यसभा के उपसभापति जब कानून पास हो रहा था तब, सदन के अध्यक्ष के रूप में बैठे तो थे पर उनका आचरण, एक आदेशपालक की तरह लग रहा था। लगता था, वे एक ऐसे आदेश का पालन करने के लिये संकल्पित हैं, जिन्हें वे छोड़ नहीं सकते। राज्यसभा की कार्यवाही का वीडियो जिन्होंने देखा होगा, वे मेरी बात समझ सकते हैं। राज्यसभा के लिये वह, एक काला दिन था। उस कालिमा के लिये सरकार से अधिक, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जिम्मेदार हैं, जिन्होंने संसदीय परंपरा और मर्यादा को बनाये रखने के बजाय खुद ही उसे बिखर जाने दिया। यह शर्मनाक था।
कृषि कानून अब अस्तित्वहीन हैं और उसके प्राविधान पर चर्चा करने का अब कोई औचित्य भी नहीं है, पर संसद में जिस तरह से पिछले सात सालों में सरकार ने कुछ कानून बनाये हैं और उन पर न तो विशद चर्चा हुई और न ही नियमानुसार मत विभाजन हुआ, की प्रवृत्ति जो एक तरह से, संसद की अवहेलना ही है पर चर्चा करना ज़रूरी है। संसद में कानून कैसे बनता है, इस पर एक नज़र डालते हैं।
कानून बनाने के लिये, उसे विधेयक के रूप में, संसद के किसी एक सदन में सरकार या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। मोटे तौर पर, विधेयक दो प्रकार के होते हैं:
(क) सरकारी विधेयक और
(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक।
विधेयक का मसौदा उस विषय से संबंधित सरकार के मंत्रालय में विधि मंत्रालय की सहायता से तैयार किया जाता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद इसे संसद के सामने लाया जाता है। संबंधित मंत्री द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। केवल वित्त विधेयक के मामले में यह पाबंदी है कि, वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता।
कानून बनने के पहले, प्रत्येक विधेयक के प्रत्येक सदन में तीन वाचन होते हैं।
● विधेयक ‘पेश करना,’ विधेयक का पहला वाचन है। इस स्तर पर चर्चा नहीं की जाती है।
● विधेयक का दूसरा वाचन सबसे अधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि इसी अवस्था में इसकी विस्तृत एवं बारीकी से जांच और चर्चा की जाती है।
● जब विधेयक के सभी खंडों पर और अनुसूचियों पर, यदि कोई हों, सदन विचार कर उन्हें स्वीकृत कर लेता है। तब मंत्री यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को पास किया जाए। यह तीसरा वाचन कहलाता है।
जिस सदन में विधेयक पेश किया गया हो उसमें पास किए जाने के बाद उसे सहमति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहाँ विधेयक फिर इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है।
किसी विधेयक पर दोनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध होने पर एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसका समाधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। जब दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक अलग अलग या संयुक्त बैठक में पास कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देता है तो अनुमति की तिथि से विधेयक अधिनियम बन जाता है।
संशोधन के द्वारा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बदलाव लाया जा सकता है। किंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान के मूल ढांचे या मूल तत्वों को नष्ट या न्यून करने वाला कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
संसद के कार्यों में विविधता के साथ कार्य व्यस्तता भी रहती है। चूंकि समय सीमित होता है, इसलिए संसद के समक्ष प्रस्तुत सभी विधायी या अन्य मामलों पर गहन विचार नहीं हो पाता है। इसलिए, अतिरिक्त विधायी कार्य संसदीय समितियों द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों की समितियों की संरचना कुछ अपवादों को छोड़कर एक जैसी होती है। यह संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के तहत अधिनियमित होती है। सामान्यत: ये दो प्रकार की होती हैं।
● स्थायी समितियां, जो प्रतिवर्ष या समय-समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं। इनका कार्य कमोबेश निरंतर चलता रहता है।
● तदर्थ समितियां, जिनकी नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है तथा अपना काम पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट पेश कर देने के बाद ये समाप्त हो जाती हैं।
विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की स्थापना संसद ने 1993 में की थी। वर्तमान में विभागों एवं मंत्रालयों से जुड़ी हुई इस प्रकार की 24 समितियां हैं। प्रत्येक कमेटी में 31 सदस्य होते हैं। इनमें से 21 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा से होते हैं। संसद में दलों की सदस्य संख्या के हिसाब से उनको इस कमेटी में सदस्यता दी जाती है। कानून बनने वाले बिल पर स्थायी समिति विचार करती है। इसके लिए आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। समिति मसले से जुड़े विशेषज्ञों की राय जानने के लिए उनको आमंत्रित भी कर सकती है। इस प्रकार समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती है इसे सदन के पटल पर रखा जाता है।
संसदीय समिति की अनुशंसा, सदन में मान ही ली जाय, तरह की कोई बाध्यता नहीं होती। कमेटी का गठन तो इसलिए किया जाता है कि सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वह सभी बिलों पर विस्तार से चर्चा करे और सभी बिलों के लिए जनता की राय भी ले। सभी बिल समिति के पास भेजे भी नहीं जाते हैं। लेकिन अधिकांश बिल इसके पास भेजे जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब कोई बिल बगैर समिति के पास गए ही पारित हुए।
स्थायी समिति छोटी संसद की तरह है, जो दलगत राजनीति से ऊपर मुद्दों को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखती है। इसमें विभिन्न विचारों पर चर्चा की जाती है और फिर यह लोगों के हित में सिफारिशें देती है। संसद में मुद्दे ज्यादा होते हैं। समय कम। हर पहलू पर व्यापक चर्चा नहीं हो सकती। वह काम संसदीय समिति करती है। इसमें छोटी सी छोटी बातों पर चर्चा होती है और उस हिसाब से मसविदा तैयार किया जाता है। संसद सत्र आमतौर पर लगभग सौ दिन ही चलता है, जबकि ये समितियां हमेशा काम करती रहती हैं।
ब्रिटेन और अमेरिका में भी इस तरह की समितियों की व्यवस्था है। सदन में किसी सदस्य को जो कर्त्तव्य, दायित्व और विशेषाधिकार मिला हुआ है वहीं स्थायी सदस्य के रूप में भी उसे प्राप्त है। स्थायी समिति के कार्यक्षेत्र में न्यायपालिका भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। स्थायी समितियों की व्यवस्था इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि यह सरकार की योजनाओं को देखने का काम करती है कि उन्हें जनता के हित में चलाना उपयोगी है या नहीं। सरकार कानून बनाने के लिए कोई विधेयक सदन में लाती है तो उन पर समाज के हर तबके को मौका देकर उनकी राय लेना और उसके आधार पर एक सुसंगत रिपोर्ट देना समिति का प्रमुख दायित्व है। भले ही सरकार उसकी रिपोर्ट को विधेयक के प्रारूप में शामिल करे या इसे खारिज कर दे।
2014 के बाद सरकार ने कुछ ऐसे क़ानून बनाये हैं जिनके बारे में संसद में चर्चा हुयी ही नहीं है और न ही उन संसदीय नियमो का पालन किया गया है जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है। उदाहरण के लिये, नोटबन्दी, अनुच्छेद 370 में संशोधन, नागरिकता संशोधन विधेयक, और सबसे महत्वपूर्ण यह तीन किसान कानून थे। हर सत्तारूढ़ दल को अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू और चुनावी वादे को पूरा करने का अधिकार है, क्योंकि उसे बहुमत जनता ने दिया है, पर वे वादे उन्ही संसदीय परंपराओं और कायदे कानून की राह से ही लागू होंगे न कि एक स्वेच्छाचारी शासक की भ्रू भंगिमा के अनुसार।
उपरोक्त वर्णित सभी कानून, बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनका असर व्यापक है, पर न तो वे संसदीय समिति में गए, न उनके एक्सपर्ट से राय मशविरा लिया गया, न ही जनता के बीच तमाम माध्यमों से चर्चा की गयी, बस सदन में आएस बोलवा कर उन्हें पारित कर दिया गया। यह कानून बनाना नहीं, कानून थोपना हुआ। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इन कानूनों का प्रबल विरोध हुआ और कानून, या तो वापस लेने पड़े या वे नियमावली न बनने के कारण लागू नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह धड़ाधड़ कानून बनाने और विधेयक पारित करने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने, तंज करते हुए कहा था, कि कानून चाट पकौड़ी की तरह बनाये जा रहे हैं।
ऐसे कानूनों का क्या परिणाम हो सकता है, यह एक साल से चल रहे किसान आंदोलन ने बता दिया है। यह आंदोलन सरकार की स्वेच्छाचारिता, ज़िद, अहंकार के खिलाफ भी था, कानून और कृषि नीति के खिलाफ तो था ही। चोरी चोरी कानून बनाना, और चुपके चुपके वापस ले लेना, यह सरकार की एकाधिकारवादी कार्यशैली को प्रमाणित करता है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री का पद इतना अधिक शक्ति केंद्रित होता चला जा रहा है कि संविधान में शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पॉवर, बहस, चर्चा, कैबिनेट की अवधारणा, जन संवाद आदि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जा रही है। जबकि हमने वेस्ट मिनिस्टर मॉडल की जो संसदीय व्यवस्था चुनी है उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट का बॉस नहीं बल्कि सभी बराबरों मे प्रथम होता है। पर आज वह स्थिति नहीं है।
यह स्थिति 2014 के बाद ही बननी शुरू हो गयी थी, और इस पर टिप्पणी करते हुए अरुण शौरी ने कहा भी था कि यह ढाई लोगों की सरकार है। यह तंज नरेंद्र मोदी, अमित शाह को दो और अरुण जेटली को आधा मानते हुए किया गया था। अब तो यह दो की ही सरकार कही और मानी जाने लगी है। इसका आशय यह है कि संसद में चर्चा और बहस तो अलग बात है, पर, क्या कैबिनेट में भी इन कानूनों की मेरिट पर खुल कर चर्चा हुयी थी इस पर भी संशय है। याद कीजिए, नोटबन्दी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले के बारे में संसद में भी विपक्ष ने यह संदेह व्यक्त किया था कि, इसका निर्णय लेते समय वित्तमंत्री से कोई चर्चा नहीं की गयी थी। आज नोटबन्दी एक विफल ही नहीं बल्कि वह एक ऐसा आत्मघाती वित्तीय कदम सिद्ध हुआ है कि, देश की अर्थव्यवस्था आज तक उबर नहीं पा रही है।
हम सबको सुनिश्चित करना होगा कि, संसद सर्वोच्च है, यह पवित्र वाक्य, कहीं जुमलों की भीड़ में एक जुमले की शक्ल न अख्तियार कर ले। प्रधानमंत्री, सरकार के प्रमुख हैं और उन्हें सरकार चलाने के लिये जनता ने चुना है, पर वे निरंकुश नहीं हैं और न ही उनके समर्थकों को ऐसा सोचना भी चाहिए। पर इधर जिस तरह से सुरक्षा के नाम पर संसद में उनके आने के समय, सांसदों को रोका जा रहा है, सदन में व्यवधान पहुंचाने के नाम सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, उनसे संवाद तक नहीं किया जा रहा है, सदन के पीठासीन अध्यक्ष, विशेषकर राज्यसभा के उपसभापति का आचरण, सरकार के एक आज्ञापालक यस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की तर्ज पर होता जा रहा है, उससे न तो प्रधानमंत्री की छवि अच्छी बन रही है और न ही संसद की गरिमा बढ़ रही है। इससे देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्था का महत्व घटाया जा रहा है और राज्यसभा की गरिमा को जितनी चोट उसके सभापति और उपसभापति ने पहुंचाई है, वह दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।
हमे एक सजग, सचेत और सतर्क नागरिक की तरह अपने अधिकारों और दायित्व को याद रखते हुए, देश के संविधान के अनुसार, सत्ता के हर उस कदम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर, एकाधिकारवादी शक्ति केंद्रित सत्ता केंद्र की ओर ले जाती है। किसान आंदोलन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने जनता के जनार्दन रूप को सामने ला दिया और सत्ता का अहंकार ध्वस्त कर दिया। संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण, देश के लिये घातक है।
( विजय शंकर सिंह रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं और आजकल कानपुर में रहते हैं।)