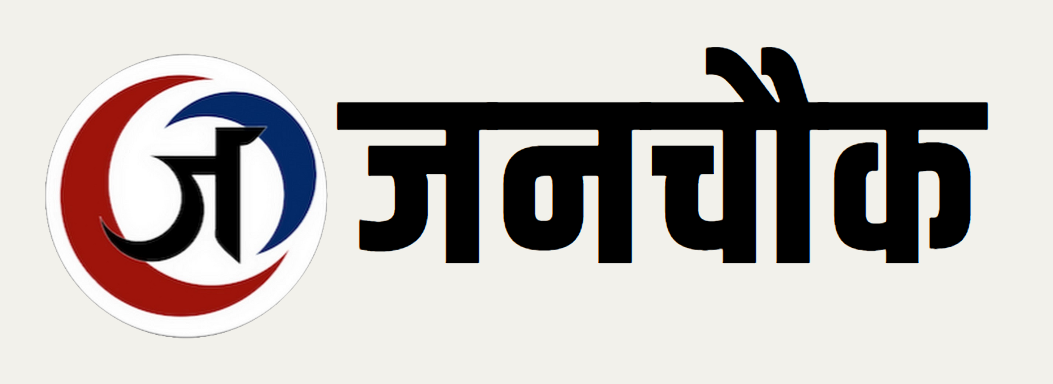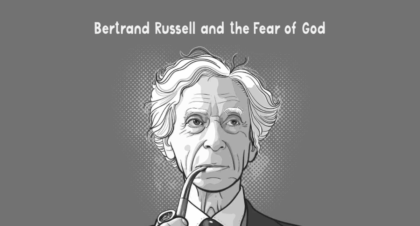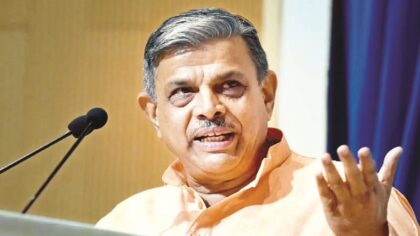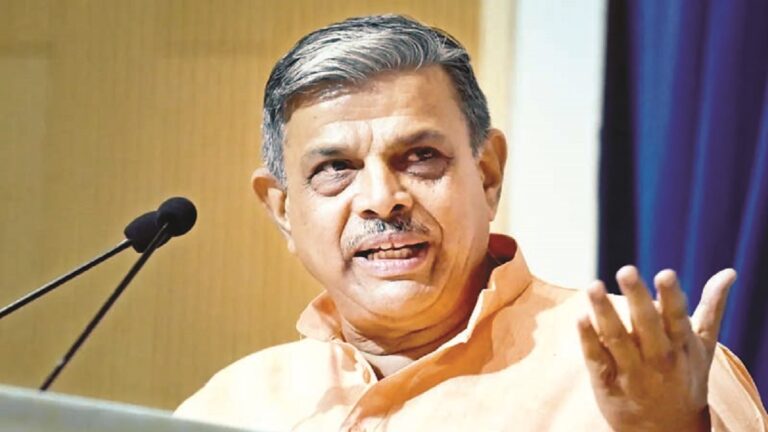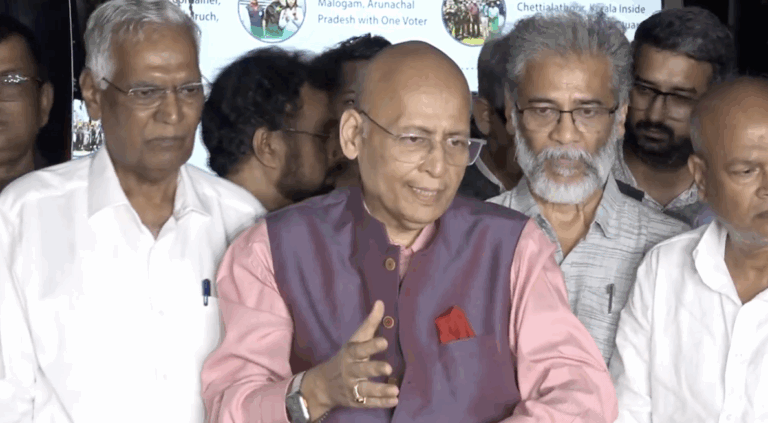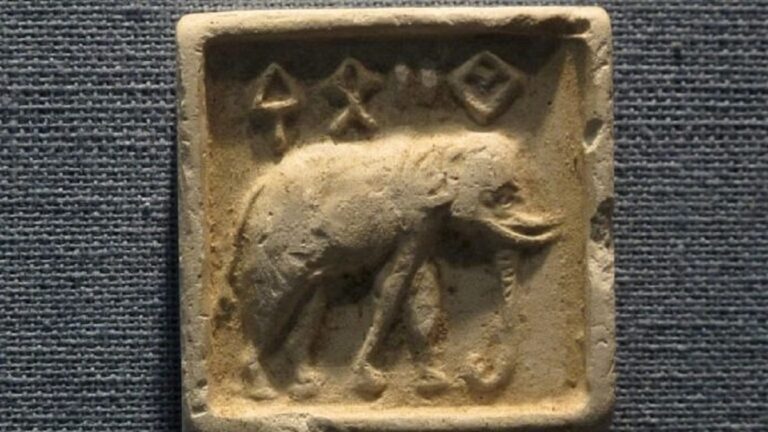जनचौक पर बीते 26 जून को परमजीत बॉबी का एक लेख छपा, ‘आपातकाल: तथ्य और भ्रांतियां’। वे लिखते हैं: “आपातकाल भी एक संवैधानिक प्रावधान है, जिसका उपयोग उपरोक्त विषम परिस्थितियों में किया जा सकता है, अर्थात् आपातकाल संविधान की हत्या कदापि नहीं है।” कुछ ऐसी ही बात 25 जून के पॉडकास्ट ‘अंबेडकरनामा’ में थी, जिसका शीर्षक था: “किसी के लिए होगा ‘आपातकाल’, लेकिन दलितों के लिए स्वर्णकाल था: चंद्रभान प्रसाद”। इसके साथ एक और शीर्षक था: “दलित उत्थान और सामंती पूंजीपति शक्तियों के विद्रोह को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने लगाई इमरजेंसी”। होस्ट प्रो. रतनलाल ने चंद्रभान प्रसाद के साथ बातचीत में मुख्यतः आपातकाल को दलित परिप्रेक्ष्य से देखने पर जोर दिया।
आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सरकारी और गैर-सरकारी विज्ञापनों तथा लेखों की बाढ़ आ गई। आपातकाल के समय सबसे मुखर माना जाने वाला अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने तो पुराने दिनों के लेख, उनसे जुड़े संस्मरण, घटनाओं से संबंधित बातें और कई तरह के रिपोर्ताज का अंबार लगा दिया। इनमें मुख्य बात यही थी कि आपातकाल संविधान और लोकतंत्र की हत्या थी।
इस पूरे मसले पर कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस पहले भी इसे गलती मान चुकी है, लेकिन यह गलती किस प्रकार की थी, इस संबंध में कभी स्पष्टता सामने नहीं आई। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने सिख समुदाय के नरसंहार पर अतीत में हुई गलती को स्वीकार किया था और उनके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी।
जब उस आपातकाल की बात हो रही है, तो वर्तमान में चल रहे ‘आपातकाल’ के बारे में भी अब खुलकर चर्चा होने लगी है। बातचीत में सारा मसला ‘परिप्रेक्ष्य’ का बनता हुआ दिख रहा है। इस घोषित और अघोषित आपातकाल को कैसे देखा जाए? कानूनी और विधायी नजरिए से आपातकाल एक संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है, जो राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार देता है। और, इंदिरा गांधी ने इसका प्रयोग किया। परमजीत बॉबी के शब्दों में, यह डॉ. आंबेडकर द्वारा दिया गया प्रावधान है। इसलिए यह असंवैधानिक नहीं है।
आपातकाल बनाम आपातकाल: यह आसान-सा दिखने वाला तर्क उतना सरल नहीं है, जितना प्रतीत होता है। इंदिरा गांधी के समय में संविधान में इतने संशोधन किए गए कि मूल संविधान में एक और छोटा-सा संविधान ही जुड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे मोदी-शाह के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार ने किया है। इस काल में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था ही संशोधनों की भेंट चढ़ती दिख रही है। यह सारा काम संविधान के दायरे में रहकर करने के दावे के साथ किया जा रहा है। हालांकि, न्यायपालिका ने सीमित सक्रियता के साथ इसके कुछ प्रावधान Nodify: प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
यह सवाल जरूर है कि आपातकाल को कैसे देखा जाए? संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाएं किसी राज्य के लिए होती हैं। ये व्यवस्थाएं राज्य को चलाने के साथ-साथ उसे बचाए रखने के लिए भी वैधानिक प्रावधान करती हैं। अर्थात्, यह मानकर चलती हैं कि यह व्यवस्था भविष्य में टूट और बिखर भी सकती है। ऐसे में, आपातकालीन परिस्थितियों की परिकल्पना के आधार पर राज्य को आपातकालीन वैधानिक व्यवस्थाएं भी प्रदान की जाती हैं।
भारत में संविधान के निर्माण के समय भारतीय राज्य उपनिवेशिक मानचित्र के हिसाब से नहीं बन रहा था; वह टूट चुका था। उस उपनिवेशिक दौर में कई ऐसे राज्य उभरकर आए थे, जो नए बन रहे राज्यों का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे। 15 अगस्त 1947 के बाद, संविधान निर्माण के समय तक जो प्रावधान बनाए जा रहे थे, उनमें राज्य का राजनीतिक मानचित्र, इसका आर्थिक-सामाजिक प्रबंधन, और राज्य को निर्णय लेने की क्षमता पर अधिक जोर दिया गया था।
मुख्य बात थी राज्य को एक केंद्रीभूत निर्णयकारी संस्था के रूप में विकसित करना, जो अंतर्विरोधों के ऊपर खड़ा होकर उन्हें नियंत्रित कर सके। भारत का पहला संवैधानिक संशोधन इसी नियंत्रण को स्थापित करने के लिए आया था। और, आज भी राज्य को एक नियंत्रणकारी संस्था में ढालने की सारी कवायदें पूरी हो रही हैं।
आपातकाल राज्य को एक नियंत्रणकारी संस्था बनने का अवसर प्रदान करता है, खासकर तब जब राजनीतिक बर्चस्व टूट रहा हो और यह सवाल खड़ा हो कि राज्य पर किसी राजनीतिक समूह का नियंत्रण हो। इस तरह, आपातकाल राजनीतिक समूहों के बीच की टकराहट को भी अभिव्यक्त करता है। राजनीतिक समूहों से निपटने के लिए जरूरी होता है कि उनकी गतिविधियों के अधिकार छीन लिए जाएं। यह छीनने का प्रावधान दो तरह से हो सकता है।
पहला, किसी संगठन, पार्टी, समूह, या व्यक्ति को प्रतिबंधित कर दिया जाए और उसके अस्तित्व को ही अवैध घोषित कर दिया जाए। दूसरा, सामान्य नागरिक अधिकारों को ही समाप्त कर दिया जाए। इन दोनों ही मसलों में राज्य के भीतर के अंतर्विरोध और राजनीतिक क्षमता एक मुख्य पक्ष होता है। ऐसे में, नियंत्रणकारी समूह अंतर्विरोधों का फायदा उठाने के लिए अपने समर्थक समूहों को खुली छूट देता है और साथ ही नए समूहों को सुविधाएं प्रदान करता है। इंदिरा गांधी ने ठीक यही किया। कुछ समूहों को अपने पक्ष में किया, अपने समर्थक समूहों को खुली छूट दी, और कई समूहों को पक्षहीन बने रहने के लिए विवश किया।
लेकिन सवाल यही है कि उस समय राज्य के सामने ऐसी क्या चुनौती थी, जिससे राज्य के बने रहने पर ही सवाल खड़ा हो गया था? आज भी यह बहस का विषय बना हुआ है। 1970 तक भारत का सामंतवाद प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर संवैधानिक संरचना के साथ समाहित हो चुका था और उस पर वर्चस्व हासिल कर चुका था।
इस समय तक भारत का राजनीतिक मानचित्र भी लगभग पूरा बन चुका था। राज्यों में नई तरह की सरकारों के साथ सामंजस्य भी स्थापित हो चुका था। आरएसएस कांग्रेस का हिस्सा बनकर काम करने की विवशता में फंसा हुआ था। महाराष्ट्र में दलित आंदोलन और बंगाल में नक्सलबाड़ी ही ऐसी दो धाराएं थीं, जिन्होंने उस समय की राज्य व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनका भयावह दमन हुआ और दोबारा उभरने में एक दशक से अधिक समय लगा।
आपातकाल- भारतीय राज्य का दूसरा चरण: मुख्यतः राज्य के भीतर की शक्तियों का पुनर्संयोजन था। भारत का जो कथित पूंजीपति वर्ग था, उसे ट्रेड यूनियनों से मुक्ति और मजदूर वर्ग पर अधिक नियंत्रण की जरूरत थी। इंदिरा गांधी ने सर्वाधिक इसी हिस्से पर हमला किया और इस दौरान पूंजीपतियों ने मजदूर वर्ग का भयावह शोषण किया। इस प्रक्रिया में मजदूरों के संगठन बिखर गए, जो आज तक पुनर्संगठित नहीं हो पाए और आपातकाल के पहले जैसे संघर्ष को दोबारा नहीं बना पाए।
दूसरा पक्ष, भूमि पर नियंत्रणकारी क्षमता को बनाए रखने और संयोजित करने से संबंधित था। कांग्रेस ने कभी भी जमींदारों और बड़े भूस्वामियों का विरोध नहीं किया। उसने भूमि को उनके मालिकाना हक में रखते हुए सहकारी समितियों (कोऑपरेटिव) को विकसित करने पर जोर दिया।
इसका मुख्य प्रभाव गुजरात और महाराष्ट्र पर पड़ा। पंजाब से लेकर बंगाल तक कांग्रेस ने इस तरह के प्रयासों पर अधिक जोर नहीं दिया और ऐसे भूस्वामियों का समर्थन किया। कांग्रेस के सामने मुख्य समस्या भूमि प्रबंधन को लेकर थी। इसे लेकर इंदिरा गांधी के साथ हुए अंतर्विरोधों को पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बंगाल और कुछ हद तक बिहार में देखा जा सकता moo: सकता है।
नए और पुराने आपातकाल के बीच का विमर्श: नई और पुरानी आपातकाल की तुलना में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसमें एक को अच्छा बताया जाए। जब मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार आई, तो उसने सबसे पहले सत्ता के समीकरण को अपने पक्ष में करना शुरू किया। यह काम अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हो चुका था। इसने अपने पूंजीपति वर्ग के साथ-साथ कांग्रेसी पूंजीपतियों को भी अपने पक्ष में लाने का काम किया। जमीनों पर कब्जेदारी नए सिरे से शुरू हुई। अपने समूहों को खुली छूट दी गई, ताकि सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकें।
‘हिंदू व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और उसका सैन्यीकरण’ एक ऐसा सूत्र है, जिसे लागू करने के लिए सारे कानूनों को ताक पर रख दिया गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक फेरबदल और उस पर कब्जा भी ठीक इंदिरा गांधी की तर्ज पर किया जा रहा है, लेकिन अब कई गुना आक्रामक तरीके से। जिस तरह इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी में विरोधी पक्ष को बर्दाश्त नहीं किया, वही काम भाजपा के अंदर भी चल रहा है। संविधान और संसद को अपने मनमुताबिक ढालने के लिए सारी परंपराओं को ताक पर रखकर उन्हें अनुकूल बना देने की कोशिश रोज बढ़ रही है।
मजदूर वर्ग और किसानों की ओर देखें, तो वहां क्या हो रहा है? ट्रेड यूनियनों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। मजदूर आंदोलन और उससे जुड़ी हर गतिविधि को ‘देशद्रोह’ के अंतर्गत ला दिया गया है। मजदूरों के आवास की समस्या को हल किए बिना उन्हें उजाड़ देने में जो बेरहमी दिखाई जा रही है, वह युद्ध के समय जैसी है। पिछले दस सालों में मजदूरों की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठेका प्रथा अलग से उनसे पैसा वसूलती है।
फैक्ट्री और निर्माण स्थलों पर मजदूरों की मृत्यु और दोषियों का बच निकलना भारत के इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। यही हाल किसानों का है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, खासकर माओवादियों, पर जिस तरह का हमला हुआ है, वह अभूतपूर्व है। इसी तरह दलित, आदिवासी, मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले बढ़ रहे हैं, जो पिछले आपातकाल से थोड़े भिन्न जरूर हैं।
आपातकाल: प्रभुत्वशाली वर्ग का राज्य पर कब्जा: तब और अब के ‘आपातकाल’ में एक फर्क जरूर है, वह है राज्य की मूल वैधानिक व्यवस्था में फेरबदल। यह फेरबदल वैधानिक तरीकों से तो हो ही रहा है, साथ ही कानून की आड़ में एक घातक हस्तक्षेप भी हो रहा है। यह है वोट का अधिकार और सरकार चुनने में इसका प्रयोग। यह भारतीय राज्य को विश्व पटल पर वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आधार पर इसे विशाल लोकतंत्र कहा जाता है।
पिछले कुछ सालों में अनुकूल वोटरों को पक्ष में करने, विरोधियों को नियंत्रित करने, वोटों की संख्या में बढ़ोतरी करने जैसे कार्य, जो जनसंख्या के अनुपात में उपयुक्त नहीं प्रतीत होते, दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में तो दिए गए वोटों को ही बदल देने का प्रयास हुआ था। इस तरह की गतिविधियां राज्य को एक चरम नियंत्रणकारी संस्था में बदल सकती हैं और अन्य समूहों को बाहर कर सकती हैं, लेकिन इससे उसकी वैधानिकता पर सवाल उठ खड़ा होगा। यह राज्य अपने नए रूप में सामने आएगा, जिसे अपने लिए नई संवैधानिक व्यवस्था और विधायी तंत्र बनाना होगा। सत्तापक्ष की ओर से ऐसा दावा भी हो रहा है।
निश्चित रूप से इस राज्य का चरित्र वही नहीं होगा, जो इंदिरा गांधी के समय था। इस स्थिति में राज्य में आ रहे बदलाव का पहला प्रतिरोध उसके नियंत्रणकारी समूहों के बीच से ही आएगा। जैसा कि इतिहास में देखा गया है, ऐसे प्रतिरोध आमतौर पर कमजोर और बिखरे हुए होते हैं। इनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। संभव है, आने वाले समय में कुछ फेरबदल हो, लेकिन जिस बिंदु तक राज्य पहुंच चुका है, वहां से पीछे हटना अब बेमानी हो चुका है।
ऐसे में, इस आपातकाल बनाम उस आपातकाल की बहस में जाना उचित नहीं है। दोनों ही आपातकाल थे और दोनों ने नागरिकों के मूलभूत अधिकार छीन लिए। दोनों ने ही प्रतिरोध को कुचल दिया। दोनों ने मेहनतकश आबादी के उत्पादों पर कब्जा किया और उन्हें सामान्य जीवन से भी वंचित किया। दोनों ने ही मजदूरों के आवासों पर हमला किया और उन्हें शहरों से बाहर कर दिया। दोनों ने संगठनों और उनके नेताओं पर हमला किया और उन्हें जेलों में डाल दिया। प्रदर्शन के अधिकार तक छीन लिए गए। दोनों ने ही आम जन को उनकी क्षमता से वंचित किया और स्वयं को उनके नियंता के रूप में स्थापित किया। ‘मोदी है तो मुमकिन है’ इस आपातकाल का नारा है।
आपातकाल किसी राज्य की आकांक्षा हो सकती है, क्योंकि कोई भी राज्य एक नियंत्रणकारी संस्था होता है और बने रहने के लिए वह इस ताकत को लगातार अपने पक्ष में करता रहता है। यही आधुनिक पूंजीवादी राज्यों और भ्रष्ट समाजवादी राज्यों का अंतर्विरोध है। वे नियंत्रणकारी होने के लिए अपने लोकतंत्र की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए अभिशप्त हैं।
लेकिन यह अभिशाप ही है, जिसका असर आम जन पर पड़ता है। राज्य उससे संगठित होने, बोलने, जीवन जीने, शिक्षित होने, और यहां तक कि आवास और वोट देने के अधिकार तक छीन लेता है। यह भस्मासुर बन जाता है। ऐसे में, आपातकाल के बारे में यह कहना कि वह अच्छा था और यह बुरा है, मूलतः ऐसी बुराई को चुनने जैसा है, जो हमारे जीने के मूलभूत अधिकारों को ही छीन लेता है। मूल बात है राजनीति और राज्य को उचित परिप्रेक्ष्य में देखना और मूल नागरिक अधिकारों को एक मानक बनाकर विश्लेषण की पद्धति अपनाना।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं)