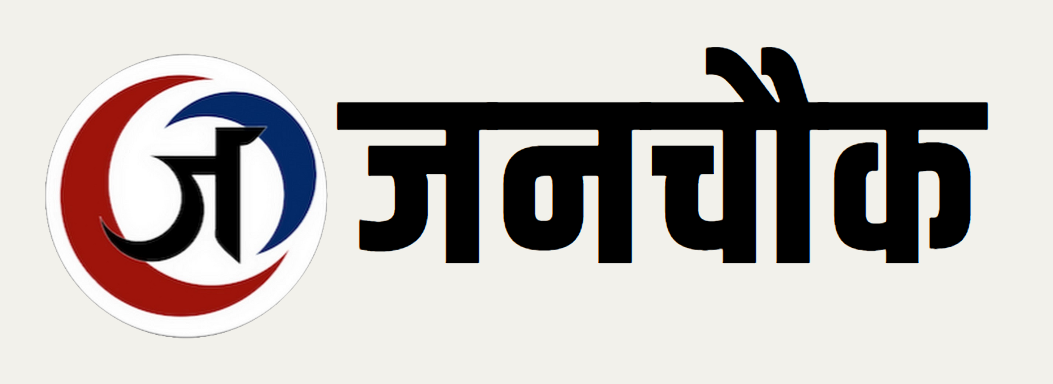क्या योगेंद्र यादव कुछ वाम बुद्धिजीवियों की तरह राजकमल प्रकाशन के पब्लिसिटी टूल की भूमिका में हैं या वे हर कड़े वक़्त में फ़ासिज़्म के प्रति जनता को अनुकूल बनाने की भारत के समाजवादी नेताओं की पुरानी परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं? या फिर `भारत जोड़ो अभियान` के संयोजक योगेंद्र यादव को कांग्रेस नेता राहुल गाँधी की वर्ण-जाति और साम्प्रदायिकता के सवालों पर रेडिकल पोजीशन ने विचलित कर दिया है और वे उनके लिए निर्मल वर्मा के बहाने सॉफ्ट हिन्दुत्व का पुराना मॉडल पेश कर रहे हैं? हिन्दी लेखक निर्मल वर्मा पर उनका लेख `रीविजिटिंग निर्मल वर्मा` (द इंडियन एक्सप्रेस, 17 जून 2025) यह सब सोचने के लिए मज़बूर कर रहा है।
सबसे पहले योगेंद्र यादव का शुक्रिया बनता है कि उन्होंने लेख की शुरुआत में ही उस तथ्य का, बहुत खुलकर न सही, उल्लेख ज़रूर कर दिया है जिससे प्रगतिशील धारा में व्याप्त निर्मल-भक्त मुँह चुराते रहते हैं। वे लिखते हैं- “बाद में जाकर उनका (निर्मल वर्मा का) झुकाव भाजपा की ओर हो गया और उन्हें हिन्दुत्व समर्थक करार दिया गया। उन्होंने इस तरह के आक्षेपों को अपनी अवमानना माना, लेकिन मंदिर और मंडल विवादों पर अपने विवादास्पद विचारों के कारण वह इन आक्षेपों के घेरे में आते रहे।“ निर्मल वर्मा के `सामाजिक और राजनीतिक लेखों` पर मोहित योगेंद्र यह दावा करते हुए कि विचारक के रूप में उन्हें याद नहीं किया गया, `सकारात्मक राष्ट्रवाद के लिए उनकी शरण में जाने` का आह्वान करते हैं।
देखने की बात यह है कि योगेंद्र यादव के लिए `मंदिर और मंडल विवादों पर विवादास्पद विचार` किस क़दर सुपाच्य हैं। `विवादास्पद विचार` इस दौर की फ़ासिस्ट पत्रकारिता का प्रिय पदबंध है। हम देखते हैं कि मीडिया जब किसी फ़ासिस्ट बयान का ज़िक्र करता है तो पक्षधरता के लिए `विवादास्पद विचार` या `बिगड़े बोल` जैसे धूर्तता भरे शब्दों का सहारा लेता है। योगेंद्र यादव यह नहीं बताते कि `मंदिर और मंडल विवादों पर विवादास्पद विचार` क्या थे और क्या इतने मामूली थे कि `आक्षेप` कहकर पल्ला झाड़ `विचारक` की `शरण` लेकर उसके सपनों के राष्ट्रवाद का कारसेवक बन लिया जाए।
योगेंद्र यादव को बाबरी मस्जिद विध्वंस में निर्मल वर्मा के वैचारिक अभियान का खुलकर उल्लेख करना चाहिए। उन के `सकारात्मक राष्ट्रवाद` के आदर्श विचारक निर्मल उस दौर में लिख रहे थे, “…यह बात राम-जन्मभूमि-विवाद से ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगी। उनकी राय में राम-जन्मभूमि का विषय राजनीति से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ कभी राम का मंदिर रहा होगा, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ़ एक `पौराणिक विश्वास` के सहारे मस्जिद-मंदिर का मामला तय नहीं किया जा सकता।…प्रश्न यह है कि यदि राम-जन्मभूमि को मिथक मानकर एक सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाओं की कोई चिंता नहीं की जाती, तो उसी तर्क के आधार पर एक उपन्यास (सैटेनिक वर्सेज) की कल्पनाजनित कथा में यदि किसी दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को ठेस पहुँचती है, तो उसके प्रति इतनी गहरी चिंता का क्या तर्क है?“ लालकृष्ण आडवाणी के अपनी रथ-यात्रा के दौरान दिए जा रहे भाषण योगेंद्र यादव ने सुने होंगे। उनके भाषणों के `यदिवादी तर्क` निर्मल वर्मा की इस टिप्पणी जैसे ही हुआ करते थे।
बहुत से बुद्धिजीवी ऐसा भी मानते हैं कि संघ का रामजन्मभूमि मंदिर अभियान को अचानक गति देने का फ़ैसला मंडल आयोग की काट (मंडल बनाम कमंडल) के तौर पर लिया गया था। हालांकि, बाबरी मस्जिद को लेकर दुष्प्रचार और मुसलमानों के विरुद्ध अभियानों का सिलसिला पुराना था और हिन्दू-राष्ट्र की परिकल्पना हमेशा सवर्ण राष्ट्र की परिकल्पना ही थी। यह दिलचस्प है कि निर्मल वर्मा अतीत में मंदिरों के विध्वंस का बदला लेने के नारे पर खड़े किए गए `रामजन्मभूमि अभियान` के किसी `बौद्धिक` की भांति लिख रहे थे। उनका लेखन एक पूरा पैकेज था जिसमें मुसलमानों से बदला लेने के विचार के प्रति जितना समर्थन था, उतना ही विरोध ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाले भारतीय समाज के अतीत के ज़िक्र और आरक्षण को लेकर था।
योगेंद्र यादव अपने प्रिय विचारक की इस टिप्पणी पर मुलाहिज़ा फ़रमाना चाहेंगे? – “अतीत, इतिहास और मिथकों के बारे में कब चुप रहा जाए, कब बोला जाए, इसका निर्णय भी वे (धर्मनिरपेक्षी नेता और बुद्धिजीवी) अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। उस अतीत को भुला देना बेहतर है, जब बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन किया गया था अथवा लाखों की संख्या में मंदिरों को ढाया गया था क्योंकि यद्यपि यह ऐतिहासिक सत्य है, तो भी इसे याद करने पर `साम्प्रदायिक विद्वेष` फैलता; किंतु उस अतीत को अवश्य पुनर्जीवित किया जाए जब ब्राह्मणों के प्रभुत्व से भारतीय समाज में वर्ग-शोषण का सूत्रपात हुआ। यह दूसरा अतीत ऐतिहासिक रूप से सच हो न हो, कम से कम हमारे आरक्षणकर्ताओं के लिए तात्कालिक लाभ तो पहुँचा ही सकता है।“
तो निर्मल वर्मा यह भी नहीं मानते कि भारतीय समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व से कोई ख़राबी आई होगी – “ब्राह्मणों के प्रभुत्व से भारतीय समाज में वर्ग-शोषण का सूत्रपात हुआ, यह दूसरा अतीत ऐतिहासिक रूप से सच हो न हो…।“ तो इसके इलाज की किसी ज़रूरत को ख़ारिज़ करना उनके लिए स्वाभाविक है। ऐसा विचारक आज जीवित होता तो इस `सकारात्मक राष्ट्रवाद` की बानगी के तौर पर मुसलमानों और दलित-पिछड़ी जातियों के लोगों पर आए दिन हो रही ज़ुल्म-ओ-सितम की घटनाएं देखकर कितना प्रफुल्लित हो रहा होता! लेकिन, योगेंद्र यादव की समस्या क्या है? उनका `समाजवाद`, उनका `सामाजिक न्याय`, उनका `सेकुलरिज़्म` इस सब पर मोहित क्यों है कि वे निर्मल की ऐसी भयानक पक्षधरता को इतना अंडरप्ले करके, उनकी ज़रूरत पर ज़ोर देने लगते हैं? क्या वे भारत के समाजवादी पुरोधाओं की परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं?
समाजवादी राजनीति के दिग्गज डॉ. राम मनोहर लोहिया ने अपनी तमाम मेधा और राजनीतिक पैंतरेबाजी का उपयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद के लिए किया। गाँधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। प्रतिबंध हटा लिए जाने के बावजूद उसकी विश्वसनीयता पर संकट था और ख़ुद को सेकुलर कहने वाले किसी नेता का उसके साथ खड़े हो पाना आसान नहीं था। लेकिन, लोहिया ऐसे गाढ़े वक़्त में संघ के साथ बने रहे। नेहरू-इंदिरा विरोध की राजनीति के नाम पर उन्होंने संघ की राजनीतिक विंग जनसंघ को ख़ूब खाद-पानी दिया। उनके कई राजनीतिक सहयोगियों और वफ़ादार सिपहसालारों ने उन्हें टोका भी, लेकिन वे टस से मस न हुए। फिर, इंदिरा गाँधी की राजनीति के विरोध में विपक्ष की एकजुटता के नाम पर समाजवादी राजनीति के पितृ-पुरुष जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने भारी विरोध की परवाह न करते हुए आरएसएस के साथ गलबहियाँ कीं और यहाँ तक ऐलान कर डाला कि यदि आरएसएस फ़ासिस्ट है तो वे ख़ुद भी फ़ासिस्ट हैं।
कमाल की बात यह है कि गाँधी की हत्या के इल्ज़ाम से घिरी ताक़त के तारणहार बने जेपी के `समाजवाद` के साथ `गाँधीवादी` भी जोड़ा जाता है। जेपी को मोहरा बनाकर देश की मुख्यधारा में ताक़त के रूप में उभर आई संघ की राजनीतिक विंग जनसंघ ने जनता पार्टी से ताल्लुक़ तर्क करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की शक्ल इख़्तियार की तो उसने भी अपनी सियासत को `गाँधीवादी-समाजवाद` का ही नाम दिया। गो कि अब संविधान से सेकुलर और समाजवाद शब्दों तक को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है।
बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्पन्न अकेले पड़ने की स्थिति में एक बार फिर `समाजवादी आइकन` ही संकटमोचक बने थे। बेशक भारतीय जनता पार्टी अब तक एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी लेकिन कहने भर को ही सही, ख़ुद को सेकुलर कहने वाले दलों के लिए बाबरी मस्जिद विध्वंस को नज़र-अंदाज़ कर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सोशलिस्ट पोस्टर-बॉय जॉर्ज फ़र्नान्डिस और मंडल-छाप समाजवादी शरद यादव व नीतीश कुमार ने संघ की सियासत की हिमायत में खड़े होने की पहल की। नीतीश अपने डगमग स्वास्थ्य के बावजूद अभी भी भाजपा के बिहार-रथ में जुते हुए हैं।
समाजवादी क़यादत की ऐसी मशालें सियासत में ही नहीं साहित्य और वैचारिक हलक़ों में भी जन-द्रोही, पूँजीवादी और सांस्कृतिक वर्चस्ववादी परवानों को आकर्षित करती रही हैं। योगेंद्र यादव अगर संघ-भाजपा की हिन्दुत्ववादी राजनीति से मेल खाने वाले निर्मल वर्मा के विचारों में आस्था जता रहे हैं तो ऐसे सिलसिले के लिहाज़ से हैरत भी क्या है! लालू यादव जैसी जिन कुछ शख़्सियतों ने समाजवादी मसीहाओं की बनाई चालाक प्रणाली में फंसने के बजाय ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी तो इसलिए कि वे वर्णवादी सांस्कृतिक वर्चस्व के साये में राजनीतिक और सामाजिक उत्पीड़न के दौर-दौरों से गुज़रे तबकों के हालात से मुँह नहीं मोड़ पाए। योगेंद्र यादव हरियाणा की जिस अहीरवाल बेल्ट से आते हैं, वहाँ की फ़ज़ा में ऐसी रेडिकल सबार्लटन-सेकुलर सियासत की परंपरा भी नहीं रही। यहाँ `राव साहब` कहलाने वाले अहीर नेताओं ने वक़्त-बेवक़्त पाला बदलते हुए न मुस्लिम वोटरों के लंबे समर्थन की परवाह की, न सामाजिक न्याय के सवालों की। यह सब योगेंद्र यादव भी यदा-कदा प्रदर्शित करते ही रहे हैं।
शायद यह संयोग हो कि मुझे मार्च 2002 में करनाल में योगेंद्र यादव से अब तक की एकमात्र बातचीत का मौक़ा हाथ लगा था तो वे इसी रहगुज़र पर थे। वे इमरजेंसी को याद करते हुए और हरियाणा में यात्रा पर निकले थे। जिस शहर में उनका कार्यक्रम होता, वे वहाँ के अनुभवों का ज़िक्र हरियाणा में सर्वाधिक प्रसार वाले ‘दैनिक भास्कर’ में अपने कॉलम में करते। करनाल में शाम के कार्यक्रम से पहले दोपहर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ‘अमर उजाला’ के रिपोर्टर की हैसियत से मैंने पूछा कि क्या हरियाणा के वर्तमान परिदृश्य को लेकर उनसे कुछ छूट रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपनी समझ से बात रख चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको हरियाणा में आरएसएस का आक्रामक साम्प्रदायिक अभियान दिखाई क्यों नहीं दे रहा है।
उन का जवाब हतप्रभ करने वाला था। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उस तरह मुस्लिम आबादी नहीं है और यहां यह समस्या यूपी, बिहार आदि राज्यों की तरह नहीं है। गोधरा के विरोध में बंद के नाम पर करनाल में मस्ज़िद पर पथराव तो मैंने ही कवर किया था। पड़ोसी जिले कैथल में मस्ज़िद पर हमला हो चुका था। लोहारु की वारदातें भी शायद हो चुकी थीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह आपको भयावह नहीं लगता कि जहां कथित प्रोवोकेशन भी न हो, वहां यह सब हो रहा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनकी आँखों पर अपनी इस यात्रा में संघ का समर्थन हासिल होने की मज़बूरी का परदा पड़ा हुआ है। यह एक तीखी मगर सच्ची बात थी। योगेंद्र यादव की इस यात्रा का आर्किटेक्ट इसी तरह का था। करनाल में हम देख ही रहे थे। गोष्ठी की तैयारी के लिए कॉमरेडों और स्वयंसेवकों का कॉकटेल (आपातकाल के दौर की पुरानी लत) तैयार किया गया था।
योगेंद्र यादव असहज हुए लेकिन भड़के नहीं। कुछ देर ख़ामोश रहे और फिर शालीनता से बोले कि कोई संशय पैदा हुआ है तो वे सेकुलरिज्म को लेकर अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हैं। इस बातचीत ने उन्हें असहज कर दिया था। शाम को गोष्ठी में योगेंद्र यादव ने मंच से हरियाणा और देश में चलाई जा रही साम्प्रदायिक मुहिम की तीखी आलोचना की। कार्यक्रम में काफी संख्या में मौजूद स्वयंसेवकों ने उनका प्रतिवाद किया। वहां मौजूद विभिन्न प्रगतिशील और वामपंथी रुझान के संगठनों के लोग भी बोले। नोकझोंक जैसे माहौल में योगेंद्र यादव ने और दृढ़ता के साथ अपनी बात को दोहराया। लेकिन, यह सवाल हमेशा रहा ही कि वे कोंचे जाने तक हरियाणा की उन ताज़ा भयानक घटनाओं को अनदेखा क्यों करते रहे और उन्हें अंजाम देने वालों के साथ ही बदलाव का ख़्वाब देखने लगे जो कुछ बरसों बाद ही पूरा परिदृश्य बदलने जा रहे थे?
अब जबकि योगेंद्र यादव इस हिन्दुत्ववादी बदलाव के समर्थक बौद्धिक के `सकारात्मक राष्ट्रवाद` का राग अलापने बैठे हैं तो यह सवाल फिर ज़ेर-ए-नज़र है कि यह उनकी वैचारिक विरासत में शामिल है अथवा हवा का रुख या कहीं से भी कुछ पाते चले जाने का अरमान उन्हें यह सब करने पर मज़बूर कर देता है। यूपीए रिजीम में यूजीसी की सदस्यता पाने वाला यह बुद्धिजीवी कांग्रेस की सत्ता से चलाचली की बेला में कांग्रेस की मौत के लिए ट्वीट कर रहा होता है और अन्ना के फ़ासिस्ट अभियान के दौरान विचार-निरपेक्षता का दम्भ भरते हुए आम आदमी पार्टी के ज़रिये हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का ख़्वाब देखने लगता है। फिर वहां से धकियाए जाने पर दिल्ली चुनाव में NOTA दबाने की अपील करता है।
एक सवाल यह है कि `भारत जोड़ो अभियान` के संयोजक के नाते वे अब फिर कांग्रेस के नज़दीक हैं तो क्या राहुल गाँधी की साम्प्रदायिकता और ख़ासकर वर्ण-जाति के सवाल पर रेडिकल पॉजिशन उन्हें असहज कर रही है। कांग्रेस के ही बहुत से नेताओं को लगता है कि इस तरह के मसलों पर राहुल की मुखरता कांग्रेस के ख़िलाफ़ सवर्ण एकजुटता को बढ़ावा देती है। तो क्या निर्मल वर्मा के विचारों के इस कथित सकारात्मक राष्ट्रवाद का गीत कांग्रेस को ही अपने सॉफ्ट हिन्दुत्व के मॉडल पर बने रहने की सलाह के तौर पर छेड़ा गया है?
या यह कि पत्रकार, मीडिया विश्लेषक, लेखक, एक्टिविस्ट, पदयात्री, थिंक टैंक, चुनावी उम्मीदवार आदि अनेक भूमिकाओं में रहने वाले योगेंद्र यादव साहित्यिक क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा दिखाने को आतुर हैं और कुछ वाम बुद्धिजीवियों की तरह राजकमल प्रकाशन के पब्लिसिटी स्टंट के टूल की भूमिका निभाते हुए इस हद तक पहुँच गए हैं? गगन गिल ने अपने पति निर्मल वर्मा की किताबों के प्रकाशन का अधिकार राजकमल से ले लिया था। गगन गिल ने निर्मल की किताबें फिर से राजकमल को सौंप दी हैं तो प्रकाशन ने इसका ज़ोर-शोर से प्रचार किया है। अप्रैल में निर्मल वर्मा की 96वीं जयंती पर `राजकमल प्रकाशन` ने गगन गिल के सानिध्य में ‘कृती निर्मल’ कार्यक्रम का आयोजन किया तो इसी प्रकाशन की पत्रिका `आलोचना` के संपादक संजीव कुमार जो वाम लेखक संगठन जलेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, से भी निर्मल वर्मा के क़सीदे पढ़वाए गए।
संजीव कुमार ने अतिश्योक्ति भरा बयान दिया कि मुझे नहीं लगता कि निर्मल को पढ़ने वाला कोई व्यक्ति कभी असहिष्णु भी हो सकता है। बाद में उन्होंने अपने दावे के बचाव में निर्मल की कहानियों की ओट लेने की कोशिश की। एक निर्मल-भक्त ने इस कार्यक्रम में निर्मल के आलोचकों को उनके `दो-चार निबंधों` को ही पढ़ लेने की नसीहत दे डाली थी। इसी तर्ज़ पर योगेंद्र यादव अपने लेख की शुरुआत में कहते हैं – “समकालीन भारत में विचारों पर मंथन के लिए निर्मल वर्मा एक परिचित नाम नहीं है। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग उन्हें जानते भी हैं, वे आमतौर पर उन्हें सिर्फ कथाकार और उपन्यासकार मानते हैं। और जिन्होंने उनका सामाजिक और राजनीतिक लेखन पढ़ा भी हो, वे नहीं जानते कि उसे किस तरह लिया जाए।“
असल में योगेंद्र यादव झूठ बोल रहे हैं। निर्मल वर्मा सेलिब्रिटी लेखक हैं और उनके कथा साहित्य व वैचारिक निबंधों पर ख़ूब मंथन-मनन हुआ है। उनके लेखन में फ़ासिज़्म को ख़ाद-पानी देने वाले विचार पूरी स्पष्टता और पूरी दृढ़ता के साथ बार-बार आते हैं। इस हद तक कि कोई घृणित व्यक्ति ही उनकी वैचारिकी का मुरीद हो सकता है। आलोचक कृष्णमोहन ने `निर्मल वर्मा की भारतीयता और कलात्मकता का सच` लेख में ठीक ही लिखा है, “निर्मल वर्मा की मूल चेतना वर्णाश्रमवादी है, भारतीय फ़ासीवाद जिससे नाभिनालबद्ध है।
अपनी तथाकथित भारतीयता को यथासंभव रहस्यमय और आदर्शीकृत रूप देने के बावजूद यह सत्य उनके अपने वक्तव्यों से ही उजागर हो जाता है। विश्वासों, अनुष्ठानों, और जातिगत दायित्वों में इसके धार्मिक गठन का प्रसंग हम देख चुके हैं। अब ज़रा वर्णव्यवस्था को इसमें मिलने वाली केंद्रीय हैसियत पर ग़ौर करें—‘हिंदुओं के लिए जब तक “अन्य” किसी तरह अपने या अपने आंतरिक तंत्र में समाविष्ट न हो, वह एक ऐसा संबोधी हो ही नहीं सकता, जिससे अर्थपूर्ण संवाद किया जा सके। अगर अस्पृश्यता की समस्या हिन्दू समाज में विवादास्पद हो सकी तो इसका कारण यह है कि शूद्र वर्ण-व्यवस्था में समाविष्ट हैं लेकिन वे तब भी समाज की परिधि पर बने रहे। वे म्लेच्छों की तरह पराए तो नहीं, लेकिन वे पूरी तरह भीतर के भी नहीं थे।’
सवाल यह है कि ‘शूद्र’ ‘म्लेच्छों’ की तरह नहीं तो क्या अनार्यों की तरह ‘पराए’ थे। जाति, वर्ण, और नस्ल के गंदे घोल से बनी यह तस्वीर आख़िर किस भारत की है। शूद्र अपने होते तो यही तो होता कि अस्पृश्यता निर्विवाद रहती। इसी विवाद का निर्मल वर्मा को दुख है। दलितों के प्रतिरोध को पचाने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। हालांकि, जहाँ कामयाबी मिल गई वहाँ उनकी ख़ुशी भी छिपाए नहीं छिपती, जैसे कि बौद्ध धर्म के मामले में—‘वे पराये होते हुए भी अपने थे और अन्ततः वे बिल्कुल अपने हो गए, और बौद्ध धर्म भारत में लुप्त नहीं, लीन हो गया। दूसरी ओर इस्लाम और ईसाई धर्म अपने असंदिग्ध पराएपन के कारण आज तक संस्थाबद्ध रूप में भारत में अस्तित्वमान हैं।“
योगेंद्र यादव चाहें तो निर्मल वर्मा की वैचारिकी के कुछ और उद्धरण देख सकते हैं-
“आज हम अपने को आधुनिक कहने वाले, मनुस्मृति का तिरस्कार करते हैं और उसकी मनीषा तथा उसके चिंतन को तिरस्कृत करते हैं।“
“जो लोग अल्पसंख्यक वर्ग का अपने को समर्थक कहते हैं, वे बहुसंख्यक वर्ग को अलग वर्ग के रूप में स्वीकार करने से बच नहीं सकते। यही तर्क उन पर भी लागू होता है, जो समाज को जातियों और वर्ग में बांटकर देखना चाहते हैं।“
“मैं आरक्षण की नीति के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। यह उसी नीति की परिणिति है कि हम जातिवाद को आरक्षण के द्वारा लगातार विकृत और प्रदूषित कर रहे हैं।“
“हमारी ये नागरिक अधिकारों की स्वयंसिद्ध संस्थाएं (पी.यू.सी.एल. आदि) पंजाब और कश्मीर में मरने वाले निर्दोष नागरिकों की नृशंस और निरुद्देश्य हत्याओं के बारे में चुप रहती हैं, किन्तु ज्यों ही राज्य की ओर से आतंकवादियों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है, तभी अचानक वे अपना मौन व्रत तोड़कर राज्य आतंकवाद की भर्त्सना करने लगती हैं, मानो हिंसावादियों के मानवाधिकार हिंसा से संत्रस्त नागरिकों की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान हैं।“ “यह जो धर्मनिरपेक्षता की नकल करते हैं, यह भारतीय मनीषा, भारतीय परंपरा, भारतीय स्वभाव से कहीं मेल नहीं खाता।“
“…सच तो यह है कि मुझे भारत द्वारा किए गए अणुविस्फोटों पर कोई गर्व नहीं है। लेकिन मुझे इस पर शर्म भी नहीं महसूस हो रही। कश्मीर के राजा ने जब पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने के लिए भारत से सैनिक मदद मांगी थी तो अहिंसावादी गांधीजी ने इन सेनाओं को भेजे जाने का समर्थन किया था। आज जब अणु विस्फोटों के संबंध में गांधीजी की दुहाई दी जाती है, तो अक्सर लोग इस कृत्य को भुला देते हैं।“
ऐसा नहीं है कि निर्मल वर्मा के इन विचारों से योगेंद्र यादव वाक़िफ़ नहीं हैं। अपने लेख में वे इसका ज़िक्र करते चलते हैं लेकिन हर बार `फिर भी` के सहारे उनकी शरण में जाने की ज़रूरत भी जताते चलते हैं। मसलन- “धर्मनिरपेक्षता की उनकी आलोचना निर्मम और कभी-कभी अतिशयोक्तिपूर्ण भी होती थी, फिर भी इसने हिंदू सांप्रदायिकता की आलोचना करने के लिए भी तर्क दिए।“ वर्णाश्रमी, साम्प्रदायिक और उन्मादी राष्ट्रवाद के पक्षधर निर्मल वर्मा को बंगाल के पुनर्जागरण और आधुनिक भारतीय विद्वानों से क्यों दिक्कत न होगी लेकिन योगेंद्र यादव की बौद्धिक गुलामी का कारण क्या हो सकता है?
`सांस्कृतिक उपनिवेशवाद` के विरोध के जुमले की आड़ में वे निर्मल वर्मा की ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक पक्षधरता की स्वीकार्यता के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? वाम विरोध और असल में ब्राह्मणवादी झुकाव में जो मासूम तर्क तुलसीदास के लिए दिए जाते हैं, लगभग उन्हीं के सहारे वे निर्मल वर्मा के विचारों को अपनाने की गुहार लगाते हैं। ऐसी ही मासूमियत में वे कहते हैं, “दिलचस्प बात यह है कि वामपंथियों ने तो उन्हें नकार दिया और उन पर प्रहार किया, लेकिन दक्षिणपंथियों ने कभी भी उनके विचारों को स्वीकार नहीं किया।“
योगेंद्र यादव का यह दावा भी मज़ेदार है कि “क्योंकि वह हमें ऐसे सवाल पूछने के लिए मजबूर करते हैं जिनसे ‘प्रगतिशील’ आधुनिक भारतीय बचते रहे हैं। क्योंकि इस चुप्पी और उदासीनता से पैदा हुई रिक्तता के कारण हमारे राष्ट्रवाद को नकली तत्वों ने हथिया लिया है। क्योंकि निर्मल वर्मा इन प्रश्नों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो तीखे भी होते हैं और रचनात्मक भी। क्योंकि जब तक हम इन असहज प्रश्नों का सामना नहीं करते, तब तक हम अपना राष्ट्रवाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते।“ दिलचस्प यह है कि योगेंद्र यादव ने यह लिखते हुए निर्मल वर्मा के साथ ऐसे विचारकों की एक फ़ेहरिस्त ही पेश कर दी है जिनमें से कुछ के दक्षिणपंथी लेखन की पहचान मैं भी कर सकता हूँ।
मसलन, धरमपाल जिनके साथ गाँधीवादी विशेषण जोड़ा जाता है लेकिन विचारों के लिहाज़ से वे संघी ठहरते हैं। उनकी जो एक किताब कभी हाथ लगी थी, उसका लब्बो-लुआब यही था कि अंग्रेजों से आने से पहले हमारी गुरुकुल व्यवस्था और तमाम परंपराएं महान थीं। योगेंद्र यादव `सांस्कृतिक उपनिवेशवाद` के विरोध के जिस फ़िक़रे के सहारे निर्मल वर्मा की ज़रूरत जता रहे थे, असल में वह निर्मल जैसे वर्ण-इलीट का यह शिकवा है कि ब्राह्मणवाद के हाथों शिक्षा और सम्मान से वंचित तबके कैसे आधुनिक शिक्षा के सहारे समाज में कुछ जगह पा गए। योगेंद्र यादव की सूची में एक नाम जाने-माने दक्षिणपंथी रमेश चंद्र शाह का भी है जो गाहे-ब-गाहे सीधे संघ के औज़ार के तौर पर भी पेश आने में नहीं हिचकते हैं। उन्होंने एक नाम आशीष नन्दी का भी लिया है, सेकुलरिज़्म से जिनका गहरा बैर जग-ज़ाहिर है?
तो योगेंद्र यादव के ऐसे नवरत्नों का राष्ट्रवाद उनको मुबारक हो। बात को समेटते हुए सिर्फ़ यह कि निर्मल वर्मा का वाम से प्रेम और मोहभंग भी कम रोचक नहीं है। बंगाल के उनके नज़दीकी वाम नेता की सिफ़ारिश से नामवर और पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस उनके लिए सक्रिय रहे। वाम से रिश्ता उनके लिए जब तक फलदायी रहा, बरक़रार रहा। सोवियत संघ की `साम्यवादी सत्ता` के प्राग पर हमले ने निर्मल वर्मा को बदल दिया था, यह प्रचार हिन्दी लेखकों का या तो ख़ुद को या दूसरों को झाँसा देने की अदा से ज़्यादा कुछ नहीं है।
किसी भी तरह की `राजनीतिक हिंसा` या `तानाशाही` से विचलित व्यक्ति जो एक सुधी लेखक है, किस तरह एक फ़ासिस्ट अभियान का विचारक-प्रचारक बन सकता है? एक कथित सौम्य व्यक्ति माक़ूल वक़्त आने पर खुलकर मनुस्मृति के साथ खड़ा है, वर्णाश्रम को सही ठहराता है, आरक्षण का विरोध करता है और `आधुनिक` दौर में इस विचारधारा के उग्र राजनीतिक उभार की उस मुहिम का समर्थन करता है। ऐसे प्रो-फ़ासिस्ट विचारक पर फ़िदा बुद्धिजीवी को क्या कहा जाए, यह योगेंद्र यादव को ख़ुद तय करना चाहिए।
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित योगेंद्र यादव का लेख:
(धीरेश सैनी वरिष्ठ पत्रकार और टिप्पणीकार हैं।)