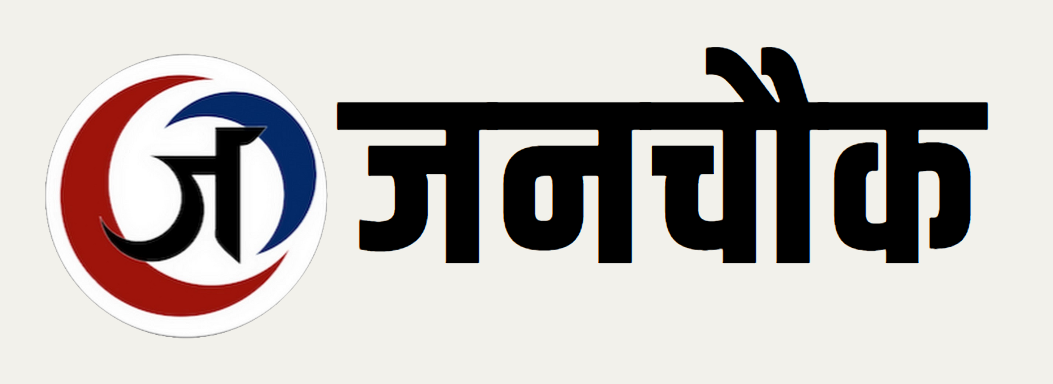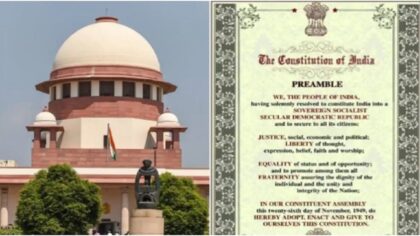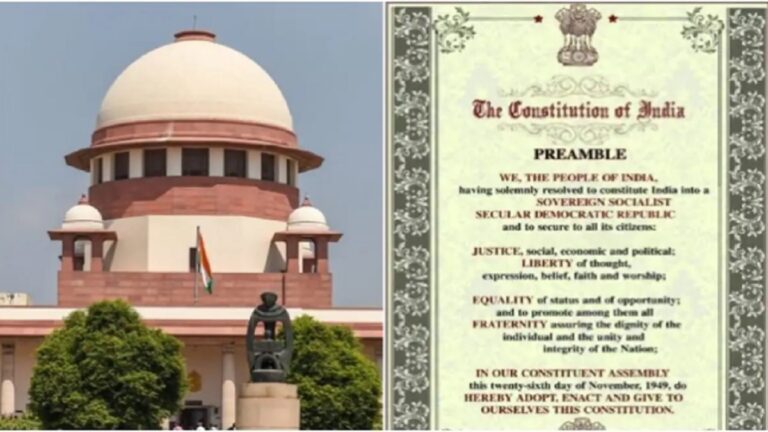आसिफ तन्हा, देवांगना कलीता और नताशा नरवाल की जमानत के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस जे भंभानी के पारित आदेश ने यूएपीए न्यायशास्त्र के पूरे ब्लैक बॉक्स को खोल दिया है। यूएपीए भारतीय न्यायशास्त्र का कई कारणों से ब्लैक बॉक्स बन गया था। पहला, जैसा कि आदेश में चिन्हित किया गया है कि यूएपीए के सेक्शन-15 में ‘आतंकवाद’ की परिभाषा बेहद अस्पष्ट है और इसे एक ऐसे लाइसेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जिसमें सभी प्रकार के उल्लंघनों को आतंकवाद के तौर पर पेश किया जा सकता है। यह आदेश उस बात पर और प्रकाश डालेगा कि कैसे लोगों को यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोपी बनाया जाता है।
राज्य को इस बात को दिखाने की जरूरत पड़ती है कि कैसे कथित अपराध या फिर उल्लंघन आईपीसी या फिर दूसरे प्रासंगिक कानूनों के तहत आने वाले परंपरागत अपराधों से जुड़े कानूनों के जरिये डील नहीं किया जाना चाहिए। यह इस बात को भी समझने में मदद करता है कि एक देश में सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्या को आतंकवाद की समस्या के बराबर नहीं रखा जाना चाहिए। इन दोनों बातों के बीच बिल्कुल साफ अंतर करता है कि लिस्ट एक और दो के तहत पहला राज्य का विषय है जबकि दूसरा केंद्र का। यह आदेश कानून को लागू करने के संबंध में संघवाद के निहितार्थ के लिहाज से भी बेहद प्रभावकारी होगा।
दूसरा, यह कम से कम जब कोई केस होगा तो उसे यूएपीए के तहत चार्ज करने के लिए एक सामान्य मानक निर्धारित करता है। और खास करके यह आदेश इस बात पर जोर देता है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, व्यक्तियों के रूप में उनके द्वारा किए गए कृत्यों से संबंधित होना चाहिए और उसे विशेष रूप से तैयार किया जाना चाहिए। यह हाल के दिनों में जारी चलन के खिलाफ है जिसमें चार्जशीट तथ्यों से ज्यादा अटकलबाजियों पर निर्भर होती है। व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाइयों की जगह बड़े राजनीतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए आरोपों को तय किया जाता है। और फिर यह सब कुछ बिल्कुल अस्पष्ट तरीके से तैयार किया जाता है।
तीसरा, यह आदेश जमानत के महत्वपूर्ण मुद्दे को खोलता है। यूएपीए की व्यापक दायरे में व्याख्या की जाती है और जब जमानत की बारी आती है तो यह उसके लिए काफकेस्क कानून बन सकता है। यह बात जमानत देने से रोक देती है अगर वहां विश्वास करने का कोई तार्किक आधार है कि अभियोजन का केस प्रथम दृष्ट्या सत्य हो सकता है। इस मामले में समस्या इस बात की है कि प्राय: अभियोजन पक्ष के वर्जन को बगैर किसी क्रास पूछताछ के स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष को और ज्यादा ही कैच-22 की स्थिति में खड़ा कर दिया है। जिसमें उसने अदालतों को जमानत की सुनवाई के समय केस की मेरिट पर ज्यादा तहकीकात करने से रोक दिया है। यह आदेश इस तथ्य को दोहराता है कि न्यायालयों के पास अभी भी एक जगह है जिसमें वे जमानत की सुनवाई के दौरान भी सरकार के केस की समीक्षा कर सकते हैं। वे परीक्षण कर सकते हैं जैसा कि इस आदेश में हुआ, कानून को कैसे लागू किया गया। इसके साथ ही वे प्रमाण से जुड़े सवालों में भी प्रवेश कर सकते हैं। हालाँकि, यहाँ थोड़ी वैचारिक चुनौती जरूर है। कोर्ट ने ठीक ही मामले में स्टेट द्वारा पेश किए गए प्रमाणों की प्रकृति जानने की कोशिश की और उसे बेहद कारगर तरीके से ध्वस्त कर दिया। इन आदेशों में लाए गए विचारों के आधार पर इस बात की कल्पना कर पाना कठिन है कि कोई दूसरी कोर्ट राज्य के मामले को अभियोजन के लिए बनाए रखेगा।
सवाल यह है कि अगर कोई ऊंची अदालत एक जमानत की सुनवाई करती है तो कैसे उसके आदेश इस तरह से तैयार किए जा सकते हैं जो पूरे चले ट्रायल के नतीजे को नहीं समझ पाता है। इस मामले में आरोप और प्रमाण स्पष्ट रूप से बेतुके थे। यहां यह देख पाना बिल्कुल कठिन था कि कैसे कोई दूसरी कोर्ट किसी और नतीजे पर पहुंचती। लेकिन जब कोई ऊंची अदालत कोई जमानत की सुनवाई करती है और अभियोजन पक्ष के केस को ध्वस्त करने के आधार पर जमानत देती है तो इसका फिर फुल ट्रायल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह केस राज्य को इस बात का बेहद गहरा तर्क देता है कि उसे खास कर इस कारण से बहुत सारी परिस्थितियों में जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए: जमानत का विरोध करना बगैर फुल ट्रायल के संदर्भ के केस को बड़े परीक्षण का रास्ता खोल देता है। यह एक बेहद दिलचस्प अवधारणात्मक मुद्दा है।
यह आदेश हमारे नागरिक अधिकारों को राज्य की सत्ता द्वारा अपने ब्लैक होल में समाने से रोकने की दिशा में एक बड़ा स्वागत योग्य प्रयास है। यूएपीए एक समस्याग्रस्त कानून है क्योंकि यह निर्दोष होने की किसी पूर्व कल्पना पर ही हमला करता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह से बनता जा रहा है जैसे मूल अधिकार हैवियस कार्पस हो गए हों। स्टेट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक अपराध के तौर पर तोड़-मरोड़ रहा हो, सामान्य विरोध भी या तो दबाया जा रहा है या फिर उसे आपराधिक बना दिया जा रहा है, जमानत नियमित तौर पर खारिज कर दी जा रही है और राज्य सक्रिय रूप से मतभेद रखने वालों को निशाना बना रहा है। इस संदर्भ में कुछ सामान्य ज्ञान के सिद्धांतों का फिर से दोहराव बेहद स्वागत योग्य है: यह संवैधानिक विवेक के फिर से स्थापित होने के लिहाज से एक उम्मीद और कुछ सहायता मुहैया कराता है।
लेकिन भारत में नागरिक अधिकारों की दिशा को लेकर ज्यादा आशान्वित होना भी बहुत जल्दबाजी होगी। यह बेहद सुकून का विषय है कि ट्रायल कोर्ट ने अंत में आरोपियों को रिहा कर दिया। लेकिन उससे पहले उनकी रिहाई में इस आधार पर एक दिन की देरी कर दी गयी थी कि उनके पते प्रमाणित नहीं किए जा सके हैं। अगर राज्य किसी ऐसे शख्स का पता प्रमाणित नहीं कर पाया है जिसको उसने एक साल से ज्यादा हिरासत में रखा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर हंसा जाए या फिर चिल्लाया जाए। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अधिकारियों ने अपनी माफी के एक पैरोडी वर्जन पर काम करने का फैसला किया। लेकिन इस सच्चाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है। आदेश दिल्ली पुलिस और गृहमंत्रालय में बैठे उनके आकाओं के लिए एक कलंक है। किसी भी सभ्य लोकतंत्र में सिर शर्म से झुक गया होता। बजाय इसके यहां हम राज्य द्वारा उससे भी ज्यादा हमलावर एक अपील पाएंगे। हम केवल आशा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता के इस पक्ष को झुकने नहीं देगा।
हम यह भी जानते हैं कि मील के पत्थरों वाले आदेश अक्सर राज्य या फिर न्यायालय की प्रकृति पर बहुत कम प्रभाव डाल पाते हैं। वो कभी-कभी हाईप्रोफाइल केसों में ही काम करते हैं। कुछ समय वे ड्यूटी करने वाले जजों के विवेक को परिलक्षित करते हैं जैसा कि इन जजों ने शायद किया है। लेकिन ज्यादा तो नहीं कभी-कभी पैन में प्रकाश की तरह से चमक कर हमें इस भ्रम को बनाए रखने की छूट देते हैं कि न्यायपालिका किसी दिन न्याय मुहैया करेगी। अपने उदाहरण की शक्ति से क्या यह आदेश भीमा कोरेगांव केस में जारी न्याय की त्रासदी पर भी असर डालेगा और सुधा भारद्वाज तथा आनंद तेलतुंबडे के भविष्य को प्रभावित करेगा? कल ही इस अखबार ने मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफान की कहानी को अपने फ्रंट पेज पर प्रकाशित किया था। जिन्हें नौ साल बाद यूएपीए से संबंधित आरोपों से मुक्त किया गया था। उन्होंने अपने कीमती सात साल जेल में बिताए थे जिनमें उनकी जमानत के चार आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। यह इस बात को याद दिलाने लायक है कि यूएपीए की विकृति किन्हीं खास राजनीतिक दलों के लिए विशिष्ट नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल सिस्टम में समाहित है।
इस जमानत आदेश ने यूएपीए न्यायशास्त्र के ब्लैक बॉक्स को खोल दिया है। यह बिल्कुल तार्किक है, बगैर किसी हिस्टीरिया के और बिल्कुल पूरे संवैधानिक सामान्य ज्ञान के तहत। लेकिन क्या यह आदेश हाल के दिनों में न्यायपालिका के दामन पर लगे काले धब्बों को साफ करने के लिहाज से पर्याप्त होगा।
(प्रताप भानु मेहता का यह लेख आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। साभार लेकर इसका यहां अनुवाद दिया जा रहा है।)