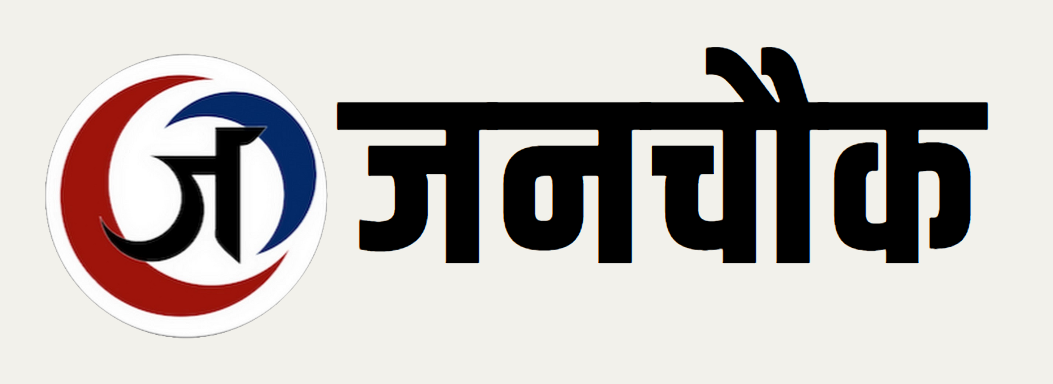आजादी के साथ ही भारतीय संविधान के बनाने की प्रक्रिया के दौरान ही हमारे पुरखों ने इस बात का हमेशा ख्याल रखा और उम्मीद जताई थी। इस गैर बराबरी, भेदभाव और सामंती मूल्यों पर निर्मित भारतीय समाज को न्यायप्रिय, समता मूलक, समावेशी और लोकतान्त्रिक बनाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया को ही राष्ट्र निर्माण कहा गया और इस देश के शिक्षण संस्थानों मुख्यतया विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को अगुआ भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन आजादी के 74 वर्ष बाद एक सवाल फिर उठने लगा है कि क्या हमारे विश्वविद्यालय संविधान राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर पाए या नहीं ?
भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज मे एक राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरुरी था सभी समुदायों, जातियों, पंथ, लिंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म के लोगों को शामिल किया जाए और उनके ज्ञान और श्रम का उपयोग किया जा सके लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आदिवासी, वंचित शोषित और अल्पसंख्यकों को जनगणना रजिस्टर और मतदाता सूची में दर्ज एक नंबर तक सीमित कर दिया गया। उन्हें आंकड़ा बना दिया गया जिसका इस्तेमाल सिर्फ कोरे कागज को रंगने में किया गया। इस देश के विश्वविद्यालय इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं।
विश्वविद्यालय का मतलब एक ऐसी जगह जहां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आए हुए लोग अपने ज्ञान को अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं और देश दुनिया की बेहतरी के लिए नए ज्ञान का सृजन करते हैं। एक ऐसी जगह जहां सवाल पूछने, बहस, परिचर्चा, मतभेद की आजादी हो। तर्क, विज्ञान के सहारे समाज को आगे बढ़ाने कि बात हो जहाँ पाखंड, अन्धविश्वास को चुनौती दी जा सके। एक ऐसी जगह जहां दुनिया कि बेहतरी बनाने कि लड़ाई में रुकावट डालने वाली हर ताकत के खिलाफ वैश्विक विरोध तैयार होता हो।
भारत के संदर्भ में देखें तो कुछ अपवाद को छोड़ दें तो कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला। ज्यादातर शिक्षण संस्थान सामंती, जातिवादी और 1990 के बाद पूंजीवादी मूल्यों को आगे बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। इस देश के शिक्षण संस्थान अपनी स्थापना से लेकर आज तक खास जाति के कब्जे में रहे हैं उन्हें समावेशी बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई।
1950 के बाद राजनैतिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर विधानसभा-लोकसभा और अखिल भारतीय सेवाओं के स्तर पर आदिवासी और अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए आरक्षण को लागू कर दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालयों के स्तर पर इसे लागू नहीं किया गया। जिन विश्वविद्यालय को राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा करनी थी उनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व 1997 में पंजाब हाईकोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग को 2008 तक इंतजार कराया गया। इसके पूर्व अपवाद को छोड़ दें तो कुछ गिने चुने प्रोफेसर ही इन समुदायों से थे। आरक्षण लागू होने के बावजूद भी विश्वविद्यालयों में इन तबकों के लिए प्रवेश मुश्किल बना दिया गया।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 8 जुलाई 2020 में सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ लक्ष्मण यादव द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्न के जवाब में जानकारी देते हुए कहा की 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (इनसे संबद्ध कॉलेजों के आंकड़े शामिल नही हैं) में अन्य पिछड़ा वर्ग के 96.65%, अनुसूचित जनजाति के 93.98% और अनुसूचित जाति के 82.82% प्रोफ़ेसर पद रिक्त हैं। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर यह आंकड़ा ओबीसी 94.30%, एसटी 86.1% और एससी के 76.57% पद रिक्त हैं तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पर ओबीसी 41.82%, एसटी 33.47% और एससी 27.92% पद रिक्त हैं। 2021 में लोकसभा में सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा था की अखिल भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जनजाति 88% और अनुसूचित जाति के 49% पद, और इन्द्रिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली में अनुसूचित जनजाति 49% और अनुसूचित जाति 45% पद रिक्त हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, दलित और पिछड़ों के योगदान से रोकने और सामाजिक न्याय की हत्या हैं।
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय जिस इस देश का प्रगतिशिल और लोकतान्त्रिक कैम्पस कहा जाता रहा है और कई मायनों में है भी लेकिन जब मामला आदिवासी, दलित, पिछड़ों को हिस्सेदारी देने का या पढ़ने का मौका देने का आता है तब यह विश्वविद्यालय अपने जातीय और भाषायी चरित्र में अभिजात वर्ग के कब्जे वाला संस्थान नजर आता है। इसकी वजह ये रही कि जब कांग्रेस और वामपंथी राजनीति असरदार थी तब इसमें बैठे अधिकांश लोग उसी तरह का चोला ओढ़कर इन विश्वविद्यालयों में घुस गए और आजीवन अपने सजातीय, क्षेत्र, भाषायी लोगों को मौका देते रहे।
JNU ने 2007 मे अपनी “कार्यकारी परिषद (ई.सी) मे “यूजीसी गाइडलाइंस फॉर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी” के मद्देनजर एसटी & एससी को एसोसियेट और प्रोफेसर के स्तर पर और ओबीसी को असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पर आरक्षण लागू करने का फैसला किया लेकिन आरक्षण विरोधी खेमे के चलते 2010 तक उस पर अमल नहीं लिया गया। नवम्बर 2009 में जेएनयू के 30 आरक्षण विरोधी प्रोफेसरों ने जेएनयू एग्जिक्यूटिव कौंसिल को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आरक्षण को लागू करने के गंभीर परिणाम होंगे”। तत्कालीन वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखते हुए आरक्षण विरोधी खेमे में शामिल वाई.के. अलग, टी.के. ओमान और बिपिन चंद्र जैसे प्रोफेसरों ने कहा कि “जेएनयू जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स में असिस्टेंट और एसोसियेट स्तर पर आरक्षण लागू करने से भारतीय समाज के डिसएडवांटेज (वंचित) समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लोग निजी और विदेश विश्वविद्यालयों मे चले जाएँगे और वंचित तबका विश्व स्तरीय शिक्षा से महरुम हो जायेगा “।
प्रगतिशील और उदार माने जाने वाले इन तमाम प्रोफेसरों के जहन में ये बात थी कि जो लोग वंचित, शोषित तबके से आते हैं उनमें प्रतिभा नहीं होती है, प्रतिभा पर केवल सवर्ण जातियों, अंग्रेजी भाषी, कुलीनों का विशेषाधिकार है और यही लोग वंचित शोषितों का उद्धार कर सकते हैं। दरअसल मेरिट का यह लॉजिक मनुस्मृति का आधुनिक संस्करण है। जिसके माध्यम से आदिवासी, दलित और पिछड़ों को विश्वविद्यालय में घुसने से रोकना है ताकि सवर्ण वर्चस्व को चुनौती न दी जा सके।
जबकि मेरिट की अवधारणा सवर्ण जातियों के संदर्भ में बिल्कुल अलग है वहां आपका सजातीय होना ही काफी था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर स्वर्गीय नामवर सिंह ने अपने भाई काशीनाथ सिंह को 20 जुलाई 1976 को एक चिट्ठी (काशी के नाम पुस्तक मे संकलित है) में लिखा “प्रिय काशी, डॉ विजयपाल सिंह के सुपुत्र अशोक सिंह को बड़ी मुश्किल से समाजशास्त्र में प्रवेश दिला दिया। मुझे सपने में भी ख्याल न था कि यह लड़का इतना कमज़ोर होगा। इंटरव्यू में वह हिंदी के दो उपन्यासों के भी नाम न बता सका। प्रेमचन्द के बारे में दो शब्द न कह सका। लोग हैरान थे कि काशी विश्वविद्यालय का 75% अंक पाने वाला हिंदी एमए ऐसा है। बहरहाल, मैंने बात दी थी, तो बात रह गई। एहसान तो वे क्या मानेंगे, लेकिन ‘अपना पैगामे मोहब्बत है जहां तक पहुंचे’, तुम्हें लिख दिया कि सनद रहे और वक्त पर काम आए…”।
जेएनयू एडमिशन में वंचित शोषितों के साथ भेदभाव की यह नामवरी संस्कृति का इतिहास पुराना है जो आज भी बदस्तूर जारी है। हालांकि नवम्बर 1980 में उच्चतम न्यायालय की पी एन भगवती, वाई वी चन्द्रचूड, वी आर कृष्ण अय्यर, सैय्यद मुस्तफा फजल अली और ए डी कौशल की 5 सदस्यों कि संविधान पीठ ने कहा कि “मौजूदा हालत में कुल नम्बरों का 15% से अधिक मौखिक परीक्षा में नम्बर का दिया जाना न केवल अनुचित और मनमाना है बल्कि संवैधानिक रूप से अवैध है”।
लेकिन जेएनयू में एमफिल पीएचडी में एडमिशन के लिए साक्षात्कार अभी भी 30% है। जेएनयू प्रशासन द्वारा अलग अलग वर्षों में गठित प्रो. सुखदेव थोराट कमेटी 2011, प्रो राजीव भट्ट कमेटी 2013 और प्रो अब्दुल नफे कमेटी 2016 ने स्वीकार किया कि “साक्षात्कार में भेदभाव होता है” और साक्षात्कार का प्रतिशत 30 से घटाकर 15% करने का सुझाव दिया था। 2012 में जेएनयू छात्र संघ ने भी अपने पर्चे में विस्तार से इसे बताया। 2007-11 के आंकड़ों के आधार पर कहा कि साक्षात्कार में सामान्य वर्ग और आदिवासी तबके से आने वाले छात्र-छात्राओं के मामले में 27.9% से लेकर 37.4% प्रतिशत का अंतर है वहीं सामान्य वर्ग और दलित वर्ग के छात्र-छात्राओं के अंकों में 29.5% से 59.2% अंकों का अंतर हैं ओबीसी के संदर्भ मे यह 3.8 से लेकर 34.3% अंकों का अंतर है।
वर्ष 2021 पीएचडी प्रवेश परीक्षा के परिणामों में भी इसी तरह की धांधली देखी गई है जहाँ आदिवासी, दलित और पिछ्ड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को साक्षात्कार के 30 अंकों मे से 1 और 2 अंक देकर बाहर कर दिया गया है। जबकि लिखित परीक्षा के अंकों में इस तरह का अंतर नहीं है कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पाए और साक्षात्कार में 1 अंक दिए जाने के बावजूद उनका एडमिशन “आरक्षित” सीट पर हो गया है लेकिन यदि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता तो वो सब अनारक्षित सीटों पर प्रवेश पाते।
दरअसल जेएनयू जिसे प्रगतिशील और लोकतान्त्रिक विश्वविद्यालय माना जाता रहा है वह अब आदिवासी, दलित और पिछ्ड़े तबके कि प्रतिभाओं कि हत्या का केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे समय में जब देश में फासीवाद का हमला झेल रहा है और सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों पर पूंजीपति गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं ऐसे में वंचित शोषितों तबकों को विश्वविद्यालय से बाहर करके या उन्हें उनका वाजिब हिस्सा दिए बिना आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं ऐसे में बहुत जरूर है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए ताकि इस देश और समाज को लोकतान्त्रिक और समावेशी बनाया जा सके।
(डॉ. जितेंद्र मीणा दिल्ली विश्वविद्यालय के श्याम लाल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)