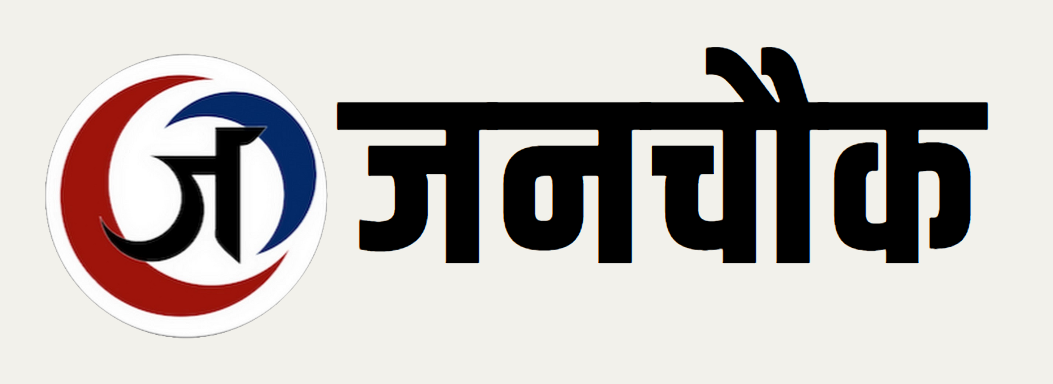जब दुनिया के अधिकांश धर्म और सभ्यताएं अपने विशेष पर्वों को उल्लास और उत्सव के रूप में मनाते हैं, तब मुहर्रम, विशेषकर उसका दसवां दिन ‘आशूरा’, एक अलग ही भावभूमि पर खड़ा दिखाई देता है। यह न तो किसी राज्य की स्थापना की स्मृति है, न किसी विजय का उत्सव; यह एक ऐसी वेदना की विरासत है, जो समय की सीमाओं को पार कर नैतिकता, प्रतिरोध और मनुष्यता के पक्ष में खड़ी होती है।
मुहर्रम न केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद है, बल्कि वह मानव चेतना की गहराई में बसी वह प्रेरणा है, जो बताती है कि कभी-कभी हारते हुए भी इंसान विजयी होता है, जब वह सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए मरता है।
इतिहास के पन्नों से: करबला का मर्म
सन 680 ई. में इस्लामी इतिहास के सबसे निर्णायक और दर्दनाक अध्याय की रचना हुई- करबला की त्रासदी। यह वह समय था जब इस्लाम एक राजनीतिक सत्ता में बदलता जा रहा था, और धर्म के मूल उद्देश्य- न्याय, करुणा, समानता जैसे मूल्य सत्तालोलुपता की भेंट चढ़ रहे थे।
पैगंबर मुहम्मद के नवासे इमाम हुसैन, जिनकी परवरिश न्याय, बराबरी और मानवता के उच्चतम मूल्यों में हुई थी, उन्होंने इस अधोगति के विरुद्ध खड़ा होना चुना। यज़ीद, जो अब उस उम्मयद साम्राज्य का ख़लीफा था, एक ऐसी सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था, जो बल, भय और भ्रष्टाचार से शासित थी।
हुसैन ने यज़ीद की बैअत यानी आज्ञाकारिता को यह कहकर अस्वीकार कर दिया —
“मेरे जैसा व्यक्ति यज़ीद जैसे व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता।”
यही अस्वीकार एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया। हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ यह जानते हुए कूफ़ा की ओर चले कि यह रास्ता शहादत की ओर जा सकता है। उन्हें करबला के रेगिस्तान में रोक लिया गया, पानी से वंचित किया गया, बच्चों तक को प्यासा रखा गया। और 10 मुहर्रम को उन्हें और उनके परिजनों को बेरहमी से शहीद कर दिया गया।
यह युद्ध संख्या का नहीं, मूल्य और नैतिकता का था। हुसैन हार गए, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। करबला ने बता दिया कि सत्ता की तलवारें सच्चाई को काट नहीं सकतीं।
करबला: मातम से आंदोलन तक का सफ़र
करबला की यह घटना इतनी सशक्त थी कि इतिहास में इसे दफ़्न नहीं किया जा सका। शुरुआत में अब्बासी और उमय्यद शासन ने इस स्मृति को कुचलने की भरपूर कोशिश की। परंतु, ग़म-ए-हुसैन लोगों के दिलों से कभी मिटाया नहीं जा सका। मातम, मजलिस, नौहे, मर्सिये- सबने इस घटना को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा।
ईरान में सफ़वी शासकों ने शिया इस्लाम को राजधर्म बना दिया, और तभी से मुहर्रम की रस्में सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गईं। ताज़िया, शबिह, सिपारा, और आलम अब धार्मिक कर्मकांड ही नहीं, सांस्कृतिक प्रतीक भी बन गए।
विविधताओं का संगम भारत मुहर्रम को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना के रूप में भी अपनाता आया है। लखनऊ, हैदराबाद, कश्मीर, कोलकाता, और छोटे कस्बों तक में मुहर्रम न केवल शिया मुसलमानों, बल्कि सुन्नी, हिंदू और सिख समुदायों द्वारा भी आदर से मनाया जाता रहा है।
यह परंपरा जंजीरों से आत्मवंचना का नहीं, बल्कि आत्मबलिदान की गौरवगाथा का उत्सव है, जो बताती है कि सत्य की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान भी दिया जा सकता है।
मुहर्रम: आत्मा की पुकार और समय से परे की स्मृति
करबला की स्मृति ने कभी केवल धार्मिक दायरे में सीमित रहना स्वीकार नहीं किया। यह एक ऐसी सार्वकालिक चेतना है, जो हर समय और समाज में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ देती है। हुसैन केवल शिया मुसलमानों के नायक नहीं हैं, वह हर उस इंसान के नायक हैं, जो ज़ुल्म के सामने झुकने से इनकार करता है।
गांधी जी ने हुसैन की प्रेरणा से सत्याग्रह को आकार दिया, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने करबला को क्रांति की चेतना में बदला, और आज भी दुनिया भर के आंदोलनों में “हुसैनी साहस” की मिसाल दी जाती है।
हुसैन का संदेश था:
“यदि तुम धर्म को नहीं मानते, तो कम से कम मनुष्यता का तो लिहाज करो।”
यह वाक्य आज भी धर्मांधता और अमानवीयता के शोर में एक नैतिक गूंज बनकर जीवित है।
करबला: सत्ता के खिलाफ ज़मीर की आवाज़
हुसैन की लड़ाई किसी तख़्त के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा था —
“मैं इसीलिए निकला हूं ताकि अपने नाना की उम्मत में सुधार कर सकूं।”
यह सुधार सत्ता के तलवार से नहीं, ज़मीर और न्याय के रास्ते से आना था। इसीलिए करबला की लड़ाई कोई भू-राजनीतिक घटना नहीं थी; वह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और नैतिक युद्ध था, जिसमें अकेलेपन में भी हुसैन विजयी हुए।
आज जब दुनिया भर में धार्मिकता का नाम लेकर अत्याचार किए जाते हैं, जब मज़हब सत्ता का औज़ार बनता जा रहा है, तब करबला की याद हमें रोकती है, टोकती है और पूछती है- “क्या तुम हुसैनी हो या यज़ीदी?”
मुहर्रम- प्रतिरोध का वैश्विक प्रतीक
मुहर्रम आज केवल एक रस्म नहीं, एक जीवंत प्रतिरोध की वैश्विक चेतना है। यह बताता है कि इतिहास केवल बादशाहों द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि उन लोगों के आंसुओं से भी लिखा जाता है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं।
“या हुसैन” की सदा केवल शोक नहीं है, यह वह पुकार है जो हर युग में हर निर्दोष, शोषित और सताए हुए इंसान के दिल से उठती है।
हुसैन हमें सिखाते हैं कि अगर किसी को सत्ता मिले भी, लेकिन वो नैतिकता खो दे, तो वह अंततः हार ही जाता है।
हुसैन हमें यह भी सिखाते हैं कि सत्य के लिए मरने वाला कभी मरता नहीं, वह इतिहास का स्थायी आदर्श बन जाता है।
मुहर्रम की स्मृति हमें इस आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है कि हम अन्याय के साथ खड़े हैं, या उसके विरुद्ध ? क्या हम सत्ता के अंधकार में आंखें मूंदे हुए हैं, या करबला की रोशनी में सत्य को पहचान पा रहे हैं ?
करबला का रास्ता कठिन है, लेकिन यही मनुष्यता का असली रास्ता है।
यही है मुहर्रम की वास्तविक विरासत-एक दुखद स्मृति, जो हमें सबसे सुंदर और साहसी बनाती है।
(उपेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं।)