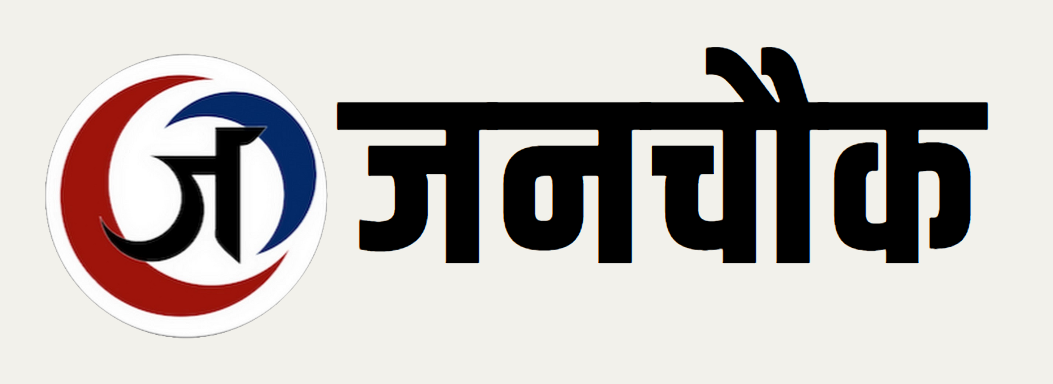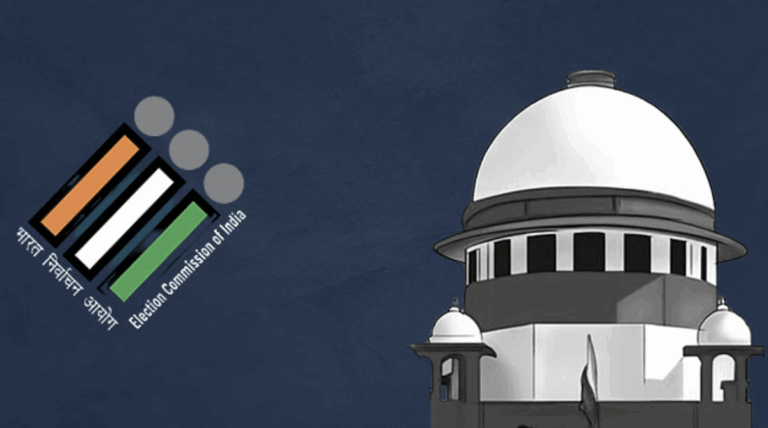भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना ने मीडिया में बढ़ती सांप्रदायिकता पर चिंता जता कर अच्छी पहल की है। इससे देश के विभिन्न संस्थानों को एक संदेश जाएगा और मीडिया को भी आइना देखने का मौका मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतने से सांप्रदायिकता जैसी जटिल समस्या का हल निकल आएगा यह सोचना दिवास्वप्न देखने जैसा है। ऐसा सोचना वैसे ही है जैसे कभी कभी अदालतें और चुनाव आयोग सोचते हैं कि कुछ आदेशों के पारित कर देने और बंदिशें लगा देने से राजनीति का अपराधीकरण मिट जाएगा। यह तो वैसा ही हुआ जैसे समस्या की जड़ को जानने की बजाय उसकी फुनगी को पकड़ कर समाधान निकाला जाए।
सांप्रदायिकता की समस्या का हल तभी निकल सकता है जब हम यह समझें कि वह उत्पन्न कहां से होती है और उसका समाधान कौन कर सकता है ? सांप्रदायिकता की समस्या समाज के मानस की वह समस्या है जिसे सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा निर्मित किया जाता है। इसलिए उसका समाधान उस मानसिकता को दूर करना है जो सांप्रदायिक होती है। अगर उसका समाधान बहुसंख्यकवादी सत्ता से निकालने को कहा जाएगा तो यह तो भेड़िए से बकरी की रखवाली करने जैसी बात हुई। सांप्रदायिकता की उत्पत्ति उस प्राकृतिक प्रवृत्ति से होती है जहां जीव-जंतुओं के सभी समुदायों में अपने कुटुंब की रक्षा की प्रवृत्ति होती है। ऐसा करते हुए वह समुदाय दूसरे समुदाय से अपनी दूरी बनाता है और उसके विरुद्ध एक तरह की गोलबंदी रखता है। लेकिन जब राष्ट्रीयता और नागरिकता का निर्माण होता है तब मनुष्य इस प्रवृत्ति से मुक्त होने लगता है और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा की बजाय पारस्परिक सहयोग का वातावरण निर्मित करता है।
लेकिन जिन राष्ट्रीयताओं और नागरिकताओं के निर्माण में पारस्परिक सहयोग निर्मित नहीं हो पाता वहां सांप्रदायिकता की समस्या विकट हो जाती है और वह देश को कमजोर करती है। जहां राष्ट्रीयता का निर्माण पारस्परिक विश्वास, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टि के माध्यम से माध्यम से होता है, वहीं सांप्रदायिकता का निर्माण पारस्परिक अविश्वास, नफरत, प्रतिस्पर्धा, असहिष्णुता और अतार्किकता और अवैज्ञानिक दृष्टि के माध्यम से होता है। राष्ट्रीयता अगर सामाजिक ताने बाने को सुलझाती है तो सांप्रदायिकता उसे उलझा देती है। राष्ट्रीयता जहां आत्म बलिदान के लिए प्रेरित करती है वहीं सांप्रदायिकता दूसरे की जान लेने की सीख देती है। राष्ट्रीयता मित्रता निर्मित करती है तो सांप्रदायिकता शत्रुता पहले बनाती है और उसकी प्रेरणा से मित्रता का निर्माण करती है। राष्ट्रीयता का आख्यान तैयार करने में मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। कभी वह अपने और पराए के आधार पर उसे बनाता है तो कभी कुछ मूल्यों के आधार पर। आमतौर पर सांप्रदायिकता का विलोम धर्म निरपेक्षता यानी सेक्यूलरिज्म को माना जाता है लेकिन भारत के संदर्भ में यह जरा अलग हटकर है। यहां सेक्यूलरिज्म कायम होने की बजाय सर्वधर्म समभाव की स्थापना करने पर ज्यादा जोर रहा है। यहां कई धार्मिक व्यक्ति अपने व्यवहार में एकदम सांप्रदायिक नहीं थे जबकि कई नास्तिक लोग अपने व्यवहार और सिद्धांत में घनघोर सांप्रदायिक निकले।
रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद धार्मिक होकर भी सांप्रदायिक नहीं थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना, विनायक दामोदर सावरकर नास्तिक होकर भी सांप्रदायिक थे। भक्ति आंदोलन ईश्वर में यकीन करने वाला था, लेकिन वह सांप्रदायिकता को मिटाने वाला था। 1857 की क्रांति धार्मिक आधार पर खड़ी हुई लेकिन उसके भीतर गजब का सर्वधर्म समभाव था। लेकिन जैसे-जैसे आजादी की लड़ाई आगे बढ़ती गई उसमें सांप्रदायिकता प्रवेश पाती गई। जबकि लड़ाई आगे बढ़ने के साथ उसमें नागरिक अधिकारों और आधुनिक शासन प्रणाली की मांग के साथ सेक्यूलर विचारों का प्रवेश हो रहा था। भारत की सांप्रदायिक समस्या पर वैसे तो देश के हर चिंतक, समाजशास्त्री और महापुरुष ने कोई न कोई टिप्पणी जरूर की है, लेकिन उस बारे में 1931 की भगवान दास कमेटी की रपट ध्यान देने लायक है। कांग्रेस ने कानपुर दंगों और उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या के बाद भगवान दास की अध्यक्षता में सांप्रदायिक समस्या की जांच के लिए समिति बनाई थी। यह रपट कहती है कि इतिहास की सकारात्मक समझ, समन्वयपूर्ण रहन-सहन और राजनीतिक सामाजिक ढांचे के नवनिर्माण के प्रयास के बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मीडिया के एक हिस्से में यह प्रवृत्ति देखी है कि वह हर चीज को सांप्रदायिक नजरिए से देखता है। जबकि भारत के सोलीसिटर जनरल यानी सरकार के वकील तुषार मेहता इस दृष्टिदोष का हल कुछ पुराने और कुछ नए कानूनों में देखते हैं। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की बात को अखबारों और विशेषकर हिंदी अखबारों ने तो वेब पोर्टल पर डाल दिया है। जबकि सांप्रदायिक नजरिए से हर चीज को देखने और प्रस्तुत करने में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया और डिजिटल मीडिया सभी का बराबर का हिस्सा है। सांप्रदायिकता के इस हमाम में हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और व्यापक समाज नंगा खड़ा है।
जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में व्याप्त सांप्रदायिकता पर सरकार (और व्यापक समाज) का ध्यान खींचा है उससे एक दिन पहले एक हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव देते हुए जो टिप्पणियां की हैं उससे लगता है कि सांप्रदायिकता के एजेंडे को बढ़ाने में न्यायपालिका की भी अपनी भूमिका है। यह दावा करना कि सिर्फ गाय ही ऐसा पशु है जो आक्सीजन की सांस लेता है और उसे छोड़ता भी है अपने आप में अवैज्ञानिक दावा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकृति में सारे जीवों के उच्छवास में आक्सीजन की कुछ न कुछ मात्रा रहती है। अब दिक्कत यह है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली टिप्पणी पर हिंदी के ज्यादातर अखबारों ने समर्थन में संपादकीय लिखे हैं। लेकिन शायद ही हिंदी का कोई अखबार हो जिसने उस टिप्पणी की वैज्ञानिकता पर सवाल उठाया हो। सभी को पंचगव्य बड़ा पवित्र लगता है। इसलिए यह कहना कि सांप्रदायिकता सिर्फ वेब पोर्टल फैला रहे हैं गलत है। उसे फैलाने में हिंदी के अखबारों और चैनलों का भारी योगदान है।
मीडिया के सांप्रदायीकरण की यह शुरुआत 1977 में ही हो गई थी। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो लालकृष्ण आडवाणी देश के सूचना और प्रसारण मंत्री बने। उन्होंने राष्ट्रीय अखबारों में बड़े पैमाने पर उन लोगों की भर्ती करवाई जो संघ परिवार से जुड़े थे। उससे बाद अस्सी के अंत और नब्बे के दशक में जब सांप्रदायिकता उभार पर आई तो विभिन्न राज्य सरकारों और हिंदुत्व समर्थक अफसरों से सहयोग पाकर मीडिया में संघ से प्रशिक्षण पाए पत्रकार घुस चुके थे। जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी ने भले ही बाबरी मस्जिद विध्वंस का विरोध किया और अपने आखिरी दिनों में सेक्यूलर छवि निर्मित करने में सफल रहे लेकिन उनके चारों ओर हिंदुत्ववादियों का जमावड़ा था। संघ परिवार से जुड़े पत्रकार उनके विशेष कृपापात्र भी रहे। आज वे सब पत्रकारिता के विभिन्न संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों पर कब्जा जमाकर बैठे हैं और मीडिया में नियुक्ति से लेकर उसकी सामग्री के चयन और प्रसारण में एकांगी दृष्टि को प्रमुखता प्रदान किए हुए हैं। बल्कि अगर यह कहें कि संघ की आलोचना करने वालों के लिए अब मुख्यधारा के मीडिया में जगह नहीं बची तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।
सुरेंद्र प्रताप सिंह जो कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं उनके तमाम शिष्य हिंदुत्ववादी ही निकले। लेकिन सांप्रदायिकता का यह डीएनए आया कहां से इसके बारे में किसी एक तबके और हिस्से को दोष देना अनुचित होगा। राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी कहते हैं कि चुनावी खेल से निकली सांप्रदायिकता। आशीष नंदी इसके लिए आधुनिकता को जिम्मेदार बताते हैं और समुदायवाद की ओर लौटने की सीख देते हैं। गांधी जी कहते थे कि धर्म की गलत समझ से पैदा होती है सांप्रदायिकता। कई विद्वानों का मत है कि जिस समाज में व्यक्ति अधिकारों का महत्व नहीं होता वहीं ऐसी समस्या जन्म लेती है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहती है कि मीडिया में सांप्रदायिकता बढ़ रही है और सरकार कहती है कि हमने कानून बनाए हैं तो यह न तो समस्या पर मुकम्मल बयान है और न ही उसका मुफीद इलाज।
इसके बावजूद नब्बे के दशक और इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में मीडिया के भीतर सांप्रदायिकता का विरोध करने की हिम्मत थी क्योंकि तब सत्ता में एक ऐसा गठबंधन था जो खुले तौर पर बहुसंख्यकवादी नहीं था। उस समय मीडिया भी सांप्रदायिकता के विरोध का साहस जुटा लेता था और वैसे लोगों को निशाने पर रखता था जो दंगा कराते थे या सांप्रदायिक टिप्पणियां करते थे। लेकिन 2014 के बाद मीडिया का वह साहस कमजोर होता गया। कभी इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा को खामोश करा दिया जाता है, तो कभी एनडीटीवी पर कार्रवाई करके उसे बदल दिया जाता है। अब तो चैनलों के पैनल सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यालय से तय होते हैं। वरना 2014 से पहले तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाली बहसें भी कराता था।
भारत में सांप्रदायिकता की समस्या निश्चित तौर पर उस मीडिया में ज्यादा दिखती है जो धनतंत्र और राजनीति तंत्र का भोंपू बन गया है और वही बोलता है जो सत्ता में बैठे लोगों को अनुकूल लगता है। लेकिन सांप्रदायिकता की बीमारी व्यक्ति के मानस में, परिवार के मानस में, समाज के मानस में और उनसे निकल कर बने राजनीतिक और धार्मिक संगठनों में घर कर चुकी है। वह लगातार फैल रही है और संभव है कि आने वाले कुछ समय में समाज, उसकी संस्थाएं और संविधान उतना भी कहने की स्थिति में न हो जितना आज भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है। संगठित राजनीति, संगठित धर्म और एकाधिकारवादी पूंजी ने अद्भुत गठजोड़ बनाया है। वे सांप्रदायिकता को बढ़ाने के खेल में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और लोकतंत्र के मूल्यों को हराकर अपनी पार्टी, अपने धर्म और अपनी पूंजी की विजय पताका फहराने में लगे हैं। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को निर्देश देने और डराने की बजाय उनकी सहमति से नीतियां बननी चाहिए और सरकारें चलनी चाहिए। लेकिन अब इससे ठीक विपरीत आचरण हो रहा है और मीडिया उसे सही बता रहा है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमें सचेत करती है। यह टिप्पणी उसी तरह से सावधान करती है जैसे कि इकबाल ने कहा था कि वतन की फिक्र कर नादां कयामत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। तेरी दास्तां भी न होगी दास्तानों में।
(अरुण कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)