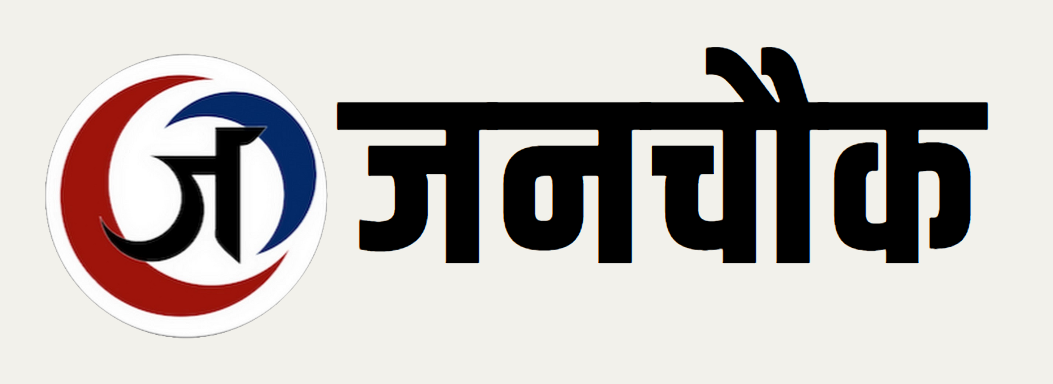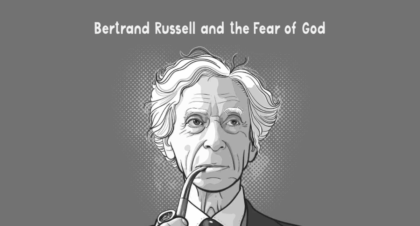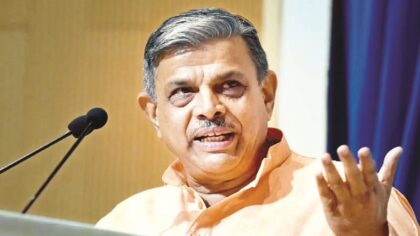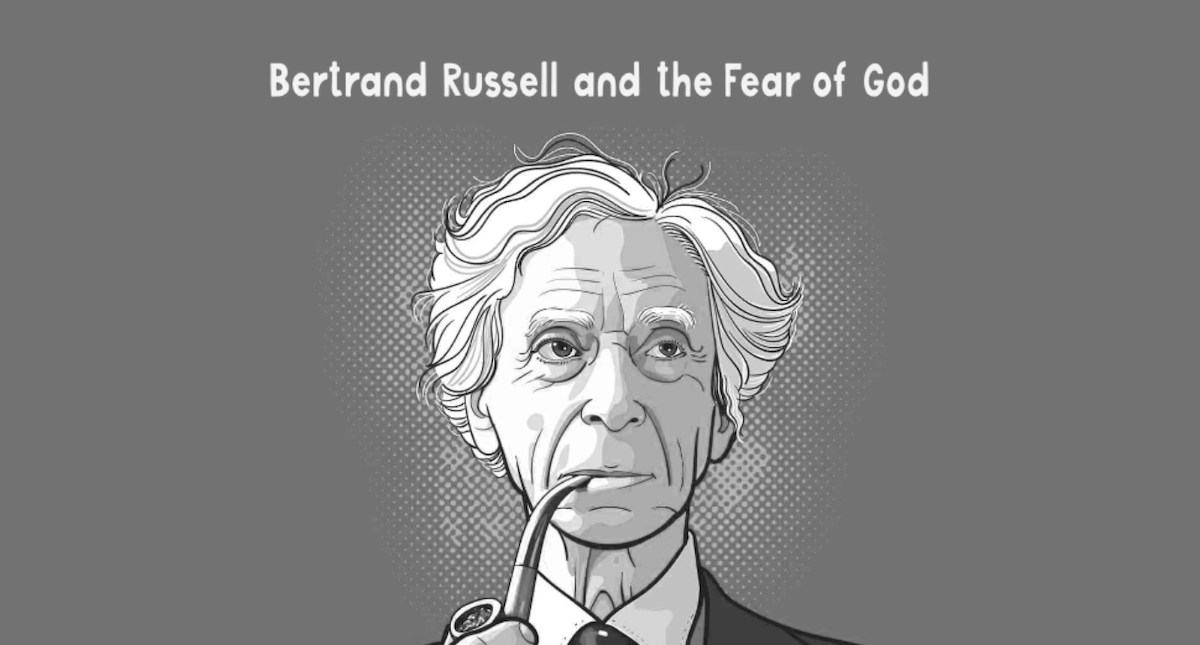बर्ट्रेंड रसेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Religion and Science सन 1935 में लिखी थी, जब दुनिया धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक सोच के बीच तीव्र संघर्ष से गुज़र रही थी। रसेल ने साहसपूर्वक यह सवाल उठाया था कि क्या धार्मिक मान्यताएं, विशेषकर संगठित धर्म, मनुष्य के ज्ञान और प्रगति के मार्ग में बाधा बन रही हैं? लगभग एक शताब्दी बाद, भारत जैसे देश में जहां एक ओर विज्ञान और तकनीक तेज़ी से आगे बढ़ रही है और दूसरी ओर धार्मिक आस्थाएं जनजीवन में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि रसेल ने अपनी किताब में जो विचार सामने रखे थे,वे क्या आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं?
तर्क बनाम आस्था: एक शाश्वत संघर्ष
रसेल का मूल तर्क यह था कि जब धर्म तर्क और प्रमाण पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ टकराता है, तो वह ज्ञान के विकास को बाधित करता है। उन्होंने इसके लिए गैलीलियो के उत्पीड़न से लेकर विकासवाद के विरोध तक के ऐतिहासिक उदाहरण दिए हैं। मगर भारत में तो यह संघर्ष आज भी जारी है।
जब विज्ञान की बातें धार्मिक आस्थाओं से टकराती हैं, तब कई बार भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ‘भारतीय संस्कृति का अपमान’ बताकर खारिज कर दिया जाता है। यहां तक कि स्कूली पाठ्यक्रमों से डार्विन के सिद्धांत को हटाने की कोशिशें हो चुकी हैं, और कई मंचों पर यह दावा किया गया है कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी, परमाणु बम और विमान पहले से मौजूद थे। इस तरह के दावे दरअसल रसेल के उसी डर की पुष्टि करते हैं कि जब पौराणिक कथाओं को तथ्य बना दिया जाता है, तब वैज्ञानिक सोच हास्यास्पद और हाशिए पर चली जाती है।
राजनीति और धर्म का खतरनाक गठजोड़
रसेल ने आगाह किया था कि जब धर्म सत्ता से जुड़ जाता है, तब वह विचार स्वतंत्रता को कुचल देता है। भारत में आज यही देखने को मिल रहा है। धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति केवल चुनावी लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज को दो हिस्सों में बांटने का औज़ार भी बन चुकी है।
जब कोई वैज्ञानिक या लेखक किसी धार्मिक प्रथा की आलोचना करता है,चाहे वह मंदिर में महिलाओं की एंट्री हो, तीन तलाक़ हो या जातिगत भेदभाव,तो उसके ख़िलाफ न केवल सामाजिक बहिष्कार, बल्कि हिंसा तक की घटनाएं सामने आती हैं। डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या इसका ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे में रसेल की चेतावनी और अधिक गंभीर लगती है।
विज्ञान, नैतिकता और मानवीय जिम्मेदारी
रसेल ने यह भी कहा था कि विज्ञान बिना नैतिकता के ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन उस नैतिकता का आधार धर्म नहीं, बल्कि तर्क और मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। भारत में जहां डिजिटल निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आनुवांशिक शोध जैसे तकनीकी विकास तेज़ है, वहीं नैतिक बहसें न के बराबर हैं।
आधुनिक विज्ञान से जुड़े सवालों जैसे निजता, पर्यावरण, डेटा सुरक्षा, या सामाजिक विषमता पर न तो धार्मिक संस्थाएं कोई स्पष्ट दिशा देती हैं और न ही सरकारें इन विषयों पर गंभीर बहस को प्रोत्साहित करती हैं। ऐसे में रसेल का यह प्रश्न आज भी भारत के लिए प्रासंगिक है कि क्या विज्ञान मानव कल्याण के लिए काम कर रहा है या केवल मुनाफे और नियंत्रण का उपकरण बन गया है?
शिक्षा का क्षेत्र: संघर्ष की सबसे बड़ी ज़मीन
रसेल मानते थे कि शिक्षा वह क्षेत्र है, जहां धर्म और विज्ञान के बीच टकराव या सामंजस्य तय होता है। भारत में यह संघर्ष साफ दिखाई देता है। एक ओर तो वैज्ञानिक सोच को संवैधानिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(h) के रूप में मान्यता मिली है, दूसरी ओर स्कूली पाठ्यक्रमों को धार्मिक या राजनीतिक नजरिए से बार-बार बदला जा रहा है।
इतिहास के पाठों को धार्मिक गौरव गाथा में बदला जा रहा है, और सामाजिक विज्ञान को धार्मिक कट्टरता के रंग में रंगा जा रहा है। ऐसे में प्रश्न है कि बच्चों में तर्कशीलता और विवेकशीलता कैसे पनपेगी?
भारत की विशेषता: समन्वय की परंपरा
हालांकि, भारत का सांस्कृतिक इतिहास केवल टकराव की कहानी नहीं है। यह वह देश है, जहां चार्वाक जैसे भौतिकवादी विचारक भी हुए हैं और बुद्ध, नानक, कबीर, अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने धर्म की आलोचना कर नैतिकता की नई परिभाषाएं भी दी हैं। भारत की परंपरा में प्रश्न पूछने और सुधार की गुंजाइश रही है, जो पश्चिमी धर्म की जड़ता से अलग है।
इसलिए, भारत में रसेल की चेतावनी को स्वीकार करना धर्म को नकारना नहीं है, बल्कि धर्म को एक मानवीय, तर्कसंगत और प्रगतिशील दिशा में ले जाना है।
रसेल आज भी क्यों जरूरी हैं ?
Religion and Science आज भी एक ऐसा दर्पण है, जिसमें भारत अपने भीतर झांक सकता है। यह पुस्तक एक चेतावनी है कि अगर धर्म वैज्ञानिक सोच, सामाजिक न्याय और विचार स्वतंत्रता के रास्ते में आएगा, तो वह मनुष्य के कल्याण का नहीं, विनाश का कारण बन जाएगा।
भारत को न तो धर्म से भागना है और न ही विज्ञान को अंध भक्ति से ढक देना है। हमें रसेल की तरह नैतिक साहस दिखाना होगा- धर्म और विज्ञान दोनों से सवाल पूछने का साहस, और सत्य को सर्वोपरि मानने का विवेक।
(उपेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं।)