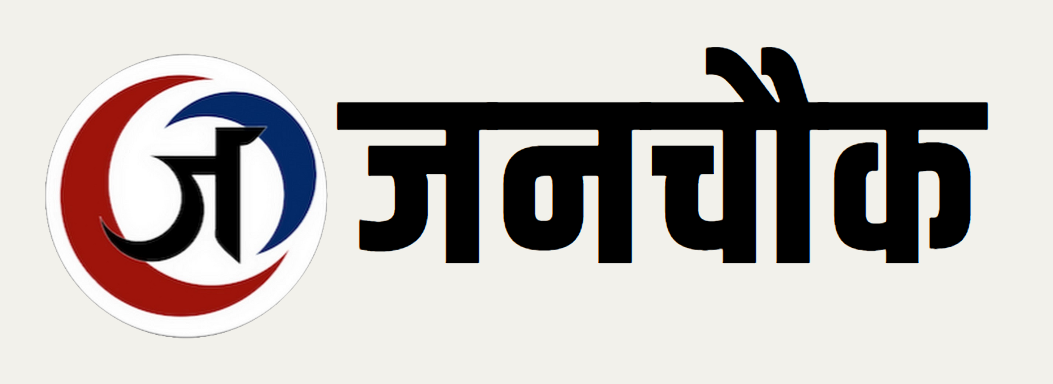आजादी के पचहत्तर वर्ष पूरे होने का जश्न एक तरफ बड़े उत्साह और कहीं-कहीं उन्मत्तता के साथ भी मनाया गया, वहीं हाल ही में ऐसी घटनाएँ भी हुईं, जिनसे यह भी इशारा मिला कि जिस आजादी और लोकतंत्र के ढोलक हम बजा रहे हैं, उनसे हमारा सामाजिक जीवन अभी अछूता ही रह गया है।
राजस्थान की घटना बड़ी भयावह थी। एक नन्हें बच्चे को उसके हेड मास्टर ने सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस मटकी को छू लिया था जो उस बच्चे की ‘नीच जाति’ वालों के लिए नहीं थी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पिछली 2 अगस्त को एक सरकारी स्कूल टीचर ने एक दलित बच्ची को इसलिए बेतरह पीटा क्योंकि वह आगे की बेंच पर बैठ गई थी। बच्ची बारहवीं कक्षा में पढ़ती थी। जुलाई महीने की एक खबर के अनुसार हापुड़ जिले के उदयपुर गाँव में एक प्राथमिक स्कूल की दो दलित छात्राओं के यूनिफार्म को शिक्षिकाओं ने उतरवा दिया था और उनको दो अन्य छात्राओं को दे दिया था ताकि वे अपनी तस्वीर खिंचवा सकें।
बाद में छात्राओं के अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षिकाओं को निलंबित करने के आदेश जारी हुए थे। इस तरह के न जाने कितने उदाहरण मिलेंगे। करीब दो हफ्ते पहले नेल्लोर में वाईएसआर कांग्रेस के नेता द्वारा ‘प्रताड़ित’ किये जाने के बाद एक दलित युवक ने आत्महत्या कर ली। अभी हाल ही में, मुजफ्फरनगर के ताजपुर गाँव में ग्राम प्रधान ने एक दलित युवक को भीड़ के सामने चप्पलों से मारा। पिछले कुछ महीनों में कई जगह ऐसा हुआ। महोबा, हापुड़, मुजफ्फरनगर—ये सिर्फ जगहों के नाम हैं। उस ज़हर का जो जातिवाद के नाम पर फैला है, उसका कोई विशेष नाम नहीं, कोई ठिकाना नहीं। यह कहीं भी, कभी भी कोबरा बन कर किसी को डंस सकता है।
आजादी का ‘अमृत’ बरस रहा है कि नहीं इसे तो लोग अपने व्यक्तिगत, सामाजिक अनुभवों पर ही बता सकते हैं, पर जातिवाद के विष का बादल पूरे देश में कहीं भी, कभी फट सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अछूत जैसे रुग्ण शब्द से तो सभी परिचित हैं, पर किसी समय में इस देश में ऐसी भी जातियां रही हैं, जिन्हें देखना भी वर्जित था। बीसवीं सदी की शुरुआत में ही केरल को स्वामी विवेकानंद ने ‘जातिवाद का पागलखाना’ कहा था। वहां पर कुछ लोगों को सिर्फ दिन के बारह बजे बाहर निकलने की अनुमति थी क्योंकि उस समय उनकी परछाई दूर तक नहीं फैलती थी। उनकी परछाई भी किसी ‘ऊंची जाति’ वाले को छू जाए, तो वह अशुद्ध हो जाता था। उन्हें अपनी गर्दन में एक घंटा लटका कर निकलना पड़ता था और उसे लगातार बजाते रहना पड़ता था, जिससे सवर्ण दूर से ही उनके आने की आहट पा जाएँ और दूर हो जाएँ।
आज भी ये बातें सच हैं, दूर के गावों में हैं, इक्का-दुक्का हैं, ख़बरों में नहीं आतीं, पर उनकी जड़ें बरसों से हमारे सामूहिक मन में बनी हुई हैं। राजनीतिक परिवर्तन जल्दी-जल्दी होते हैं। हर पांच साल में एक नया ‘मसीहा’आता है और हम सोचते हैं हमारा जीवन बदल जाएगा। पर लोकतंत्र की सुरभि न ही हमारे सामाजिक आचरण का स्पर्श करती है न ही परिवार और शिक्षा जैसी समाज की अन्य संस्थाओं का। रंग बिरंगे उत्सवों की नीचे हम इस तरह की बदरंग भद्दगियों को बड़ी कुटिलता के साथ छिपा ले जाते हैं।देश का छात्र कई तरह के हादसों का शिकार होता है जिसे आसानी से टाला भी जा सकता था। पर सबसे अधिक फ़िक्र जाति, धर्म के नाम पर शैक्षणिक संस्थानों के भीतर ही उनके साथ साथ भेदभाव किये जाने की घटनाओं को लेकर होती है।
शैक्षणिक संस्थानों की बहुत कीमती भूमिका है कि वे वर्तमान और भविष्य की ऐसी पीढ़ियां तैयार करें जिनमें जिम्मेदार और कुशल लोग हों, उनके पास ज्ञान और समझ दोनों हो, सकारात्मक दृष्टिकोण और सह-अस्तित्व की गहरी भावना हो। यदि स्कूल और कॉलेज ही हिंसा के केंद्र बन जायेंगे, चाहे वे दूसरों के प्रति हो, या स्वयं के प्रति; बिल्कुल शुरुआती स्तर पर ही जातिवाद, सम्प्रदाय, नस्लवाद और स्त्री संबंधी विषाक्त बातें शिक्षक छात्रों तक और छात्र एक दूसरे तक पहुंचा देंगे, तो ऐसे में देश और समाज का भविष्य तो गहरे अँधेरे में ही ड़ूब जाएगा। बचपन में ही यदि इस तरह के अनुभव हों तो वे बच्चों के अचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर हिंसा, मारपीट वगैरह उन्हें सामान्य आचरण की तरह प्रतीत होने लगता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षकों को एक ऐसा आदर्श बनने की ज़रूरत है, जो इन बीमारियों से ऊपर उठ चुका हो, या कम से कम ऊपर उठने का ईमानदार प्रयास कर रहा हो।
हमारी आबादी का एक तिहाई हिस्सा अपने हर दिन का बड़ा हिस्सा स्कूल या कॉलेज में बिताता है। यह समय उनको समझने, समझाने और उनमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाने के लिए सबसे सही है। यही समय है जब शिक्षक बच्चों को बौद्धिक लब्धि (आई क्यू) के साथ भावनात्मक लब्धि (ई क्यू) के महत्व के बारे में बता सकता है। एक लोकतंत्र में रहने वाले लोग अलग-अलग हो सकते हैं, पर वे विभाजित नहीं। विभाजित कौमें सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकतीं।
उनके पास कई तरह की आजादियां हैं जिन्हें संविधान परिभाषित करता है वगैरह। इस तरह की समझ किताबों की पढ़ाई के साथ-साथ भी दी जा सकती है। पर इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण उन लोगों के द्वारा जरूरी है जो शिक्षा के इस आयाम को गहराई से समझते हैं, इस दिशा में उन्होंने काम किया है।विकसित देशों ने इन सभी जरूरतों को समझा है और उनमें से कई ने इन मुद्दों पर सजगता के साथ काम भी किया है। फ़िनलैंड का एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है।
फ़िनलैंड जैसे देशों में इस बात का महत्व बखूबी समझा गया कि देश के विकास के लिए लोगों में सही समझ पैदा करना बहुत जरूरी है। शैक्षणिक संस्थानों ने ख़ास तौर पर स्टडी मॉडल और प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार किये जिनकी मदद से बच्चों में व्यवहार, सोच एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन आ सके। इन कार्यक्रमों को तैयार करने में अभिभावक, नेता, शैक्षणिक संस्थान, राजनीतिक दल और समाज सेवी संगठन सभी शामिल हुए। सवाल यह है कि क्या हम अपने शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों और छात्रों में इस तरह का अंदरूनी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। क्या इसके लिए हमारे पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है या फिर हम इस तरह के परिवर्तन इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि इसके राजनीतिक नुकसान हैं? जाति के नाम पर वोट लूटने की आदत इतनी पुरानी और इतनी फायदेमंद है कि उसे ख़त्म करने में राजनीतिक दलों का ही नुकसान है। तो उसके खात्मे की बात तो की जा सकती है, पर उसे ख़त्म करना एक बिलकुल अलग बात है।
शिक्षकों का बौद्धिक और नैतिक स्तर (सामाजिक, परंपरागत अर्थ में नहीं, बल्कि गहरे अर्थ में) बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही संस्थान में काम करने वाले अन्य कर्मियों के साथ भी नियमित रूप से बातचीत की जानी चाहिए। जातिवाद और साम्प्रदायिकता के ज़हर को फैलाने का काम ये भी खूब करते हैं। शिक्षकों के किये-धरे पर पानी फेरना इनके बाएं हाथ का खेल है। बुनियादी रूप से यह प्रक्रिया शिक्षक की समझ और प्रशिक्षण से शुरू होती है।
उनकी दिलचस्पी होनी चाहिए इस बात में कि समाज में गहरे बदलाव आयें। जातिवाद और साम्प्रदायिकता का ज़हर शांत हो। समानता, आजादी, भाईचारे में उनकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए, सिर्फ बौद्धिक और मौखिक नहीं। शैक्षणिक संस्थान के बाकी गैर-शिक्षक कर्मियों में यह समझ लाने का काम भी शिक्षक ही कर सकते हैं, यदि वे लगातार सतर्क और सजग रहें। स्कूल कॉलेजों को इन मूल्यों को सम्प्रेषित करने के लिए लगातार अभिभावकों के संपर्क में रहने की ज़रूरी है। यह काम वे ऑफ लाइन बैठकों या फिर डिजिटल माध्यमों से भी कर सकते हैं। इन दोनों का भी समय समय पर उपयोग किया जा सकता है।
दुर्भाग्य से शिक्षा डिग्रियां बटोरने और नौकरी पाने का एक माध्यम भर बन कर रह गई है। इन चीज़ों की अपनी सीमित भूमिका है, पर ह्रदय के संवर्धन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में गांधी जी ने बातें भी की थीं, और व्यावहारिक स्तर पर काम भी किया था। सही शिक्षा को सामाजिक विभाजन दूर करने के प्रयास करने चाहिए। छात्र को नए माहौल, लगातार बदलते हुए जीवन, नाकामयाबी, कामयाबी और विनम्रता, दुश्चिंताओं और अवसाद के साथ जीना सिखाने का काम भी स्कूलों, अभिभावकों और पेशेवर मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है।
शिक्षा संस्थान को कभी भी धर्म, जाति, क्षेत्र और रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना है, इसे सरकार, शिक्षा बोर्ड और संस्थान के प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा। इस तरह की घटनाएँ हो भी जाएँ तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बाकी छात्र इन बातों से प्रभावित न हो पाएं। इससे निपटने के तुरंत उपाय शुरू किये जाने चाहिए जिनसे उनके दिलो-दिमाग पर पड़े नकारात्मक प्रभाव को मिटाया जा सके।
चैतन्य नागर पत्रकार, लेखक और अनुवादक हैं। आप आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)