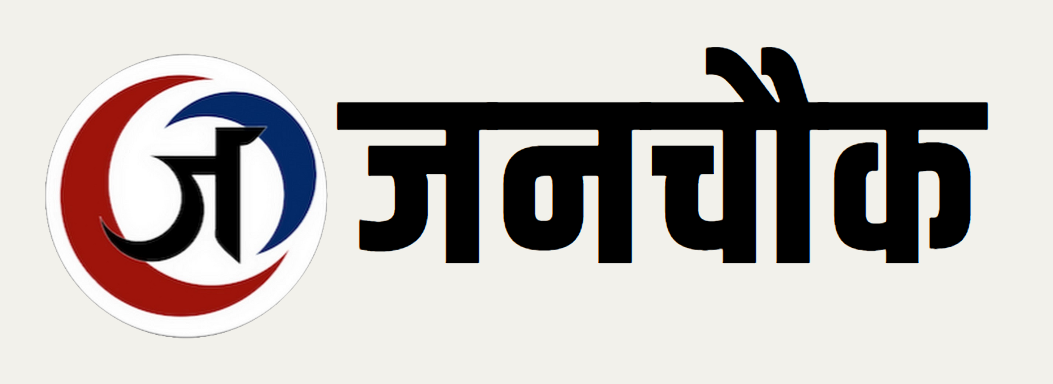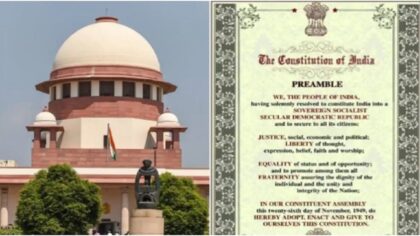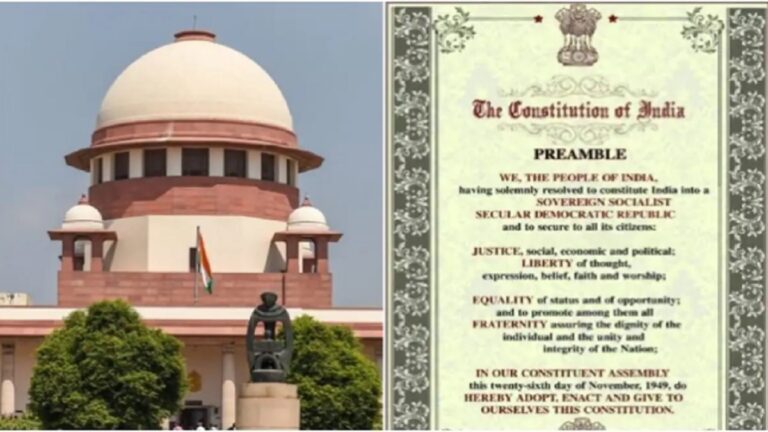व्यक्ति हो, धर्म हो या राष्ट्र, जब अपनी कमियों को जानने-समझने और सुधारने का काम छोड़ कर दूसरों की कमियों को उजागर करने लगता है तो समझना चाहिए कि उसके आगे बढ़ने का रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। क्योंकि वह अब दूसरों की कमियों का उल्लेख करके अपनी कमियों को वाजिब ठहराना शुरू कर चुका होता है।
ज्ञान-विज्ञान रोज-ब-रोज नये क्षितिज छू रहा होता है, नयी खोजें हो रही होती हैं। इसके आलोक में समाज भी, धीमी गति से ही सही, अपनी मूल्य-मान्यताओं और विधि-विधान को निरंतर पुनर्निरीक्षित, संशोधित और अनुकूलित करते रहते हैं। सभ्यताओं के विकास के किसी दौर में, किन्हीं तत्कालीन परिस्थितियों में अस्तित्व में आयीं तमाम परम्पराएं, जो बाद में पत्थर की लकीर मानी जाने लगती हैं, इसी क्रम में कब उनकी चूलें हिल जाती हैं और अस्तित्वहीन होते-होते कब वे विलुप्त हो जाती हैं, पता ही नहीं चल पाता। रूढ़ हो चुके धार्मिक रीति-रिवाज भी इसी सिलसिले के साथ, अनजाने ही अपनी प्रासंगिकता खोते चले जाते हैं और ग़ैरज़रूरी, और कभी-कभी तो बोझ, लगने लगते हैं और धीरे-धीरे उनका परित्याग कर दिया जाता है।
यह सब तो सामाजिक विकास की सहज-स्वाभाविक गतिकी का हिस्सा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ, या कभी-कभी बहुत सारे रीति-रिवाज पूरे समुदाय के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने लगते हैं। उनकी विकसित हो रही समझदारी के प्रतिकूल दिखने लगते हैं और हथकड़ी और बेड़ी जैसे प्रतीत होने लगते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में समाज की बेचैनी और आशाओं-आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति आगे आते हैं और देखते-देखते एक विशाल धर्मसुधार आंदोलन खड़ा हो जाता है।
सामाजिक विकास की सामान्य गतिकी के तहत जो परिवर्तन सदियों में होते हैं, ये आंदोलन उतना परिवर्तन दशकों, या कभी-कभी वर्षों में कर डालते हैं। ये आंदोलन शताब्दियों के फंसे हुए मलबे और कचरे को एक झटके में साफ करके पूरे समुदाय को फिर से प्रवाहमान कर देते हैं।
अनुयायियों की संख्या के लिहाज से भारत के दोनों बड़े धर्मों में लंबे अरसे से कोई सुधार आंदोलन नहीं हुआ है, जबकि दोनों को इसकी जरूरत है। लेकिन यहां मैं खास करके बहुसंख्यकों के धर्म, हिंदू धर्म की चर्चा करूंगा, एक तो इसलिए कि पिछले कई दशकों से यहां बहुसंख्यकवाद की राजनीति परवान चढ़ी हुई है, और इसी बैसाखी के सहारे सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया जा चुका है। और दूसरे, इसलिए कि धर्मसुधार का मंतव्य ही अपने धर्म में सुधार होता है, न कि दूसरे धर्म में सुधार। दूसरे धर्म में सुधार का आह्वान तो आजकल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का अस्त्र बन चुका है। धर्म की राजनीति करने वालों की सारी कोशिश रहती है कि दूसरे धर्म की कमियों को उजागर किया जाए और अपने धर्म की कमियों को जायज ठहराया जाए और गौरवान्वित किया जाए। किसी धर्म के लोगों को एकजुट करने के लिए दूसरे धर्म के प्रति घृणा फैलाने की जगह अपने धर्म के भीतर के संबंधों की घृणास्पद प्रकृति के खात्मे की कोई इच्छा तक दिखाई नहीं देती।
भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच एक धर्मसुधार आंदोलन अति आवश्यक हो गया है। हिंदुओं को अपना वोट बैंक मानने वालों की ऐसी कोई मंशा नहीं है। जोर-जोर से हिंदू-हिंदू चिल्लाने वाले लोग और संगठन हिंदुओं के बीच कोई भी सामाजिक सुधार न तो करना चाहते हैं, न ही होने देना चाहते हैं। हिंदू-हिंदू चिल्लाते हुए वे भूल जाते हैं कि उनके बीच आपसी संबंध और भाईचारा कितना कमजोर है। हिंदुओं की एकता की बात करने वाले ही खुद अपने ही धर्म के लोगों, और अपने सगे भाई तक का हक दबा लेने के लिए सारी तिकड़म लगा रहे हैं।
करोड़ों हिंदुओं के पास कोई संपत्ति नहीं है, रोजी-रोटी के साधन नहीं हैं, शिक्षा, चिकित्सा के अवसर और अधिकार नहीं हैं। जिनके पास संपत्ति और साधन हैं, वे दूसरों को ये सुविधाएं दिलाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनको दूसरे धर्मों के खिलाफ आवाज उठाने को ललकार रहे हैं। एक धर्म के भीतर तो कम से कम इतनी बराबरी, आत्मीयता और भाईचारे की भावना होनी ही चाहिए कि उसके सभी सदस्य उस धर्म के साथ अपना जुड़ाव महसूस कर सकें; लिंग, जाति, वर्ण, क्षेत्र, वेश, भाषा, पंथ, मत-मतांतर के आधार पर ऊंचा या नीचा न महसूस करें; धन-संपदा के मालिकाने में ग़ैरबराबरी के आधार पर शोषित होने और ग़ुलामी करने को मजबूर न हों।
हिंदू समाज बुरी तरह से बंटा हुआ समाज है। जातीय भेदभाव और छुआछूत अब भी जारी है, भारी आर्थिक असमानता है। इसे दूर करने की ये लोग कोई कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसे बनाये रखने के लिए सारी ताक़त लगा रहे हैं। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के अपमान और उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं रोज घटती रहती हैं। ये घटनाएं इतनी आम हैं कि ज्यादातर लोग तो इनकी नोटिस तक नहीं लेते। समाज और अर्थव्यवस्था के सभी अन्य हिस्सों की तरह मीडिया में भी उच्च जातियों तथा उच्चजातीय सोच के वर्चस्व के कारण अधिसंख्य ऐसी घटनाओं को सहज-स्वाभाविक माना जाता है और वे प्रकाश में भी नहीं आ पातीं।
‘एनसीआरबी’ के आंकड़ों के अनुसार केवल 2018 से 2020 के दौरान देश भर में दलितों के खिलाफ अपराध की 1,30,000 घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें से केवल उत्तर प्रदेश में 36,467, बिहार में 20,973, राजस्थान में 18,418 और मध्यप्रदेश में 16,952 दर्ज की गयीं। पूरी हिंदी पट्टी उच्चजाति वर्चस्ववादी घृणा का गढ़ बनी हुई है। ‘इक्वलिटी नाउ’ के अनुसार प्रतिदिन 10 दलित महिलाओं या लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी जान जाने के डर से न्याय की गुहार नहीं लगातीं।
हिंदू समाज के बीच भाईचारे का आलम यह है कि दलितों के साथ हुए अन्याय की किसी घटना के प्रकाश में आते ही, तथ्यों की पड़ताल किये बिना ही उच्च जातियां अपनी जाति के अभियुक्त के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं और जातीय पंचायतों का आयोजन करके गोलबंदी शुरू कर देती हैं। हत्या और सामूहिक बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों के मामलों में भी यही होता है, इसकी बानगी जालौर और हाथरस जैसी हाल की घटनाओं में भी हमने देखा है। पीड़ित को न्याय दिलाने का रत्ती भर जज्बा नहीं रहता। ऐसे में धर्म के आधार पर एकता के बोध की गुंजाइश ही कहां रह जाती है।
भारतीय समाज में यों भी आर्थिक असमानता की स्थिति भीषण रही है, जिसमें जातीय पिरामिड के निचले हिस्से किसी भी तरह की संपत्ति के अधिकार से पूर्णतः वंचित रहे हैं, लेकिन अब तो यह असमानता सारी हदें पार करती जा रही है। ‘ऑक्सफैम’ की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के ऊपरी 10% लोगों के पास पूरी राष्ट्रीय संपदा का 77%, यानि निचले 50% लोगों से 22 गुना ज्यादा संपदा एकत्रित हो चुकी है। एक साल में देश की कुल कमाई का 73% हिस्सा केवल ऊपरी 1% लोगों के हाथों में जाने लगा है। जाहिर है कि पहले से ही वंचित निचली जातियों के हाथों में तो और भी ‘न कुछ’ के बराबर ही पहुंचता होगा। लेकिन हिंदू एकता का नारा लगा-लगाकर घृणा का माहौल बनाते रहने और राजनीति की रोटी सेंकने वालों में इस निर्लज्ज असमानता के खिलाफ कहीं कोई सुगबुगाहट तक नहीं है।
यहां तक कि उच्च जाति के हिंदुओं में दलितों-पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ भारी आक्रोश रहता है। लेकिन हाल के वर्षों में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के अंधाधुंध निजीकरण से सारी की सारी नौकरियों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन खत्म कर दी गयी, इस सबसे न केवल दलितों के, बल्कि पूरे हिंदू समाज के कंगालीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इस पर भी न कहीं चर्चा है, न ही इसके खिलाफ एकजुटता और संघर्ष की कोई पहल दिख रही है।
हमारा समाज महिलाओं के लिए अब भी एक पराया समाज बना हुआ है। वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, न घर के भीतर, न घर के बाहर, यहां तक कि गर्भ के भीतर भी नहीं। हमारी यह आधी आबादी कन्या भ्रूणहत्या, कन्या शिशु हत्या, परवरिश से रोजगार तक लैंगिक भेदभाव की शिकार, पैतृक संपत्ति में अधिकार के मामले में भेदभाव, दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या, जीवन के हर मोड़ पर घरेलू हिंसा और शैशव से वृद्धावस्था तक किसी भी उम्र में बलात्कार की आशंका से घिरी हुई जीवन जी रही है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक लैंगिक हिंसा की शिकार 85% महिलाएं इस संबंध में किसी से सहायता नहीं मांगतीं और केवल 1% ही पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराती हैं। जाहिर है कि इन महिलाओं के अधिसंख्य उत्पीड़क और शिकारी उनके सगे-संबंधी और स्वधर्मी लोग ही हैं। लेकिन हम हिंदू खुद अपनी ही आधी आबादी की इस बेइंतहां वेदना के प्रति घोर असंवेदनशील बने हुए हैं। इस मुद्दे पर धर्म के सभी स्वघोषित ठेकेदारों के मुंह में दही जम जाती है। जो समाज इस हद तक निर्लज्ज है कि दूसरे धर्म की निरीह स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा पाये हुए हिंदुओं का स्वागत करता है, मिठाइयां बांटता है, उन्हें संस्कारी ब्राह्मण बताता है, उसके भीतर सदियों से जड़ जमाये बैठे स्त्री-द्वेष की महज कल्पना ही की जा सकती है।
वेश्यावृत्ति किसी भी समाज के लिए कलंक का विषय होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों को खत्म करना, जिनमें कोई भी स्त्री वेश्या का पेशा अपनाने को मजबूर होती है, किसी भी सभ्य समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हमारे किसी भी धर्म-ध्वजाधारी ने आज तक न इस संबंध में कोई आह्वान किया है, न ही इस पेशे को पैदा करने वाली परिस्थितियों पर कोई ऐतराज जताया है।
किसी धर्म को अगर छोड़कर लोग जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके साथ ये लोग जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हैं। या तो उन्हें अपने धर्म में कोई कमी नजर आ रही है, या अन्य धर्म में कोई अच्छाई नजर आ रही है, या दोनों बातें सही हैं। इनका पता लगाने और ठीक करने की कहीं कोई कोशिश नहीं दिख रही। ये चीजें बलपूर्वक रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, जो अंततः लोगों में अपने धर्म से और ज्यादा मोहभंग पैदा करेंगी।
क्या हिंदू धर्म का मतलब यही है, कि काल्पनिक अतीत का कोई जमाना लौटा लाया गया है, जहां चारों तरफ हवन-कुंड हैं, अग्निशिखाएं आसमान छू रही हैं, लंबी-लंबी दाढ़ियों वाले पीतांबरधारी ऋषि लोग इन कुंडों में हवन-सामग्री और कूड़े भर-भर कर घी झोंकते जा रहे हैं, पूरा वायुमंडल इस पवित्र, सुगंधित, गाढ़े धुएं से भरा हुआ है, पगडंडियों पर घोड़े, रथ और बैलगाड़ियां दौड़ रही हैं?! या हिंदू धर्म का अपने अनुयायियों की रोजी-रोटी, न्याय और आत्मसम्मान जैसी रोजमर्रा की जरूरतों से भी कुछ लेना-देना है!
अपने अतीत को गौरवशाली साबित करने की कोशिश में ये लोग पूरे समाज को अतीत के पाताल लोक में पहुंचाने पर आमादा हैं। पूरी दुनिया जब अपने बच्चों को ज्ञान-विज्ञान सिखा रही है, उस समय ये लोग हमारे बच्चों को हस्तरेखा, ज्योतिष, हवन, जादू-टोना, भूत-बांधना और गोबर-गोमूत्र पान की महत्ता सिखाना चाह रहे हैं। हमें यह पता करते रहने की जरूरत है कि क्या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, विश्वविद्यालयों और उत्पादन के बड़े-बड़े केंद्रों के बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हमारे ही धर्म के लोग भी अपने बच्चों को यही सब पढ़ा रहे हैं कि केवल हमारे बच्चों को ही यह सब परोसा जा रहा है।
हमारे कुछ धार्मिक नेता तो शातिर होते हैं वे तो जानबूझ कर अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा हमारा समाज है, इसमें बड़ी संख्या ऐसे नेताओं की भी है जो इन ऊल-जुलूल, बेसिर-पैर की बातों पर वास्तव में विश्वास करते हैं। ऐसा इसलिए है कि इस समाज में ज्ञानोदय की क्रांति हुई ही नहीं।
बात जब तक कम पढ़े-लिखे और मान्यता-प्राप्त कम समझदार लोगों के बावला होने तक सीमित हो, तब तक तो फिर भी झेला जा सकता है, लेकिन जब मान्यता-प्राप्त सर्वाधिक समझदार हिज हाइनेस लोग लुच्चे-लफंगों को पीछे छोड़ने लगें तो समझना चाहिए कि अब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा है। समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। कोई सभ्यतागत दोष है जिसकी वजह से सारे प्रोडक्ट न्यूनाधिक मात्रा में दोषपूर्ण होते जा रहे हैं, और दोष की जड़ों को पहचान कर पूरे सिस्टम को फॉर्मेट मारना अनिवार्य हो गया है।
हीनता-ग्रंथि से पैदा हुई कुंठा के कारण भी किसी समाज की दो गतियां संभव हैं। एक तो वह भविष्योन्मुखी होकर अपने वर्तमान और भविष्य को संवारने में अपने प्राणपण से जुट सकता है। जबकि दूसरी स्थिति में वह अतीतोन्मुखी हो सकता है और एक काल्पनिक गौरवशाली अतीत को पुनर्प्राप्त करने में अपनी सारी ऊर्जा झोंक सकता है। दुर्भाग्य से भारत के वर्तमान नेतृत्व ने उसके लिए दूसरा वाला रास्ता चुना है। जब कोई पूरी सभ्यता आगे देखने की बजाय पीछे देखते हुए आगे चल रही हो तो उसका खाईं में गिरना तय है।
आज हिंदुओं के ऊपर खतरे की चेतावनी जारी करने वाले वही लोग हैं जो एक समय सती-प्रथा के खिलाफ आंदोलन को भी हिंदू धर्म पर खतरा बता रहे थे। ये लोग समाज में ज्ञान-विज्ञान और प्रगतिशील मूल्यों की किसी भी रोशनी के प्रवेश पर खतरे की चेतावनी जारी करते रहते हैं।
हमें सोचना होगा कि अगर धर्म हमारे लौकिक जीवन को समृद्ध और सुगम बनाने और हमारी वैचारिक तथा सृजनात्मक, सभी संभावनाओं को साकार करने का जरिया नहीं बन सकता तो ऐसे धर्म की जरूरत ही क्या है? अगर धर्म हमारे जीवन को नारकीय बनाने वाली मूल्य-मान्यताओं, तौर-तरीक़ों, रीति-रिवाजों और सामाजिक-आर्थिक संबंधों को धर्म का अभिन्न भाग समझता है और उनमें परिवर्तन की कोशिश को धर्म पर हमला समझता है तो ऐसे धर्म की जरूरत ही क्या है?
न केवल हमारे धार्मिक नेतृत्व को, बल्कि हमारे पूरे समाज को इस संबंध में गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
(शैलेश स्वतंत्र लेखक हैं।)