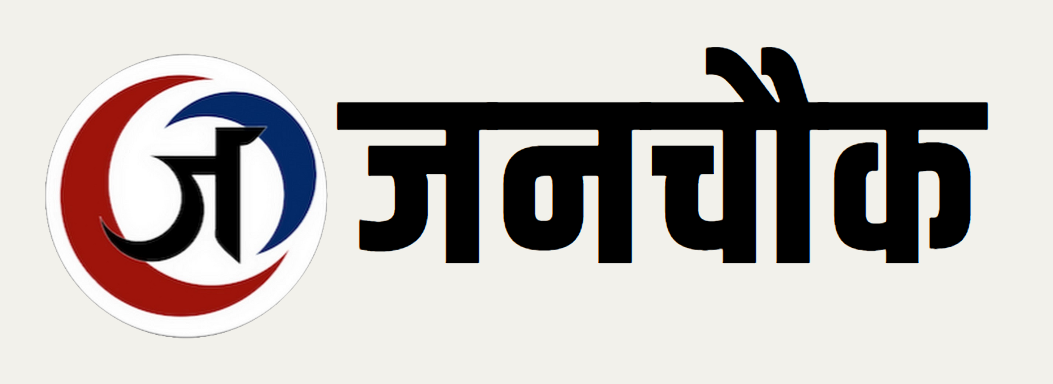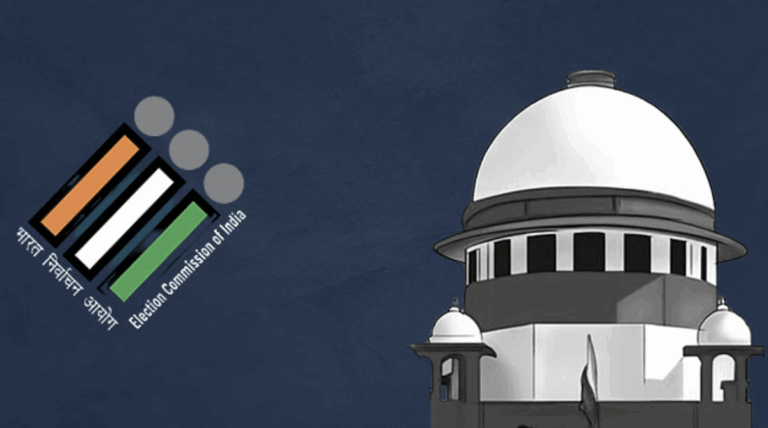वंचित तबक़ों के लिए आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी बाबा साहेब आंबेडकर का सिद्धांत रहा है। मगर, वे सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते थे। डॉ. आंबेडकर की इस बात से सीख लेते हुए दलित नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने अपनी राजनीतिक गोलबंदी के माध्यम से लोकतन्त्र में अपनी जगह बनाई। लोकतन्त्र में बन रही जगह का इस्तेमाल उन्होंने अपनी राजनीति को बनाने के लिए किया साथ ही दलित कार्यकर्ताओं द्वारा दैनंदिनी राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप भी शुरू किया गया।
इस सक्रिय हस्तक्षेप से उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया लेकिन दलितों का यह सक्रिय हस्तक्षेप और इसके व्यापक संदर्भों में बन रही बड़ी दलित सक्रियता और राजनीति ने अब अपना ध्यान दलित राजनीति की ओर बढ़ाया और राज्य तंत्र के पावर स्ट्रक्चर (सत्ता तंत्र) में भागीदारी, जोड़तोड़ के पापुलर तौर तरीकों के सारे गुण भी सीख लिए और यह सब भारतीय लोकतन्त्र का तोहफा भी रहा है उनके लिए। क्योंकि भारतीय लोकतन्त्र ने जिस तरह से अपना विकास किया उसी तरह का लोकतन्त्र दलितों को भी मिला।
इस दौरान दलितों ने अपनी पार्टी को सशक्त बनाया-जोड़तोड़ की सरकार बनाई, खुद अपने दम पर भी सरकार बनाई। इस बीच दलितों ने राजनीतिक सफलताओं-असफलताओं का एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दलितों ने जब सत्ता में भागीदारी की तब उसको बहुत कम हासिल हुआ सिवाय व्यक्तिगत नेताओं और उनकी उपलब्धियों के। लेकिन इसके उलट अगर देखा जाए तो दलितों ने अपने आंदोलनों और संघर्षों के माध्यम से अपने लिए अधिक हासिल किया है और वह भी पूरे समुदाय के लिए सामूहिक रूप से। लेकिन 21वीं सदी के दहाई के अंत में जब हम आज देखते हैं तो चीजें काफी बदल गयी हैं। जो दलित सक्रियता और दलित राजनीति ने दबाव बनाया था अब वह टूटने लगा है।
इसका सबसे सटीक संदर्भ बिहार के विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है। एक तरफ दिवंगत कद्दावर दलित नेता रामविलास की स्थापित जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा उनके सुपुत्र चिराग पासवान ने भाजपा गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की राह पकड़ ली है। लेकिन क्यों? किस आधार पर? क्या उनके पास कोई दलित एजेंडा है या सिर्फ किसी खास मकसद की चुनावी रणनीति के तौर पर उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान के पास कोई स्वतंत्र दलित एजेंडा है। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह की राजनीति करना चाहते है वह रामविलास पासवान से बिल्कुल अलग राह रखती है। रामविलास पासवान ने चाहे जिस तरह की राजनीति की हो लेकिन दलित एजेंडा और आरक्षण उनके मुख्य एजेंडे में शामिल थे।

वहीं चिराग ने कुछ समय पहले आरक्षण के प्रति एक अलग दृष्टिकोण की बात की थी जब 2016 के अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि ”जिस तरह से अमीर गैस सब्सिडी छोड़ रहे हैं उसी तरह से अमीर दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। चिराग ने यह भी कहा था कि मैं समाज को किसी भी तरह के जातिवाद से रहित देखना चाहता हूँ। इसके साथ ही आरक्षण छोड़ने का फैसला स्वेच्छा से होना चाहिए न कि जोर जबर्दस्ती से। ऐसा हो जाने पर जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। इसके आगे चिराग ने यह भी कहा था कि वह बिहार से आते हैं जहां जातिगत समीकरण हावी रहते हैं।” मुझे लगता है चिराग किसी संघर्ष की राजनीति से तो आए नहीं हैं। आरक्षण को प्राप्त करना और उसके दंश को कोई भुक्तभोगी ही अधिक ठीक ढंग से बयान कर सकता है। आरक्षण को छोड़ देना, हटा देना मैं जातिवाद को नहीं मानता हूँ, मैं जातिवाद को खत्म करना चाहता हूँ!
ये बातें किसी दूरदर्शी दलित नेता की नहीं हो सकतीं। डॉ. आंबेडकर से लेकर वर्तमान दलित नेतृत्व हो या दलित राजनीति हो सभी ने एक सामाजिक परिवर्तन की बात की है जातिवाद को खत्म करना उन सभी की प्राथमिकताओं में रहा है। लेकिन आरक्षण की कीमत पर नहीं। चिराग की बात तभी सही ढंग से प्रासंगिक होगी जब यह समीक्षा हो जाए की आरक्षण कितना प्रतिशत लागू हो पाया है और कहाँ-कहाँ लागू हो पाया है, कहाँ-कहाँ नहीं। एक सवाल के तौर पर खेल का क्षेत्र, भारतीय प्रबंधन संस्थान, सेना आदि-आदि बहुत सारी जगहें जहां दलित उपस्थिति खोजते रह जाइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं बिहार चुनाव पर।
वहीं दूसरी तरफ जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तान आवामी मोर्चा (हम) और अपने आप को ‘सन ऑफ मल्लाह’ कहने वाले मुकेश साहनी निषाद की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी), उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टियां है। जो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उल्टे सीधे गठजोड़ों से भी परहेज नहीं कर रहे हैं जबकि कल तक ये सभी भाजपा का धुर विरोध करते रहे हैं और यह विरोध दलितों-पिछड़ों के खिलाफ हिंसा, उनके संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण आदि का आधार था। चूंकि यह सब इसलिए किया जाता है ताकि अपने समुदाय के सवालों को उठाते हुये एक राजनीतिक गोलबंदी की जाए और सत्ता में किस तरह से हिस्सेदारी की जाए। क्योंकि अब इनके पास कोई व्यापक एजेंडा नहीं है सिवाय राजनीतिक सत्ता के साथ हिस्सेदारी के।
वह चाहे जैसे भी हासिल कि जा सके। बिहार विधानसभा के इस चुनाव में ही देख लीजिये गठबंधन कर रहे दलितों-पिछड़ों के जनाधार वाले दलों के पास कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ है तो चुनावी राजनीति के हिसाब से बन रहे समीकरण और उसमें हिस्सेदारी। अब मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी, जिसे सीटों के बँटवारे में भाजपा ने ना केवल ग्यारह सीटें दी बल्कि एक विधान परिषद की सीट देने की भी घोषणा की है। वहीं महादलित, दलित और पिछड़ों के वोटों को साधने की कोशिश में नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल हो गए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जेडीयू के साथ जोड़ लिया है। जीतन राम मांझी को एनडीए में आने का पहला फायदा पहुंचाया गया है। बिहार सरकार की अनुंशसा पर मांझी की सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया गया है। जीतन राम मांझी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गठबंधन सहयोगी के तौर पर ‘हम’ को कुल सात सीटें दी गई हैं जिसमें से पांच सुरक्षित सीटें हैं।
बिहार के इस चुनावी गठबंधन में जीतनराम माझी की ‘हम’ को ही देख लीजिये ये अपने नाम के हिसाब से ‘हम’ और हमारे परिवार और उसके आगे हमारे रिश्तेदार वाली कहानी को बयान कर रही है। वहीं मुकेश साहनी की वीआईपी अपने नाम के हिसाब से बिल्कुल वीआईपी ही है खबरों के अनुसार मुकेश साहनी टिकट लिए घूम रहे हैं कोई लेने ही नहीं आ रहा है।
इसके अलावा अपना अलग दल बनाने वाले नेताओं को भी चुनावी वैतरणी पार करने के लिए सहारे की जरूरत थी। कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए से इनकी बात होती रही। समय बीत गया तो बिना सहारे मैदान में उतरे हैं। कुछ हाथ-पांव समेटकर चुप बैठ गये हैं। उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा भी एनडीए से अलग होने के बाद लोकसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ी। कहीं भी सफलता नहीं मिली। लेकिन महागठबंधन में ही बने रहे। विष पीने की घोषणा भी विधानसभा चुनाव में काम नहीं आई। वह भी अब ओबैसी की पार्टी, बसपा और देवेन्द्र यादव सहित छह दलों का गठबंधन बनाकर चुनाव को नया कोण देने में लगे हैं।
अलग दल बनाने वाले नेताओं में जीतन राम मांझी को हर बार किसी ना किसी गठबंधन में जगह मिल जाती है। लेकिन, बार-बार दल और गठबंधन बदलने वाले नेताओं को जनता के पहले राज्य की राजनीति में जमे बड़े गठबंधनों ने भी छोड़ दिया। उधर, बड़े गठबंधनों में शामिल बड़े दलों के टिकट से वंचित नेता भी अपना जुगाड़ इन छोटे दलों में लगाने लगे हैं। रामेश्वर चौरसिया, राजेन्द्र सिंह और ऊषा विद्यार्थी सरीखे भाजपा के कई नेताओं ने लोजपा से टिकट हासिल कर लिया है। लेकिन अभी भी कई नेता इन छोटे दलों के बैनर से अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, देवेंद्र प्रताप यादव तथा डा. संजय चौहान के गठबंधन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विधायक ओमप्रकाश राजभर भी शामिल हो गए हैं। छह दलों को मिलाकर बने विराट लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के बैनर तले राजभर की पार्टी सुभासपा को पांच सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी गई हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि यह मोर्चा बिहार में 30 सालों की बदहाली समाप्त करने का काम करेगा। रालोसपा, बसपा, एआईएमएएम, सजद डेमोक्रेटिक, जनवादी पार्टी तथा सुभासपा के एकजुट होने से बिहार की चुनावी तस्वीर बदल गई है।

इस तरह से बिहार विधानसभा के इस चुनाव ने राज्य के कई नामदार नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया है। ऐसे कुछ नेताओं ने अपना दल बना लिया। लेकिन, इन बड़े नाम वाले नेताओं के छोटे दलों को किसी गठबंधन में जगह नहीं मिली तो अब चुनावी मैदान में अकेले अपनी जमीन तलाश रहे हैं। कोई उम्मीदवार उधार लेकर मैदान में उतर रहा है तो कोई मोर्चा बनाकर बड़े गठबंधनों को चुनौती देने का प्रयास कर अपनी साख बचाने में जुटा है। ये नेता अब चुनावी मैदान में जीत से ज्यादा खुद को राजनीति में जिन्दा रखने की कोशिश में लगे हैं। एक गठबंधन पप्पू यादव के नेतृत्व में भी बना है जिसमें भीम आर्मी भी शामिल है।
बिहार विधानसभा चुनाव में एक महागठबंधन भी है जिसको मैं बेमेल गठबंधन कहना चाहूँगा वह है राजद, कांग्रेस और लेफ्ट का। तीनों ही वैचारिक सैद्धान्तिक रूप से बिल्कुल भिन्नता वाले दल हैं। लेकिन अगर यह महागठबंधन सिर्फ भाजपा और नरेंद्र मोदी को चुनावी राजनीति में शिकस्त देना चाहता है तो मुझे कुछ शंका सी लगती है क्योंकि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लालू प्रसाद यादव जैसा करिश्मा कलेजा और नेतृत्व चाहिए जो नरेंद्र मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। पिछला चुनाव याद कीजिये लालू ने किस तरह से व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी को उन्हीं की भाषा शैली में जवाब दिया था। लेकिन इस बार लालू मैदान में नहीं हैं और लालू वाला करिश्मा इन तीनों ही दलों के किसी नेताओं में नहीं है।
इस तरह के बनते बिगड़ते गठबंधनों से भाजपा को भी इन सभी से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाजपा को इससे राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि इस तरह के गठबंधनों के प्रयोग यह बताते हैं कि इसमें पार्टी मुखिया के साथ एक दो कद्दावर नेता ही चुनाव जीतने में सफल होते है बाकी का वोट उस बड़ी पार्टी को चला जाता है जिसके साथ उसका गठबंधन हुआ है। उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा के चुनाव में ओमप्रकाश राजभर और उनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) का उदाहरण हम सबके सामने है। ओम प्रकाश राजभर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में उनकी पार्टी ने भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। राजभर समाज में उनकी पकड़ को देखते हुए ही भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग की मुहिम के तहत 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने से जोड़ा।
उन्हें आठ सीटें दी, जिसमें से चार स्थानों पर सुभासपा विजयी रही। ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा से जीते तो उनके तीन विधायक रामानंद बौद्ध रामकोला, त्रिवेणी राम जखनिया और कैलाश नाथ सोनकर अजगरा से जीते पार्टी को 6,07,911 वोट मिले थे। इस जीत ने सुभासपा को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने भाजपा से इसकी पूरी कीमत वसूलनी चाही। मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर को जगह तो मिल गई लेकिन उनकी अन्य मांगें- पार्टी के लिए लखनऊ में कार्यालय, पार्टी नेताओं को मंत्री का दर्जा आदि योगी सरकार ने पूरी नहीं की। वह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा से सीटें चाहते थे, लेकिन बात न बनने पर उन्होंने बगावती तेवर अपनाते हुए 39 सीटों पर सुभासपा उम्मीदवार उतार दिए। इस नाराजगी के चलते लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के ठीक एक दिन बाद 20 मई को उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया।
इस तरह से भारतीय चुनावी राजनीति में इस प्रकार के कई प्रयोग होते रहते हैं। लेकिन जो दल किसी खास जाति विशेष समर्थन के आधार वाले दल होते हैं उनका भविष्य ज्यादा अधिक दिन तक नहीं होता है। क्योंकि वह दबाव की राजनीति के माध्यम से सौदेबाजी वाली राजनीति करना चाहते हैं। इससे व्यापक संदर्भ में दलित और पिछड़ी राजनीति की एकता कमजोर होती है। बिहार चुनाव के संदर्भ में इस बार कुछ ऐसा ही लग रहा है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा।
चुनावी राजनीति में एक समय में दलित मुद्दे शामिल रहते थे, भले ही दबाववश रहते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की चुनावी राजनीति में पराजय ने इस समय दलित एजेंडे को भी हाशिये पर ढकेल दिया है। ऐसा लगता है कि बहुजन बहुजन समाज पार्टी की एक दलित आधारित दल के रूप में चुनावी पराजय ने मुख्यधारा के राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा को भी अब दलित मुद्दों के प्रति कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई है। चुनावी राजनीति में दलित अब अदृश्य भीड़ के रूप में अदृश्य वोटर मात्र है। जबकि इस दौर में दलित उत्पीड़न की सबसे अधिक घटनाएँ सामने आ रही है।

जब दलित मुद्दे राजनीति के केंद्र में होने चाहिए थे तब वह हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। सिर्फ दलित मुद्दे ही नहीं इस तरह की राजनीतिक गठजोड़ों की वजह से जनता के वास्तविक और व्यापक मुद्दे भी हाशिये पर चले जाते है और पूरी की पूरी बहस जाति आधारित गठजोड़ों और जातीय समीकरणों पर केन्द्रित हो जाती है। इसके लिए बड़े राजनीतिक दल चुनावी एजेंडा तय करते हैं और छोटे जाति आधारित दल उनमें फंस जाते हैं। क्योंकि बिहार के इन चुनावों में न मजदूरों के पलायन का मुद्दा बहस में है, न ही बिहार की बाढ़, बेरोजगारी के मुद्दे और न ही वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकारों से जवाबदेही के सवाल। राजनीतिक दलों की बहसों में अगर कोई मुद्दा है तो वह है सिर्फ और सिर्फ किस तरह से सरकार बना ली जाए उसके लिए चाहे जिसके साथ गठबंधन करना पड़े, वह सभी कर रहे हैं। कम से कम इस बार के बिहार के चुनाव को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है।
चुनावी राजनीति में दलित मुद्दों के अदृश्य होने की प्रक्रिया 2014 के लोकसभा चुनावों से ही शुरू हो गई थी जब सारी बहस विकास के विचार में सीमित कर दी गई थी। तब से देश विकास के पथ पर चल रहा है। और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के विधानसभा चुनावों में भी दलित मुद्दे लगभग गायब ही रहे। सिवाय गुजरात के ऊना में दलित उत्पीड़न के बाद हुए आंदोलन के। दलित-पिछड़े जनाधार वाले दलों की अपनी रणनीतिक कमजोरियाँ हैं, लेकिन आज जो स्थिति है ऐसा लगता है कि दलित राजनीति, दलित आन्दोलन, दलित नेतृत्व सब अप्रासंगिक होते जा रहे हैं।
साथ में ये भी लग सकता है कि सब कुछ भाजपामय होता जा रहा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सटीक रणनीतिकार अमित शाह को दिया जा रहा है। क्योंकि इन दोनों नेताओं की जोड़ी के सामने विपक्ष क्या पक्ष के नेता भी पानी मांगते नजर आ रहे हैं। इसी तरह की कुछ स्थिति 1970 के दशक में इंदिरा गाँधी और उनके सटीक रणनीतिकार यशवंत राव चाह्वाण और कांग्रेस की रेडिकल राजनीति के तहत दलित जनाधार वाले रिपब्लिकन दल को विभाजित कर दिया वहाँ ऐसी भगदड़ मची कि रिपब्लिकन एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास से भर गए और समय के साथ अप्रासंगिक भी हो गए। उसी धड़े के एक नेता रामदास आठवले कभी भाजपा और कभी शिवसेना के सहयोग से सांसद बनते रहते हैं। वर्तमान में वह केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं।
दलित राजनीति में स्वतंत्र रूप से एक मजबूत अभिव्यक्ति के रूप में कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी ने अपने रणनीतिक कौशलों कि वजह से उत्तर प्रदेश ही नहीं केंद्रीय राजनीति को 30 वर्षों से प्रभावित करती आई है और देश के दो बड़े राजनीतिक दलों को परेशान करके रखा हुआ था। लेकिन 2014 के बाद से स्थिति बहुत कुछ बदल सी गयी है अब यह पार्टी भी 1970 के दशक वाली रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति में पहुँच सी गयी है। मायावती के कुशल एकल नेतृत्व में इसने चुनावी राजनीति की कई सफल कहानियाँ अपने इतिहास में दर्ज की हैं लेकिन आज बसपा को सभी पुराने नेता छोड़ चुके हैं या मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है और धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के अलावा बसपा अन्य राज्यों से भी गायब होती जा रही है।
कुल मिलाकर एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में 1970 के दशक में कांग्रेस अपने उरूज पर थी तो वहीं आज भाजपा अपनी सफलता के चरम पर है। लेकिन दलित मुद्दे तब भी हाशिये पर गए थे और आज भी। इस बात को यदि व्यापक संदर्भों में देखें तो जिस तरह से सरकारों ने दलित हितों और उन्हें प्राप्त अधिकारों को समाप्त करने का कार्य किया है। तो यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि अब ”दलित सक्रियता” अब ”दलित भागीदारी” यानि दलितों द्वारा राजनीतिक भागीदारी में बदल गई है और यह भागीदारी उन्हें उल्टे सीधे गठजोड़ों की तरफ ले जा रही है। इस तरह से दलित नेतृत्व की राजनीतिक भागीदारी के बदले में दलितों-पिछड़ों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं।
(अजय कुमार, शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में फेलो रहे हैं।)